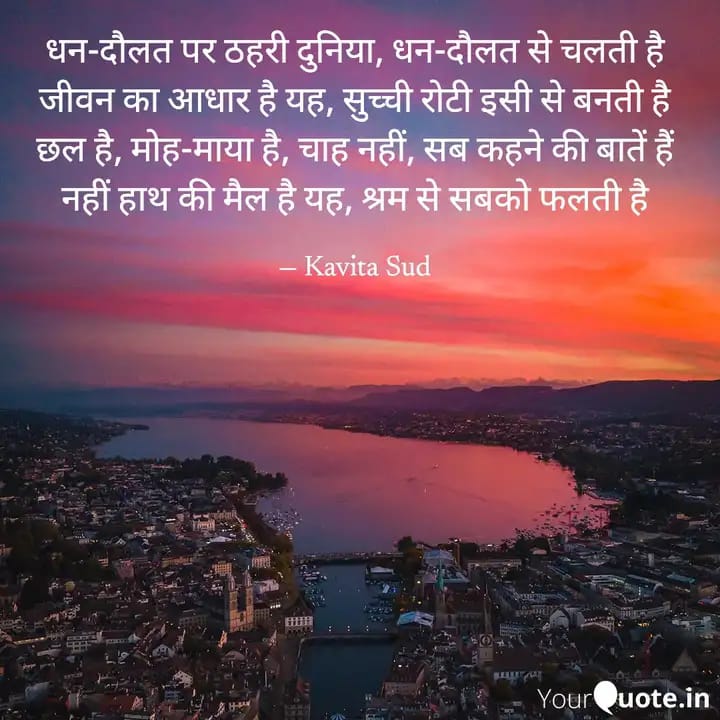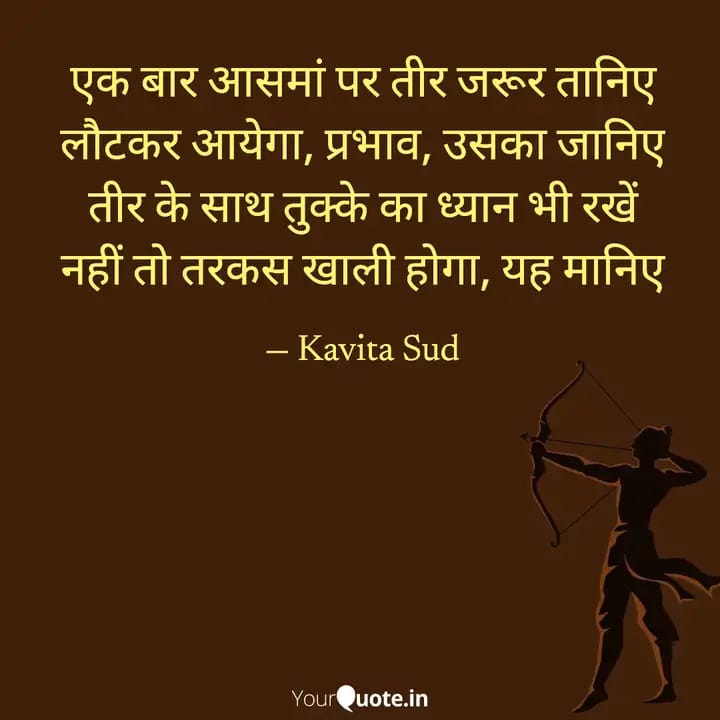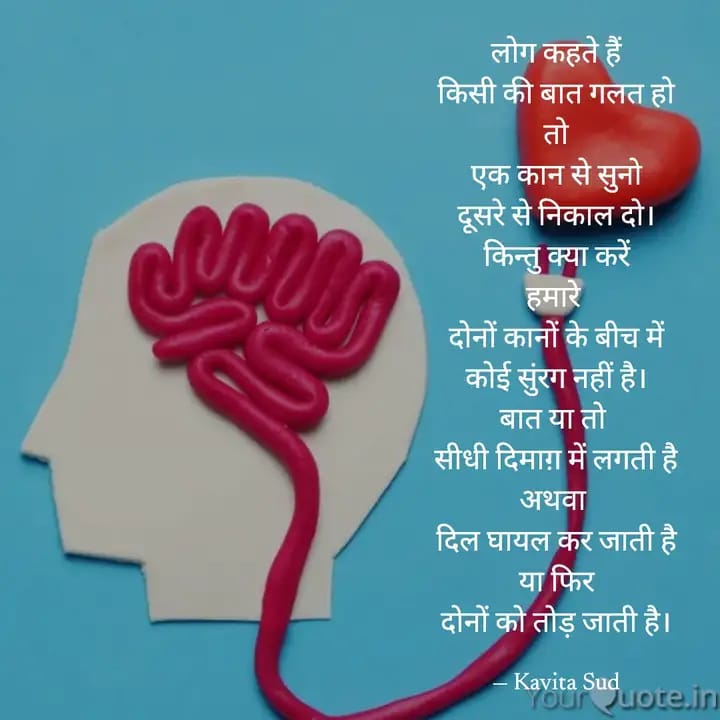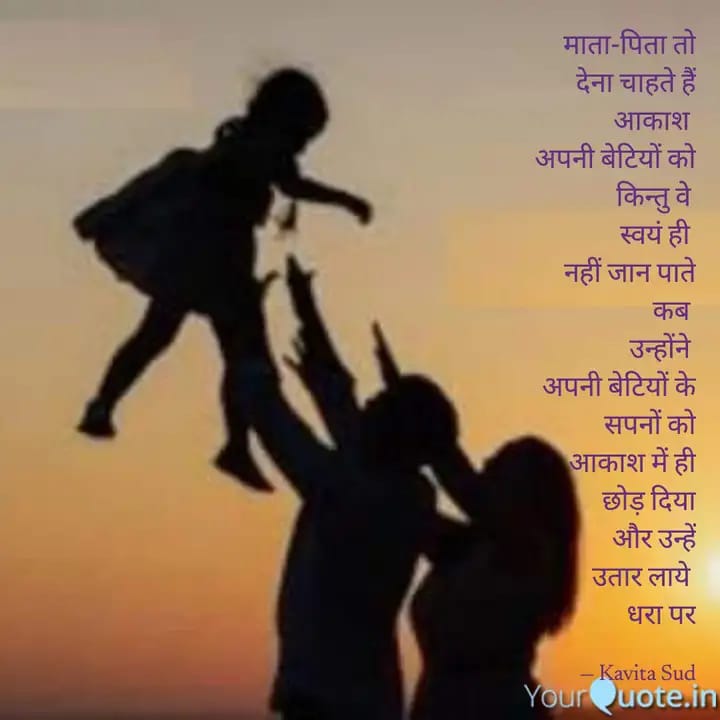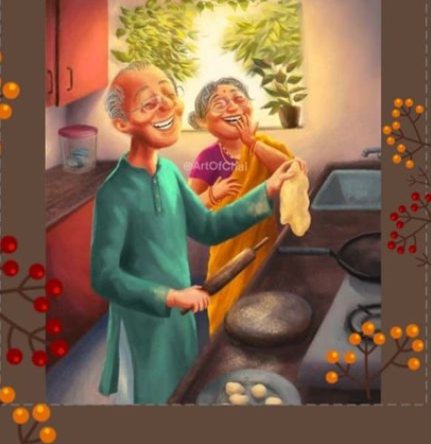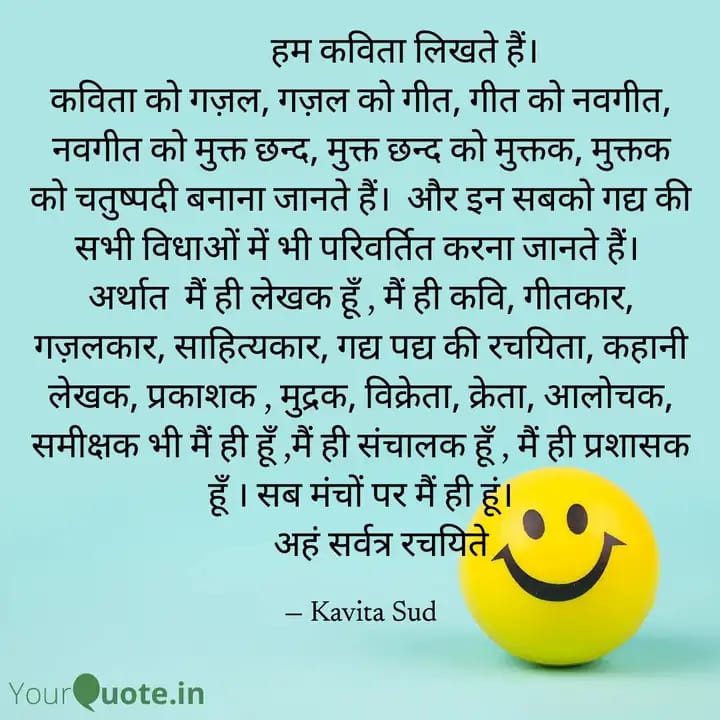बड़ा मुश्किल है Very Difficult
बड़ा मुश्किल है नाम कमाना
मेहनत का फल किसने जाना
बाधाएँ आती हैं आनी ही हैं
किसने राहें रोकी, भूल जाना
किसी के मन न भाती है
पुस्तकों पर सिर रखकर नींद बहुत अच्छी आती है
सपनों में परीक्षा देती, परिणाम की चिन्ता जाती है
सब कहते हैं पढ़-पढ़ ले, जीवन में कुछ अच्छा कर ले
कुछ भी कर लें, बन लें, तो भी किसी के मन न भाती है
तरुणी की तरुणाई
मौसम की तरुणाई से मन-मग्न हुई तरुणी
बादलों की अंगड़ाई से मन-भीग गई तरूणी
चिड़िया चहकी, कोयल कूकी, मोर बोले मधुर
मन मधुर-मधुर, प्रेम-रस में डूब गई तरुणी
व्रत एवं उपवास
‘‘व्रत’’ एवं ‘‘उपवास’’ हमारे पास ये दो शब्द हैं जिन्हें हम प्रायः एक ही अभिप्राय अथवा अर्थ में प्रयोग करते हैं अथवा कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं। किन्तु यह भी सत्य है कि पर्यायवाची शब्दों में भी अर्थ-भेद होता है।
व्याकरण के अनुसार ‘‘व्रत’’ शब्द का अर्थ ‘‘उपवास’’ के अतिरिक्त ‘‘शपथ, प्रण, क़सम, सौगंध’’ भी है। किन्तु हम वर्तमान में उपवास के लिए व्रत शब्द का ही अधिक प्रयोग करते हैं। वास्तव में उपवास करना भी एक व्रत है, सम्भवतः इसी कारण हम दोनों शब्दों का अर्थभेद भूलकर एक ही अभिप्राय से इनका प्रयोग करने लगे हैं।
क्या कभी आपने इस ओर ध्यान दिया है कि हमारे सारे व्रत बदलते मौसम में आते हैं। पहले नवरात्रि मार्च-अप्रैल में तथा दूसरी नवरात्रि सितम्बर-अक्तूबर में। इस समय मौसम बदलता है। प्रथम शीत ऋतु से ग्रीष्म में, द्वितीय सितम्बर-अक्तूबर में ग्रीष्म ऋतु से शीत में। शिवरात्रि पर्व भी मार्च में होता है और जन्माष्टी प्रायः अगस्त में, जब वर्षा ऋतु हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। उपरान्त तीज, करवाचौथ, होई आदि उपवास के पर्व भी इसी मौसम में आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में केवल जून में एक उपवास है निर्जलाकादशी। क्षेत्रानुसार भी अलग-अलग पर्व एवं व्रत-उपवास का विधान है।
बदलते मौसम में जहाँ हमारे खान-पान में परिवर्तन होने लगता है वहाँ हमारी पाचन-शक्ति भी प्रभावित होती है, निर्बल होने लगती है। उपवास एवं उपवास में विशेष एवं विविध प्रकार का खान-पान हमारे शरीर एवं पाचन-तंत्र को व्यवस्थित बनाने में सहायक होते हैं।
भारतीय मान्यताओं एवं हमारे भारतीय परिवारों में व्रत एवं उपवास एक अनुष्ठान है, पूजा विधि है, दिन, पर्व, काल की मान्यताएँ एवं परम्पराएँ हैं। स्वच्छता, पवित्रता, कठोर नियम, सबका बन्धन है। इसके अतिरिक्त माह एवं सप्ताह में कुछ दिन अधिक विशेष माने गये हैं, उन दिनों में भी खान-पान एवं व्रत का बन्धन माना जाता है, जैसे संक्राति, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, एकादशी आदि। अनेक परिवारों में इन में से किसी दिन खान-पान की शुद्धता, व्रत आदि का ध्यान किया जाता है। यह माना जाता है कि यदि सप्ताह में एक दिन उपवास किया जाये तो पाचन-शक्ति सबल रहती है एवं रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कुछ पदार्थों का भी निषेध रहता है।
इन सबके साथ ही श्रृंगार की विधियाँ भी हैं। जैसे करवाचौथ एवं तीज पर मेंहदी लगाना। मेंहदी का प्रभाव भी मानव शरीर को शीतलता प्रदान करता है, यह त्वचा के लिए लाभदायक होती है एवं रक्त प्रवाह को भी प्रभावित करती है। अधिक ज्वर की स्थिति में पैरों के तलवों में मेंहदी का लेप किया जाता था।
इन व्रतों की भोज्य सामग्री शरीर को मौसम के अनुकूल बनाने के लिए एवं पाचन-तंत्र को सशक्त बनाने में सहायक होती है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि भोजन में उन्हीं खाद्य-पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जो उसी मौसम के हों।
ये सब मान्यताएँ एवं पर्व पर्यावरण के अनुकूल, मानसिक एवं शारीरिक सन्तुलन नियन्त्रित रखने के लिए बने हैं। यह भी एक पूरा मौखिक ज्ञान-विज्ञान है जो महिलाएँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी सौंपती थीं।
किन्तु काल प्रवाह में, जीवन-शैली के परिवर्तन के साथ, दिनचर्या की कार्यविधियों के अनुकूल व्यवस्थाएँ बदलने लगीं, परम्पराएँ तिरोहित होने लगीं एवं मान्यताएँ भी। क्षेत्रानुसार मनाए जाने वाले तीज-त्योहारों, व्रतों का क्षेत्र विस्तृत होने लगा, सब मिश्रित होने लगा। इसमें कुछ भी गलत-ठीक नहीं होता, स्वाभाविक होता है। परिवार सीमित होने लगे, एकल परिवार बनने लगे और महिलाएँ घर से बाहर निकलीं। इन सब एवं अन्य अनेक कारणों से व्यवस्थाओं पर हमारा नियन्त्रण नहीं रह गया और बहुत कुछ सुविधानुसार परिवर्तित हो गया अथवा बदली हुई जीवन-शैली में हम स्वयँ को ढालने लगे जो अत्यावश्यक था। जितना स्मरण है, सुविधा है, आवश्यक है, हमारी विधियाँ वहीं तक सीमित होने लगीं। जो सब करते हैं वही हम कर लेते हैं।
बदली हुई जीवन-शैली, पारिवारिक व्यवस्थाएँ, बाहरी दायित्वों के कारण व्रतों के लिए बाज़ार स्वयँमेव ही सुविधाएँ एवं सामग्री उपलब्ध करवाने लगा। पहले हर वस्तु घर में बनाई जाती थी, किन्तु अब न वह कला बची है, न समय, न ही आवश्यकता। रसोई बदल गई, खान-पान के नियम बदल गये, समय-निर्धारण खो गया। रसोई घर स्टैंडिग हो गये, नियम स्वतः भंग होते चले गये, शायद यह कहना सकारात्मक होगा कि सुविधानुसार एवं बदली जीवन-शैली के अनुसार परिवर्तन स्वीकार कर लिए गये।
यही जीवन है और इसे हमें स्वीकार करना ही होगा अथवा करना ही चाहिए ऐसा मेरे विचार हैं।
शिकायतों का पुलिंदा
शिकायतों का
पुलिंदा है मेरे पास।
है तो सबके पास
बस सच बोलने का
मेरा ही ठेका है।
काश!
कि शिकायतें
आपसे होतीं
किसी और से होतीं,
इससे-उससे होतीं,
तब मैं कितनी प्रसन्न होती,
बिखेर देती
सारे जहाँ में।
इसकी, उसकी
बुराईयाँ कर-कर मन भरती।
किन्तु
क्या करुँ
सारी शिकायतें
अपने-आपसे ही हैं।
जहाँ बोलना चाहिए
वहाँ चुप्पी साध लेती हूँ
जहाँ मौन रहना चाहिए
वहाँ बक-झक कर जाती हूँ।
हँसते-हँसते
रोने लग जाती हूँ,
रोते-रोते हँस लेती हूँ।
न खड़े होने का सलीका
न बैठने का
न बात करने का,
बहक-बहक जाती हूँँ
मन कहीं टिकता नहीं
बस
उलझी-उलझी रह जाती हूँ।
मैं उपवास नहीं करती
मैं उपवास नहीं करती।
वह वाला
उपवास नहीं करती
जिसमें बन्धन हो।
मैंने देखा है
जो उपवास करते हैं
सारा दिन
ध्यान रहता है
अरे कुछ नहीं खाना
कुछ नहीं पीना।
अथवा
यह खाना और
यह पीना।
विशेष प्रकार का भोजन
स्वाद
कभी नमक रहित
कभी मिष्ठान्न सहित।
किस समय, किस रूप में,
यही चर्चा रहती है
दो दिन।
फिर
विशेष पूजा-पाठ,
सामग्री,
चाहे-अनचाहे
सबको उलझाना।
मैं बस मस्ती में जीती हूँ,
अपने कर्मों का
ध्यान करती हूँ,
अपनी ही
भूल-चूक पर
स्वयँ प्रायश्चित कर लेती हूँ
और अपने-आपको
स्वयँ क्षमा करती हूँ।
कौन-सा विषय चुनूँ
यह दुनिया है। आप कहेंगे कि आपको पता है कि यह दुनिया है। किन्तु बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वह भी स्मरण करना पड़ता है जो है, जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, चुभता है, चीखता है अथवा जो हम जानते हैं। क्योंकि सत्य का सामना करने में बहुत जोखिम होते हैं, उलझनें, समस्याएँ होती हैं। इस कारण इसे हम नकारते हैं और बस अपना राग अलापते हैं। क्या सच में ही आपके आस-पास कोई हलचल, खलबली, हंगामा, उपद्रव, उथल-पुथल, सनसनी, आन्दोलन नहीं है ? आस-पास, आपके परिवेश में, सड़क पर, समाचार-पत्रों से मिल रहे ज्ञान से, मीडिया से मिलने वाले समाचारों से, न जाने कितने विषय हैं जो हमारे आस-पास तैरते रहते हैं किन्तु हम उन्हें नकारते रहते हैं।
ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ तो होगा और अवश्य होगा। और हम जो तथाकथित कवि अथवा साहित्यकार कहलाते हैं या अपने को ऐसा समझते हैं तो हम ज़्यादा भावुक और संवेदनशील कहलातेे हैं। फिर हमें आज ऐसी आवाज़ें क्यों सुनाई नहीं दे रहीं। सबसे बड़ी समस्या यह कि यदि हम भुक्तभोगी भी होते हैं तब भी ऐसी बात कहने से, अथवा खुली चर्चा से डरने लगे हैं।
कुछ बने-बनाये विषय हैं आज हमारे पास लेखन के लिए। सबसे बड़ा विषय नारी है, बेचारी है, मति की मारी है, संस्कारी है, लेकिन है बुरी। या तो गंवार है अथवा आधुनिका, किन्तु दोनों ही स्थितियों में वह सामान्य नहीं है। भ्रूण हत्या है, बेटी है, निर्धनता है आदि-आदि। कहीं बहू बुरी है तो कहीं सास। कहीं दोनों ही। बेटा कुपूत है। बुरे बहू-बेटा हैं, कुपूत हैं, माता-पिता के धन के लालची हैं, उनकी सेवा न करने वाले बुरे बच्चे हैं। उनकी सम्पत्ति पर नज़र रखे हैं।जितने पति हैं सब पत्नियों के गुलाम हैं। उनके कहने से अपने माता-पिता की सेवा नहीं करते उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। और जब यह सब चुक जाये तो हम अत्यन्त आस्तिक हैं और इस विषय पर हम अबाध अपनी कलम चला सकते हैं। विशेषकर फ़ेसबुक का सारा कविता संसार इन्हीं विषयों से घिरा हुआ है। मुझे क्यों आपत्ति? मुझे नहीं आपत्ति। मैं भी तो आप सबके साथ ही हूँ।
सोचती हूँ आज इनमें से कौन-सा विषय चुनूँ कि रचना नवीन प्रतीत हो।
हादसे तो होते ही रहते हैं
2008 में भगदड़ मच जाने से करीब 145 लोगा की जान चली गई थी
नैना देवी में हादसा हुआ। श्रावण मेला था। समाचारों की विश्वसनीयता के अनुसार वहां लगभग बीस हज़ार लोग उपस्थित थे। पहाड़ी स्थान। उबड़-खाबड़, टेढ़े-मेढ़े संकरे रास्ते। सावन का महीना। मूसलाधार बारिश। ऐसी परिस्थितियों में एक हादसा हुआ। क्यों हुआ कोई नहीं जानता। कभी जांच समिति की रिपोर्ट आयेगी तब भी किसी को पता नहीं लगेगा।
किन्तु जैसा कि कहा गया कि शायद कोई अफवाह फैली कि पत्थर खिसक रहे हैं अथवा रेलिंग टूटी। यह भी कहा गया कि कुछ लोगों ने रेंलिंग से मन्दिर की छत पर चढ़ने का प्रयास किया तब यह हादसा हुआ।
किन्तु कारण कोई भी रहा हो, हादसा तो हो ही गया। वैसे भी ऐसी परिस्थितियों मंे हादसों की सम्भावनाएँ बनी ही रहती हैं। किन्तु ऐसी ही परिस्थितियों में आम आदमी की क्या भूमिका हो सकती है अथवा होनी चाहिए। जैसा कि कहा गया वहां बीस हज़ार दर्शनार्थी थे। उनके अतिरिक्त स्थानीय निवासी, पंडित-पुजारी; मार्ग में दुकानें-घर एवं भंडारों आदि में भी सैंकड़ों लोग रहे होंगे। बीस हज़ार में से लगभग एक सौ पचास लोग कुचल कर मारे गये और लगभग दो सौ लोग घायल हुए। अर्थात् उसके बाद भी वहां सुरक्षित बच गये लगभग बीस हज़ार लोग थे। किन्तु जैसा कि ऐसी परिस्थितियों में सदैव होता आया है उन हताहत लोगों की व्यवस्था के लिए पुलिस नहीं आई, सरकार ने कुछ नहीं किया, व्यवस्था नहीं थी, चिकित्सा सुविधाएँ नहीं थीं, सहायता नहीं मिली, जो भी हुआ बहुत देर से हुआ, पर्याप्त नहीं हुआ, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ; आदि -इत्यादि शिकायतें समाचार चैनलों, समाचार-पत्रों एवं लोगों ने की।
किन्तु प्रश्न यह है कि हादसा क्यों हुआ और हादसे के बाद की परिस्थितियों के लिए कौन उत्तरदायी है ? निश्चित रूप से इस हादसे के लिए वहां उपस्थित बीस हज़ार लोग ही उत्तरदायी हैं। यह कोई प्राकृतिक हादसा नहीं था, उन्हीं बीस हज़ार लोगों द्वारा उत्पे्ररित हादसा था यह। लोग मंदिरों में दर्शनों के लिए भक्ति-भाव के साथ जाते हैं। सत्य, ईमानदारी, प्रेम, सेवाभाव का पाठ पढ़ते हैं। ढेर सारे मंत्र, सूक्तियां, चालीसे, श्लोक कंठस्थ होते हैं। आगे बढ़ते हुए माता का जयकारा लगाते जाते हैं। किन्तु एक समय और एक सीमा के बाद सब भूल जाते हैं। ऐसे अवसरों पर सब जल्दी में रहते हैं। कोई भी कतार में, व्यवस्था में बना रहना नहीं चाहता। कतार तोड़कर, पैसे देकर, गलत रास्तों से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जहां दो हज़ार का स्थान है वहां हम बीस हज़ार या दो लाख एकत्र हो जाते हैं फिर कहते हैं हादसा हो गया। सरकार की गलती है, पुलिस नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। सड़कंे ठीक नहीं थीं। अब सरकार को चाहिए कि नैना देवी जैसे पहाड़ी रास्तों पर राजपथ का निर्माण करवाये। किन्तु इस चर्चा से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जो 150 लोग मारे गये और दो सौ घायल हुए उन्हें किसने मारा और किसके कारण ये लोग घायल हुए? निश्चय ही, वे स्वयँ अथवा वहां उपस्थित बीस हज़ार लोग ही इन सबकी मौत के अपराधी हैं। उपरान्त हादसे के सब लोग एक-दूसरे को रौंदकर घर की ओर जान बचाकर भाग चले। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उन्होंने किसके सिर अथवा पीठ पर पैर रखकर अपनी जान बचाई है। सम्भव है अपने ही माता-पिता, भाई-बहन अथवा किसी अन्य परिचित को रौंदकर ही वे अपने घर सुरक्षित पहुंचे हों। जो गिर गये उन्हें किसी ने नहीं उठाया क्योंकि यह तो सरकार का, पुलिस का, स्वयंसेवकों का कार्य है आम आदमी का नहीं, हमारा-आपका नहीं। हम-आप जो वहां बीस हज़ार की भीड़ के रूप में उपस्थित थे। किसी की जान बचाने का, घायल को उठाने का, मरे को मरघट पंहुचाने का हमारा दायित्व नहीं है। हम भीड़ बनकर किसी की जान तो ले सकते हैं, किन्तु किसी की जान नहीं बचा सकते। आग लगा सकते हैं, गाड़ियां जला सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, दुष्कर्म, लूट-पाट कर सकते हैं किन्तु उन व्यवस्थाओं एवं प्रबन्धनों में हाथ नहीं बंटा सकते जहां होम करते हाथ जलते हों। जहाँ कोई उपलब्धि नहीं हैं वहां कुछ क्यों किया जाये।
भंडारों में लाखों रुपये व्यय करके, देसी घी की रोटियां खिला सकते हैं, करोड़ों रुपयों की मूर्तियाँ,छत्र, सिंहासन दान कर सकते हैं, सड़क किनारे मार्ग अवरुद्ध करते हुए छबील लगा सकते हैं, भोजन बांट सकते हैं किन्तु ऐसे भीड़ वाले स्थानों पर होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए आपदा-प्रबन्धन में अपना योगदान देने में हम कतरा जाते हैं। धर्म के नाम पर दान मांगने वाले प्रायः आपका द्वार खटखटाते होंगे, मंदिरों के निर्माण के लिए, भगवती जागरण, जगराता, भंडारा, राम-लीला के लिए रसीदें काट कर पैसा मांगने में युवा से लेकर वृद्धों तक को कभी कोई संकोच नहीं होता, किन्तु किसी अस्पताल के निर्माण के लिए, शिक्षा-संस्थानों हेतु, भीड़-भीड़ वाले स्थानों पर आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था हेतु एक आम आदमी का तो क्या किसी बड़ी से बड़ी धार्मिक संस्था को भी कभी अपना महत्त योगदान प्रदान करते कभी नहीं देखा गया। किसी भी मन्दिर की सीढ़ियां चढ़ते जाईये और उस सीढ़ी पर किसी की स्मृति में बनवाने वाले का तथा जिसके नाम पर सीढ़ी बनवाई गई है, का नाम पढ़ते जाईये। ऐसे ही कितने नाम आपको द्वारों, पंखों, मार्गों आदि पर उकेरित भी मिल जायेंगे। किन्तु मैंने आज तक किसी अस्पताल अथवा विद्यालय में इस तरह के दानी का नाम नहीं देखा।
हम भीड़ बनकर तमाशा बना कते हैं, तमाशा देख सकते हैं, तमाशे में किसी को झुलसता देखकर आंखें मूंद लेते हैं क्योंकि यह तो सरकार का काम है।
अतिक्रमणः एक पक्ष
अतिक्रमण विरोधी दस्ते, नगर निगम अथवा प्रशासन जब लोगों के घर उजाड़ते हैं तो दुःख होता है। समाचार-पत्रों एवं टी.वी. चैनलों की भाषा में बात करें तो किसी का आशियाना उजड़ गया कोई बेघर हो गया, किसी के बर्तन सड़क पर बिखरे नज़र आये तो किसी के सिर से छत चली गई। सड़क पर बैठीं, घरों का बिखरा सामान समेटती रोती औरतों और भूख से बिलखते बच्चों को देखकर किसी का भी मन भर आता है। प्रशासन किसी का दुःख नहीं देखता।
अब इसी समस्या को दूसरी दृष्टि से देखें। ‘अतिक्रमण’ का क्या अर्थ है? किसी दूसरे की सम्पत्ति पर अनधिकार कब्ज़ा। दूसरे शब्दों में हम इसे सरकारी ज़मीन की चोरी कह सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की निजी ज़मीन पर अतिक्रमण होता है अथवा उसकी किसी वस्तु की चोरी होती है तो वह प्रायः दो-तीन उपाय करता है। अपनी सम्पत्ति की वापसी के लिए व्यक्तिगत प्रयास, पुलिस में रिपोर्ट एवं न्यायालय के माध्यम से; अर्थात् प्रशासन का सहयोग प्राप्त करता है। किन्तु यदि आम आदमी प्रशासन की ही सम्पत्ति की चोरी करता हो तो प्रशासन किसके पास जाये?
वस्तुतः अतिक्रमण एक चोरी है। और एक कड़वा सत्य यह कि यह चोरी प्रायः सामूहिक होती है। सड़क के किनारे बनी दुकानें एक ही पंक्ति में सड़कों पर निमार्ण बढ़ा लेती हैं और बीच में जो नहीं बढ़ाते हैं उनकी स्थिति गेहूं के साथ घुन पिसने जैसी होती है। फिर इन बढ़ी हुई दुकानों-मकानों के आगे छोटे खोखे और उनके आगे रेहड़ियां। सड़क तो नाम-मात्र की रह जाती है। हम अपनी भूमि अथवा सम्पत्ति के एक-एक इंच के लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं किन्तु सरकारी सम्पत्ति पर अनाधिकार कब्ज़ा करने में एक पल भी नहीं हिचकते। वर्तमान में सरकारी सम्पत्ति के हनन की एक मानसिकता बन चुकी है जिसका कोई बुरा भी नहीं मानता। कोई भी इसे हेय दृष्टि से नहीं देखता। न ही इसे चोरी अथवा अपराध का नाम दिया जाता है। घर के आगे सड़क पर बरामदे और साढ़ियां बनाना, छतें बढ़ाना, छज्जे बढ़ाना तो जनता का सार्वजनिक एवं सार्वजनीन अधिकार है। इसके अतिरिक्त सरकारी खाली पड़ी ज़मीन पर छोटा-सा मकान अथवा झोंपड़-पट्टियों का जाल फैलना तो एक आम-सी ही बात हो चुकी है। इस अतिक्रमण का यह कहकर समर्थन किया जाता है कि बेचारा गरीब आदमी क्या करे !
देश की आधी सड़कें तो इस अतिक्रमण की ही भेंट चढ़ चुकी हैं जो देश में ट्रैफ़िक जाम, गंदगी आदि का सबसे बढ़ा कारण हैं। नालों के उपर मकान अथवा दुकानें बढ़ा दी जाती हैं। परिणामस्वरूप नालों की सफाई नहीं हो पाती, जिस कारण धरती के भीतर और बाहर प्रदूषण बढ़ता है। पानी की निकासी नहीं होती, नालियां रुकती हैं और गंदगी एवं कूड़ा-कर्कट सड़कों पर स्थान बनाने लगते हैं। रोग पनपते हैं, पीने का पानी प्रदूषित हो जाता है, सड़क निमार्ण एवं अन्य विकास-कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। वर्षा ऋतु में सड़कें नदियाँ बन जाती हैं। ये सारी समस्याएं परस्पराश्रित हैं जिनके लिए हम प्रशासन को दोषी मानते हैं। यदि किसी विकास-कार्य अथवा निमार्ण के लिए प्रशासन के मार्ग में किसी की व्यक्तिगत एक इंच भूमि भी आ रही हो तो लोग देने के लिए तैयार नहीं होते। यदि सरकार किसी की भूमि लेती है तो बदले में लाखों -करोड़ों की प्रतिपूर्ति भी देती है और प्रायः बदले में ज़मीन अथवा अन्य सुविधाएं भी। किन्तु लोग फिर भी सन्तुष्ट नहीं होते।
अतिक्रमण एक अधिकार मान लिया गया है और इसके विरुद्ध कार्यवाही का अर्थ है सरकार की आम आदमी के प्रति दमन-नीति। तोड़-फोड़ करने से पूर्व प्रायः नोटिस दिये जाते हैं, चेतावनियां दी जाती है एवं समय भी। लोगों को यह अवसर भी दिया जाता है कि वे अपना सामन हटाकर स्वयं ही अनधिकृत निमार्ण तोड़ दें। किन्तु लोग अधिक समझदारी का प्रयोग करते हैं। समितियां बना ली जाती हैं संगठन खड़े कर लिए जाते हैं ओर लोग अपने बचाव में रैलियां, धरने, भूख-हड़ताल आदि करने लगते हैं। धरनों ओर रैलियों में महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया जाता है। महिलाओं की रोती सूरतें, बिलखते-भूखे बच्चों को दिखा-दिखाकर वे अपनी इस चोरी को मासूमियत के नीचे ढंकना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त लोगों के पास अपने इस अपराध को उचित ठहराने का सबसे बड़ा आधार है धर्म। घर के आस-पास अथवा दुकानों के बाहर धार्मिक स्थलों का अथवा प्रतीकों का निर्माण कर लिया जाता है। फिर इन स्थानों की तोड़-फोड़ को साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जाता है। महिलाएँ और बच्चे तो पहले ही अग्रिम पंक्ति में होते हैं। अंततः प्रशाासन को पुलिस बल का सहारा लेकर कार्यवाही करनी पड़ती है। जनता अपनी अनधिकृत सम्पत्ति पर अपने अधिकार को बचाये रखने के लिए प्रत्येक प्रयास करती है। परिणामस्वरूप लाठी चार्ज, आंसू गैस, बल-प्रयोग किया जाता है, जिस कारण लोगों का घायल होना एवं नुकसान होना स्वाभाविक ही है। तब पुलिस एवं प्रशाासन की निर्ममता की खूब चर्चा होती है। फिर नगर-निगम आज अनधिकृत निर्माण को तोड़कर जाता है, दो दिन बाद वहां फिर वही ढांचे दिखाई देने लगते हैं। इसके अतिरिक्त लोग संगठन बनाकर न्यायालय की शरण में चले जाते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि देश में न्याय की प्रक्रिया धीमी है और न्यायालय स्थगन आदेश तो दे ही देता है। इस प्रकार मामले वर्षों तक लटके रहते हैं। वैसे भी प्रशासनिक कार्यवाही एक लम्बी प्रक्रिया होती है जिसका लाभ सदा विरोधी पक्ष को ही मिलता है।
किन्तु इस अतिक्रमण रूपी चोरी की सीमा इतनी ही नहीं है। ‘सरकारी सम्पत्ति आपकी अपनी सम्पत्ति है’ यह वाक्य हम अनेक सार्वजनिक स्थानों पर पढ़ते हैं। जिसका अभिप्राय है कि सरकारी सम्पत्ति पर देश के प्रत्येक नागरिक का समान अधिकार है। अर्थात् यदि एक व्यक्ति सरकारी ज़मीन पर अनाधिकृत कब्ज़ा करता है तो वह देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों का हनन करता है, प्रत्येक नागरिक की सम्पत्ति का अनाधिकार प्रयोग करता है। जो सड़क एक सौ चालीस करोड़ लोगों की है उस पर एक व्यक्ति अधिकार कर लेता है और हम एक सौ चालीस करोड़ लोगों को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, हम देखकर चुपचाप निकल जाते हैं, कभी कोई आपत्ति नहीं करता। विपरीत प्रशासन द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने पर हम प्रशासन की ही निन्दा करते हैं।
इस समस्या का एक ही समाधान है और वह है प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना। प्रचार-प्रसार माध्यमों द्वारा जन-जागरण अभियान। इसके अतिरिक्त बिजली, पानी एवं भूमि-चोरी को दण्डनीय अपराध घोषित किया जाना चाहि
मेरे बाबाजी ऐसे क्यों न थे
मेरा यह आलेख उस समय का है जब मीडिया में तरह-तरह के बाबा छाये हुए थे, उनके पास खरीदा हुआ समय था, अपने चैनल थे, बहुत बड़ा प्रचार माध्यम था, जिनमें से आज कुछ कारागार में, कुछ की दुकानदारी बन्द हो चुकी है। किन्तु अपने समय में इन्होने जिन उंचाईयों को छुआ वे समझने वाली थीं। उस पर ही मेरी यह व्यंग्य रचना।
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
आजकल जब टी.वी. पर बाबाओं को देखती हूँ तो मन में एक हूक उठती है, मेरे बाबाजी ऐसे क्यों न थे? यह एक समय की बात है जब मेरे भी एक बाबाजी हुआ करते थे। वैसे मेरे एक नहीं पाँच- पाँच बाबा हुआ करते थे किन्तु मेरे एक भी बाबा ऐसे क्यों न थे यही मेरी पीड़ा है। मेरे बाबा अर्थात् मेरे पिता के पिता जिन्हें आजकल बड़े पा, दादू, दद्दा, बड़े डैड, सीनियर डैड वगैरह कहा जाता है उन्हें ही हमारे ज़माने में बाबाजी कहा जाता था। और फिर मेरे तो एक नहीं पाँच- पाँच बाबा थे। एक मेरे सगे बाबाजी और चार उनके भाई। और वे पाँचों एक ही घर में रहा करते थे। किन्तु मेरा दुख यह कि मेरे एक भी बाबाजी ऐसे क्यों न थे?
अब आप जानना चाहेंगे कि मेरे बाबाजी ‘ऐसे’ क्यों न थे अर्थात् ‘कैसे’ क्यों न थे? अब इसमें बताने की क्या बात है। आज जब मैं टी. वी. पर, समाचार-पत्रों में इन बाबाओं को देखती-सुनती हूँ तो मेरे मन में एक कसक पैदा होती है कि मेरे बाबाजी ऐसे क्यों न थे। मेरे बाबाजी - बड़े हुए, शादी कर ली, ईमानदारी का व्यवसाय किया, परिवार को ईमानदारी, सच्चाई, त्याग, सच्चरित्रता, आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया और यही सब कुछ विरासत में अपने परिवार को देकर चल बसे। अब आप ही बताईए कितना पीड़ादायक है ऐसे बाबा के परिवार का सदस्य होना।
एक मेरे बाबा थे और एक ये आजकल के बाबा हैं। हां, धोती-कुर्ता वे भी पहनते थे ये भी पहनते हैं। सच्चाई, ईमानदारी, त्याग, दान का महत्व वे भी समझाते थे और ये भी समझाते हैं। वे भी गांव में पैदा हुए थे और ये भी। किन्तु मेरे बाबाजी मिट्टी को ही सोना कहकर पुकारते रहे और ये मिट्टी में सोना गाढ़ते रहे। मेरे बाबाजी के कुर्ते के नीचे एक बंडी हुआ करती थी और इनके कुर्ते के नीचे बुलेट पू्रफ जैकेट। मेरे बाबाजी ने सारे उपदेश अपने पर थोप रखे थे और इन बाबाओें के उपदेश दूसरों को देने के लिए हैं।
काश! मेरे बाबाओं ने इन आधुनिक बाबाओं से कुछ सीखा होता तो आज हमारा जीवन कितना सुखी-सम्पन्न, आध्यात्मिक होता। एक मेरे बाबा थे छोटा-सा परिवार बसाया, उसके लिए कमाया और चल दिए। और एक ये बाबा हैं सारी दुनिया के लिए कमाते हैं। विवाह नहीं करते क्योंकि पूरा विश्व इनका परिवार है । इसी कारण इतना कमाते हैं कि पूरे विश्व का पालन-पोषण कर सकें; करें या न करें यह अलग बात है। हर गाँव, हर शहर, हर राज्य और और यहां तक कि विदेशों में भी इनके आवास हैं जिन्हें सम्मान से आश्रम कहा जाता है। अब ये आश्रम मेरे बाबाजी के पैतृक घर की तरह मिट्टी-गारे के तो होते नहीं, बायोमीट्रिक होते हैं। अब यह बायोमीट्रिक क्या होता है यह तो मुझे भी पता नहीं किन्तु कुछ तो ज़्यादा ही होता होगा तभी तो चर्चा का विषय बना हुआ है। द्वीपों पर भी इनका साम्राज्य है।
ये परिवार नहीं समर्थक और अनुयायी पैदा करते हैं। और मेरे पाँचों बाबाओं को देखो, एक ही घर में एक साथ रहते थे। अरे कोई उन्हें सद्बुद्धि देता। अपने-अपने आश्रम बनाते, क्षमा कीजिएगा अपने-अपने घर बनाते, अपनी-अपनी सम्पत्ति, अपनी-अपनी सत्ता, अपना-अपना धर्म और अपने-अपने अनुयायी। तब आज शायद मैं भी गर्व से अपने बाबाओं को स्मरण करती।
मेरे बाबाजी पैंतीस रुपये महीना कमाते थे और ये पैंतीस करोड़ के कमरे में रहते हैं। किसी के पास पचास हज़ार करोड़ की सम्पत्ति है तो किसी के पास ग्यारह हज़ार करोड़ की। जब भी एक नया कमरा खोला जाता है तो वहां कुछ किलो सोना-चांदी निकल आता है । इधर तो साड़ियाँ , विदेशी प्रसाधन का सामान और इस तरह का पता नहीं क्या-क्या सामान मिल रहा है। और दूसरी ओर मेरे बाबाजी तो तोले-माशे की बात करते ही चल बसे और यहां सोना-चांदी किलो में तोला जा रहा है। हमारी सारी आयु बीत गई उन किस्सों को सुनते-सुनते कि तुम्हारे बाबाजी ये हुआ करते थे वे हुआ करते थे। हमारे पास ये था हमारे पास वो था। उनके पास बैल थे, अपना टांगा-गाड़ी थी। घर के आगे आंगन था। अपनी ज़मीन-खेत थे। लेकिन ये बाबा करोड़ों के विमानों, वातानुकूलित गाड़ियों में यात्रा करते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ चाहें वहां सरकारी या गैर-सरकारी ज़मीन पर अपना पैर रखकर वैधानिक तौर पर उसे अपना बना लेते की ताकत रखते हैं। हमारे बाबा नून-तेल-लकड़ी में ही उलझे रहे किन्तु इन बाबाओं के अनुयायी इनकी नून-तेल-लड़की क्षमा कीजिए लड़की फिर ज़बान फ़िसल गई मेरा अभिप्राय है लकड़ी का प्रबन्ध करते हैं क्योंकि इन्हें तो अपने आश्रमों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों, क्रय-विक्रय, लाभ-हानि, नव-निर्माण, सम्पत्तियों-परिसम्पत्तियों का भी हिसाब रखना होता है। फिर देश-विदेश की यात्राएं, अनुयायियों, समर्थकों को निरन्तर दान देने के लिए प्रेरित करते रहना, राजनीतिक सम्पर्क बनाए रखना, शिविर लगा-लगाकर उपदेश दे-देकर लोगों को सार्वजनिक तौर पर लूटना जैसे कितने ही महत्वपूर्ण कार्य हैं इनके पास।
लेकिन मेरे बाबाजी ऐसे क्यों न थे?
भव्य रावण
क्यों हम
भूलना ही नहीं चाहते
रावण को।
हर वर्ष
कितनी तन्मयता से
स्मरण करते हैं
पुतले बनाते हैं
सजाते हैं
और उनके साथ
कुम्भकरण और मेघनाथ भी
आते हैं
अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित।
नवरात्रों और दशमी पर्व पर
सबसे पहले
रावण को ही
स्मरण करते हैं।
कितना बड़ा मैदान
कैसा मेला
कितने पटाखे
और कितने भव्य हों पुतले।
उस समय
स्मरण ही नहीं आता
कि इस पुतले को
बुराई के प्रतीक के रूप में
बना रहे हैं
जलाने के लिए।
राम और दुर्गा
सब पीछे छूट जाते हैं
और हम
दिनों-दिनों तक याद करते हैं
रावण को,
अह! कितना भव्य था इस बार।
कितनी रौनक थी
और कितना आनन्द आया।
धन-दौलत जीवन का आधार
धन-दौलत पर दुनिया ठहरी, धन-दौलत से चलती है
जीवन का आधार है यह, सुच्ची रोटी इसी से बनती है
छल है, मोह-माया है, चाह नहीं, कहने की बातें हैं
नहीं हाथ की मैल है यह, श्रम से सबको फलती है।
असली-नकली की पहचान कहाँ
पीतल में सोने से ज़्यादा चमक आने लगी है
सत्य पर छल-कपट की परत चढ़ने लगी है
असली-नकली की पहचान कहाँ रह गई अब
बस जोड़-तोड़ से अब ज़िन्दगी चलने लगी है।
तीर और तुक्का
एक बार आसमां पर तीर जरूर तानिए
लौटकर आयेगा, प्रभाव, उसका जानिए
तीर के साथ तुक्के का ध्यान भी रखें
नहीं तो तरकस खाली होगा, यह मानिए
वरदान और श्राप
किसी युग में
वरदान और श्राप
साथ-साथ चलते थे।
वरदान की आशा में
भक्ति
और कठोर तपस्या करते थे
किन्तु सदैव
कोई भूल
कोई चूक
ले डूबती थी
सब अच्छे कर्मों को
और वरदान से पहले
श्राप आ जाता था।
और कभी-कभी
इतनी बड़ी गठरी होती थी
भूल-चूक की
कि वरदान तक
बात पहुँच ही नहीं पाती थी
मानों कोई भारी
बैरीकेड लगा हो।
श्राप से वरदान टूटता था
और वरदान से श्राप,
काल की सीमा
अन्तहीन हुआ करती थी।
और एक खतरा
यह भी रहता था
कि पता नहीं कब वरदान
श्राप में परिवर्तित हो जाये
और श्राप वरदान में
और दोनों का घालमेल
समझ ही न आये।
-
बस
इसी डर से
मैं वरदान माँगने का
साहस ही नहीं करती
पता नहीं
भूल-चूक की
कितनी बड़ी गठरी खुल जाये
या श्राप की लम्बी सूची।
-
जो मिला है
उसमें जिये जा
मज़े की नींद लिए जा।
भीड़ पर भीड़-तंत्र
एक लाठी के सहारे
चलते
छोटे कद के
एक आम आदमी ने
कभी बांध ली थी
सारी दुनिया
अपने पीछे
बिना पुकार के भी
उसके साथ
चले थे
लाखों -लाखों लोग
सम्मिलित थे
उसकी तपस्या में
निःस्वार्थ, निःशंक।
वह हमें दे गया
एक स्वर्णिम इतिहास।
आज वह न रहा
किन्तु
उसकी मूर्तियाँ
हैं हमारे पास
लाखों-लाखों।
कुछ लोग भी हैं
उन मूर्तियों के साथ
किन्तु उसके
विचारों की भीड़
उससे छिटक कर
आज की भीड़ में
कहीं खो गई है।
दीवारों पर
अलंकृत पोस्टरों में
लटक रही है
पुस्तकों के भीतर कहीं
दब गई है।
आज
उस भीड़ पर
भीड़-तंत्र हावी हो गया है।
.
अरे हाँ !
आज उस मूर्ति पर
माल्यार्पण अवश्य करना।
ब्लॉक
कब सालों-साल बीत गये
पता ही नहीं लगा
जीवन बदल गया
दुनिया बदल गई
और मैं
वहीं की वहीं खड़ी
तुम्हारी यादों में।
प्रतिदिन
एक पत्र लिखती
और नष्ट कर देती।
अक्सर सोचा करती थी
जब मिलोगे
तो यह कहूँगी
वह कहूँगी।
किन्तु समय के साथ
पत्र यादों में रहने लगे
स्मृतियाँ धुँधलाने लगी
और चेहरा मिटने लगा।
पर उस दिन फ़ेसबुक पर
अनायास तुम्हारा चेहरा
दमक उठा
और मैं
एकाएक
लौट गई सालों पीछे
तुम्हारे साथ।
खोला तुम्हारा खाता
और चलाने लगी अंगुलियाँ
भावों का बांध
बिखरने लगा
अंगुलियाँ कंपकंपान लगीं
क्या कर रही हूँ मैं।
इतने सालों बाद
क्या लिखूँ अब
ब्लॉक का बटन दबा दिया।
दिल घायल
लोग कहते हैं
किसी की बात गलत हो
तो
एक कान से सुनो
दूसरे से निकाल दो।
किन्तु क्या करें
हमारे
दोनों कानों के बीच में
कोई सुंरग नहीं है
बात या तो
सीधी दिमाग़ में लगती है
अथवा
दिल घायल कर जाती है
अथवा
दोनों को तोड़ जाती है।
दिल का दिन
हमें
रचनाकारों से
ज्ञात हुआ
दिल का भी दिन होता है।
असमंजस में हैं हम
अपना दिल देखें
या सामने वाले का टटोलें।
एक छोटे-से दिल को
रक्त के आवागमन से
समय नहीं मिलता
और हम, उस पर
पता नहीं
क्या-क्या थोप देते हैं।
हर बात हम दिल के नाम
बोल देते हैं।
अपना दिल तो आज तक
समझ नहीं आया
औरों के दिलों का
पूरा हिसाब रखते हैं।
दिल टूटता है
दिल बिखरता है
दिल रोता है
दिल मसोसता है
दिल प्रेम-प्यार के
किस्से झेलता है।
विरह की आग में
तड़पता है
जलता है दिल
भावों में भटकता है दिल
सपने भी देखता है
ईष्र्या-द्वेष से भरा यह दिल
न जाने
किन गलियों में भटकता है।
तूफ़ान उठता है दिल में
ज्वार-भाटा
उछालें मारता है।
वैसे कभी-कभी
हँसता-गाता
गुनगुनाता, खिलखिलाता
मस्ती भी करता है।
कैसा है यह दिल
नहीं सम्हलता है।
और इतने बोझ के बाद
जब रक्त वाहिनियों में
रक्त जमता है
तब दिमाग खनकता है।
यार !
जिसे ले जाना है
ले जाओ मेरा दिल
हम
बिना दिल ही
चैन की नींद सो लेंगे।
नौ दिन बीतते ही
वर्ष में
बस दो बार
तेरे अवतरण की
प्रतीक्षा करते हैं
तेरे रूप-गुण की
चिन्ता करते हैं
सजाते हैं तेरा दरबार
तेरे मोहक रूप से
आंखें नम करते हैं
गुणगान करते हैं
तेरी शक्ति, तेरी आभा से
मन शान्त करते हैं।
दुराचारी
प्रवृत्तियों का
दमन करते हैं।
किन्तु
नौ दिन बीतते ही
तिरोहित कर
भूल जाते हैं
और लौट आते हैं
अपने चिर-स्वभाव में।
अमूल्य धन
कुछ हँसती, खिलखिलाती, गुनगुनाती स्मृतियाँ अनायास मानस पटल पर आयें, अच्छा लगता है। इन सिक्कों को देखकर सालों-साल पुरानी एक घटना मानस-पटल पर उभर आई।
वर्ष 1974
एम.ए. का प्रथम वर्ष।
उस समय इन सिक्कों का कितना महत्व होता था यह तो आप भी जानते ही होंगे। रुपये खर्च करना तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। जेब-खर्च के लिए भी पचास पैसे, ज़्यादा से ज़्यादा एक रुपया जो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकर घर से निकलते थे। पांच रुपये में तीन महीने का लोकल पास बनता था, शिमला रेलवे स्टेशन से समरहिल का, जहाँ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है।
मैं हिन्दी में एम. ए. और कर रही थी और मेरी एक सखी संस्कृत में। हमें ज्ञात हुआ कि बी.ए. के विषयानुसार विश्वविद्यालय में अधिकतम अंक प्राप्त होने के कारण हम दोनों को 150 रूपये मासिक छात्रवृत्ति मिलेगी।
हमारे लिए तो जैसे यह कुबेर का खजाना था। 6-6 महीने की राशि एकसाथ मिलनी थी। हमें कार्यालय से 900-900 रुपये के चैक मिले। पहले तो वे ही हमारे लिए एक अद्भुत अमूल्य पत्र थे, जिसे हम ऐसे देख और सम्हाल रहे थे मानों कहीं हाथ लगने से भी गल न जायें।
उपरान्त हम दोनों विश्वविद्याय परिसर में ही स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में डरते-डरते गईं।
वहाँ के कर्मचारियों का शायद हम जैसे विद्यार्थियों से सामना होता ही होगा। हम दोनों कांउटर पर डरते-डरते गईं और कहा कि पैसे लेने हैं। हम दोनों ने चैक उनके सामने रख दिये।
कर्मचारी हमारी उत्तेजना और उत्सुकता भांप गया और पूछा कौन से पैसे चाहिए आपको?
हम दोनों ही अचानक बोल बैठीं, रेज़गारी दे दीजिए।
रेज़गारी? 900 रुपये की?
और क्या, लेकर निकलेंगे तो किसी को पता तो लगेगा कि हमें छात्रवृत्ति मिली है, कोई तो पूछेगा कि आपके पास यह क्या है?
कर्मचारी हँसने लगा 1800 रुपये की रेज़गारी तो हमारे पास नहीं है, यदि यही चाहिए तो आप डिमांड दे जाईये, रिज़र्व बैंक से मंगवा देंगे।
नहीं, नहीं, आप नोट ही दे दीजिए।
और इस तरह हम 900-900 रूपये के नोट लेकर वहाँ से सीधे माल रोड आ गईं। उस समय नोट भी बड़े आकार के होते थे।
दो घंटे से भी ज़्यादा समय तक मालरोड के चक्कर काटे, कितने अपने मिले, लेकिन किसी ने हमारे मन की बात नहीं पूछी।
मालरोड पर जो भी परिचित मिले, हम यहीं सोचें कि यह ज़रूर पूछेंगे कि भई आपके बैग आज भारी लग रहे हैं क्या है इनमें।
लेकिन किसी ने नहीं पूछा। और हम घर लौट आईं, मायूस, उदास। छात्रवृत्ति मिलने का सारा आनन्द किरकिरा हो गया।
पशु-पक्षियों का आयात-निर्यात
अभयारण्य
बड़े होते जा रहे हैं
हमारे घर छोटे।
हथियार
ज़्यादा होते जा रहे हैं
प्रेम-व्यवहार ओछे।
पढ़ा करते थे
हम पुस्तकों में
प्रकृति में पूरक हैं
सभी जीव-जन्तु
परस्पर।
कौन किसका भक्षक
कौन किसका रक्षक
तय था सब
पहले से ही।
किन्तु
हम मानव हैं
अपने में उत्कृष्ट,
प्रकृति-संचालन को भी
ले लिया अपने हाथ में।
पहले वन काट-काटकर
घर बना लिए
अब घरों में
वन बना रहे हैं
पौधे तो
रोपित कर ही रहे थे
अब पशु-पक्षियों के
आयात-निर्यात करने का
समय आ गया है।
बेटियाँ धरा पर
माता-पिता तो
देना चाहते हैं
आकाश
अपनी बेटियों को
किन्तु वे
स्वयं ही
नहीं जान पाते
कब
उन्होंने
अपनी बेटियों के
सपनों को
आकाश में ही
छोड़ दिया
और उन्हें
उतार लाये
धरा पर
यादें: शिमला की बारिश की
न जाने वे कैसे लोग हैं
जो बारिश की
सौंधी खुशबू से
मदहोश हो जाते हैं
प्रेम-प्यार के
किस्सों में खो जाते हैं।
विरह और श्रृंगार की
बातों में रो जाते हैं।
सर्द सांसों से
खुशियों में
आंसुओं के
बीज बो जाते हैं।
और कितने तो
भीग जाने के डर से,
घरों में छुपकर सो जाते हैं।
यह भी कोई ज़िन्दगी है भला !
.
कभी तेज़, कभी धीमी
कभी मूसलाधार
बेपरवाह हम और बारिश !
पानी से भरी सड़क पर
छप-छपाक कर चलना
छींटे उछालना
तन-मन भीग-भीग जाना
चप्पल पानी में बहाना
कभी भागना-दौड़ना
कभी रुककर
पेड़ों से झरती बूँदों को
अंजुरी में सम्हालना
बरसती बूंदों से
सिहरती पत्तियों को
सहलाना
चीड़-देवदार की
नुकीली पत्तियों से
झरती एक-एक बूँद को
निरखना
उतराईयों पर
तेज़ दौड़ते पानी से
रेस लगाना।
और फिर
रुकती-रुकती बरसात,
बादलों के बीच से
रास्ता खोजता सूरज
रंगों की आभा बिखेरता
मानों प्रकृति
नये कलेवर में
अवतरित होती है
एक नवीन आभा लिए।
हरे-भरे वृक्ष
मानों नहा-धोकर
नये कपड़े पहन कर
धूप सेंकने आ खड़े हों।
स्मृतियों के खण्डहर
कुछ
अनचाही स्मृतियाँ
कब खंडहर बन जाती हैं
पता ही नहीं लग पाता
और हम
उन्हीं खंडहरों पर
साल-दर-साल
लीपा-पोती
करते रहते हैं
अन्दर-ही-अन्दर
दीमक पालते रहते हैं
देखने में लगती हैं
ऊँची मीनारें
किन्तु एक हाथ से
ढह जाती हैं।
प्रसन्न रहते हैं हम
इन खंडहरों के बारे में
बात करते हुए
सुनहरे अतीत के साक्षी
और इस अतीत को लेकर
हम इतने
भ्रमित रहते हैं
कि वर्तमान की
रोशनियों को
नकार बैठते हैं।
जीवन की नवीन शुरुआत
जीवन के कुछ पल
अनमोल हुआ करते हैं,
बड़ी मुश्किल से
हाथ आते हैं
जब हम
सारे दायित्वों को
लांघकर
केवल अपने लिए
जीने की कोशिश करते हैं।
नहीं अच्छा लगता
किसी का हस्तक्षेप
किसी का अपनापन
किसी की निकटता
न करे कोई
हमारी वृद्धावस्था की चिन्ता
हमारी हँसी-ठिठोली में
न बने बाधा कोई
न सोचे कोई हमारे लिए
गर्मी-सर्दी या रोग,
अब लेने दो हमें
टेढ़ेपन का आनन्द
ये जीवन की
एक नवीन शुरुआत है।
पवित्रता के मापदण्ड
पवित्रता के
मापदण्ड होते हैं
कहीं कम
कहीं ज़्यादा होते हैं।
लेकिन हर
किसी के लिए
नहीं होते हैं।
फिर
तोलते हैं
न जाने
किस तराजू में
हर बार
नये-नये माप
और दण्ड होते हैं।
जानती हूँ
अधिकांश को
मेरी यह बात
समझ नहीं आई होगी
क्योंकि
युगों-युगों से
बन रहे
इन माप और दण्डों को
आज तक
कौन समझ पाया है
जिसके माथे जड़े हैं
वह भी
वास्तविकता
कहाँ जान पाया है।
अहं सर्वत्र रचयिते : एक व्यंग्य
हम कविता लिखते हैं।
कविता को गज़ल, गज़ल को गीत, गीत को नवगीत, नवगीत को मुक्त छन्द, मुक्त छन्द को मुक्तक और चतुष्पदी बनाना जानते हैं। और इन सबको गद्य की विविध विधाओं में परिवर्तित करना भी जानते हैं।
अर्थात् , मैं ही लेखक हूँ, मैं ही कवि, गीतकार, गज़लकार, साहित्यकार, गद्य-पद्य की रचयिता, , प्रकाशक, मुद्रक, विक्रेता, क्रेता, आलोचक, समीक्षक भी मैं ही हूँ।
मैं ही संचालक हूँ, मैं ही प्रशासक हूँ।
सब मंचों पर मैं ही हूँ।
इस हेतु समय-समय पर हम कार्यशालाएँ भी आयोजित करते हैं।
अहं सर्वत्र रचयिते।
भारत
मुझे गहन आश्चर्य हुआ कि मैंने जब भी किसी को “भारत” पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा तो जो विचार मुझे मिले उनका सारांश यह था कि भारत एक अत्यन्त प्राचीन, सभ्यता-संस्कृति-सम्पन्न, वेद, पुराण, गीता, रामायण, कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, नानक आदि की धरती है यह। कुछ ऐसे ही कथन और वक्तव्य का समापन। कुछ लोगों ने इससे आगे बढ़कर आज़ादी और शहीदों की बात की। आज़ादी के वीरों के नाम और उनको नमन।
और जो वर्तमान में थे, उन्होंने भ्रष्टाचार, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों, रिश्वतखोरी, बिखरते पारिवारिक सम्बन्धों, वर्तमान में भटकी हुई, स्वार्थान्धता में जीती युवा पीढ़ी, आधुनिक नार, आदि के बारे में ही बात की।
मैं चकित !
क्या हमारा भारत बस यहीं तक सीमित है ? जब हम भारत के बारे में बात करते हैं तो इससे आगे कहने के लिए क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है? आश्चर्य होता है।
यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम एक संस्कृति-सम्पन्न प्राचीन राष्ट्र के नागरिक हैं। वे, जो हमें आज़ादी के भारत में जीवन दे गये, नमन्य हैं।
किन्तु क्या भारत इतना ही है?
आज हम एक स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर, सुशिक्षित, साधन सम्पन्न, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, गणतन्त्र, विकसित भारत के नागरिक हैं। भारत एक विकासशील नहीं विकसित देश है। भारतीय नागरिक के पास सर्वाधिक मौलिक अधिकार हैं। सूचना का अधिकार है। यह विश्व का एकमात्र देश है जहां धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वतन्त्रता है, धर्म, जाति, क्षेत्र से इतर। जल, थल और नभ तीनों क्षेत्रों पर हमारी सेनाओं का अधिकार है। भारत ऐसा पहला देश है जिसने अपनी संचार प्रणाली के लिए स्वदेशी सैटेलाईट का निर्माण किया।
चांद तक की यात्रा भारत ने तय कर ली है। स्वविकसित परमाणु उर्जा से सम्पन्न राष्ट्र होने का गौरव हमें प्राप्त है। विश्व की सवार्धिक 325 भाषाएं तथा 1650 बोलियां भारत में बोली जाती हैं। जिसमें से 29 भाषाएं संविधान में स्वीकृत हैं।
विश्व की चैथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। भारत में जीवन की औसत आयु 32 वर्ष से बढ़कर 65 वर्ष हो गई है। भारतीय नागरिक को आधुनिक सुख सुविधाओं से सम्पन्न जीवन मिला है।
1951 में शिक्षा की दर मात्र 18.23 प्रतिशत थी जो वर्तमान में 77.8 प्रतिशत से भी अधिक हो चुकी है। देश में लगभग 1000 विश्वविद्यालय तथा 45,000 महाविद्यालय हैं। इनके अतिरिक्त लगभग 1500 अन्य क्षेत्रों के उच्च शिक्षा संस्थान हैं। विदेशों से लाखों विद्यार्थी भारत में शिक्षा ग्रहण करने के आते हैं। चिकित्सा की आयुर्वेद पद्धति एवं योग के लिए पूरा विश्व भारत के समक्ष नतमस्तक है।
विश्व के सबसे अधिक समाचार पत्र भारत में प्रकाशित होते हैं।
विश्व में सबसे अधिक दोपहिया वाहनों का निर्माण भारत में होता है। दुग्ध एवं मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीनी उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे नम्बर पर तथा कपास के क्षेत्र में तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का 90 प्रतिशत हीरे तराशने का कार्य भारत में होता है। विश्व के सर्वाधिक बैंक खाते तथा डाकघर भारत में हैं।
विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला भारत में कुम्भ का मेला आयोजित होता है जिसमें लगभम 30 करोड़ लोग हिस्सा लेते हैं।
देश ने सर्वांगीण विकास किया है। आज विश्व की निर्भरता भारतीय वैज्ञानिक, चिकित्सक, इंजीनीयर, आई टी, व्यवसायी, पत्रकार, समाजसेवी, सब पर बढ़ी है।
विश्व के बड़े-बड़े देश आज भारतीय मेधा पर आश्रित हैं। डाक्टर, इंजीनियर, आई.टी, के क्षेत्र में पूरे विश्व में भारतीयों की धाक है।
मेरे प्रस्तुत आंकड़े पुराने हो सकते हैं, और इनमें और भी बढ़ोतरी निश्चित रूप से हुई होगी।
फिर भारत के बारे में बात करते हुए हमारा ध्यान इस ओर क्यों नहीं जाता?
यदि कुछ अच्छा नहीं है तो उस पर विचार करें, समाधान का प्रयास करें, अपना सहयोग दें और जो अच्छा है उसकी अधिक से अधिक चर्चा करें, सकारात्मक वातावरण बनायें।
बरसात की एक शाम
बरसात की तो हर शाम ही सुहानी होती है किन्तु कोई-कोई यादों में बसी रह जाती है। और शिमला की बरसात का तो कहना ही क्या, वो कहते हैं न बिन बादल बरसात।
शिमला में सांय माल रोड पर घूमने का हर स्थानीय निवासी को चस्का लगा हुआ होता था। आफ़िस से निकलकर घर जाने से पहले माल रोड के चार-पांच चक्कर तो लगा ही लेते थे। स्कैंडल प्वाईंट से शेरे पंजाब तक। भारी भीड़ किन्तु मज़ाल है कोई किसी से टकरा जाये अथवा कोई यह कहे कि देखो कैसे घूम रहे हैं। और चलते-चलते बालज़ीस का कोण या गरमागरम गुलाबजामुन खाने का आनन्द ही अलग होता था।
उस दिन संध्या समय अचानक मूसलाधार बरसात होने लगी किन्तु हम ठहरे देसी, तेज़ बरसात में बिना छाता ही चलती रहीं हम पांच सखियाँ। सर से पैर तक भीगती हुईं। सीधे बालज़ीस के आगे जाकर रुकीं और उसे फ़टाफ़ट पांच प्लेट गरम गुलाबजामुन का आदेश दिया। वहाँ पहले से चार लड़के खड़े थे, उन्होंने भी गुलाबजामुन का आर्डर दिया था किन्तु दुकानदार ने हमें पहले दे दिये जिससे वे कुछ नाराज़ तो हुए किन्तु बोले कुछ नहीं। उनके हाथ में भी प्लेटें आ चुकी थीं किन्तु वे हमें ही देखे जा रहे थे। हम पांचों ने आंखों में इशारा किया और एक-एक टुकड़ा खाते ही मुँह बनाया और ज़ोर से बोलीं ‘‘हाय! बिल्कुल ठण्डे !!’’ हमें देखते हुए और हमारी बात सुनकर उनमें से तीन ने पूरा-पूरा गुलाबजामुन ही मुँह में डाल लिया और चिल्लाने लगे अरे, इतना गर्म, मुँह जल गया !! पानी, पानी!! हमारा हँस-हँसकर बुरा हाल।