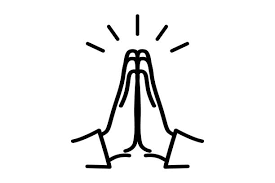संस्मरण: धर्मशाला साहित्यिक आयोजन
26 नवम्बर। धर्मशाला। पर्वत की गूंज द्वारा प्रकाशित हिमतरु दशहरा-दीपावली विशेषांक के लोकार्पण का अवसर। इसमें मेरा भी एक आलेख है। रेडियो गुंजन सिद्धवाड़ी धर्मशाला। एक सुखद अनुभव।
पर्वत की गूंज के संस्थापक, संचालक राजेन्द्र पालमपुरी जी का एक संदेश मिला कि धर्मशाला में इस हेतु एक छोटा-सा आयोजन है । यदि मैं आना चाहूं। मेरा विचार था कि आयोजन छोटा या बड़ा नहीं होता, अच्छा होता है और अच्छे लोगों से, अच्छे साहित्यकारों से मिलने के लिए होता है।
इसलिए कार्यक्रम बना लिया। ठहरने की व्यवस्था के लिए पालमपुरी जी से ही अनुरोध किया। कैलाश मनहास जी ने Dadhwal Bnb homestay में रहने की व्यवस्था करवाई। बहुत ही अच्छी।
बहुत सुन्दर, सादगीपूर्ण एवं गरिमामयी आयोजन का हिस्सा बनकर मन को बहुत अच्छा लगा। एक अपनत्व भरा कार्यक्रम। कुछ पहाड़ी कविताएं भी सुनने को मिलीं। पहाड़ी कविताओं को सुनने का अपनी ही आनन्द है। अनेक बाल कवि हिमाचल के विभिन्न भागों से उपस्थित थे और उन्हें भी सम्मानित किया गया। शायद 1990 के बाद हिमाचल में किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। शिमला मेरे भीतर बसता है और हिमाचल मुझे आकर्षित करता है। इसलिए इस अवसर को तो मैं जाने ही नहीं देना चाहती थी। इस सुन्दर आयोजन के लिए सभी मनीषियों का धन्यवाद एवं आभार।
छन्दमुक्त कविताएॅं
मैं किसी विवादास्पद विषय पर लिखने अथवा प्रतिक्रिया से बचकर चलती हूं। किन्तु कभी-कभी कुछ चुभ भी जाता है। फ़ेसबुक पर हम सब लिखने के लिए स्वतन्त्र हैं। किन्तु इतना भी न लिखें कि सीधे-सीधे अनर्गल आक्षेप हों। कुछ अति के महान लेखक यहां विराजमान हैं। सैंकड़ों मंचों के सदस्य हैं, सैंकड़ों सम्मान प्राप्त हैं। सुना है और उनकी बातों से लगता है कि वे महान छन्द विधाओं में लिखते हैं और उनसे बड़ा कोई नहीं। इस कारण वे सामूहिक रूप से किसी का भी, विशेषकर महिलाओं का अपमान कर सकते हैं। आपकी मित्र-सूची में भी होंगे, पढ़िए उनका लेख और अपने विचार दीजिए। मुझे लगता है इन महोदय को बड़े दिन से कोई सम्मान नहीं मिला अथवा किसी काव्य समारोह का निमन्त्रण तो भड़ास तो कहीं निकालनी ही थी। और ऐसे महान छन्दलेखक की भाषा! वाह!!! वे इतने महान हैं कि वे तय करेंगे कि कौन कवि है और कौन कवि नहीं।
वैसे वाह-वाही पाने और हज़ारों लाईक्स पाने का भी यह एक तरीका आजकल फ़ेसबुक पर चल रहा है कि आप जितना ही अनर्गल लिखेंगे उतने ही लाईक्स मिलेंगे।
वे लिखते हैं
“आज अगर यह मुक्त छंद वाली कविता या उल जुलूल बेसिर पैर के गद्य को कविता की श्रेणी से निकाल दिया जाय तो 90 प्रतिशत कवि इस सोशल मीडिया से गायब हो जायेंगे जिनमें 80 प्रतिशत महिला कवियत्री औऱ बाकी के पुरुष कवि कहलाने वाले लोग हैं ।”
छंद मुक्त लेखकों या अगड़म बगड़म गद्य को इधर इधर करके कविता नाम देने वाले स्त्री पुरुषों को तो मैं कवियों की श्रेणी में रखता ही नहीं ।
आप ऐसे समझिये कि जिसको कुछ नहीं आता, वह छंदमुक्त के नाम से लेखन कर कवि बन जाता है ।
जैसे जिसको कुछ नहीं आता या जिसमें कोई गुण नहीं, तो उससे कहा दिया जाता है कि चलो तुम laterine ही साफ कर दो ।“”
मैं मान लेती हूं कि छन्दमुक्त लिखने वाले कवि नहीं हैं तो सबसे पहले तो निराला, अज्ञेय, मुक्तिबोध, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह, केदारनाथ सिंह, धूमिल, कुमार विमल, गिरिजाकुमार माथुर आदि अनेक कवियों को हिन्दी साहित्य से बाहर कर देना चाहिए।
महिलाओं के परिधान
हमारे समाज में महिलाओं के परिधान की अनेक तरह से बहुत चर्चा होती है। वय-अनुसार, पारिवारिक पोस्ट के अनुसार, अर्थात अविवाहित युवती, भाभी, ननद, बहन, माँ, दादी आदि के लिए। इसके अतिरिक्त भारत में रीति-परम्पराओं, राज्यानुसार प्रचलित, एवं धार्मिक आख्यानों में भी इतनी विविधता है कि उसके अनुसार भी महिलाओं के वस्त्रों पर दृष्टि रहती है।
और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे आधुनिक समाज में महिलाओं के परिधानों के अनुसार ही उनका चरित्र-चित्रण किया जाता है। आधुनिक वस्त्र धारण करने वाली युवती के लिए मान लिया जाता है कि यह बहुत तेज़ होगी, घर-गृहस्थी के योग्य नहीं होगी, पति, सास-ससुर की सेवा करने वाली नहीं होगी। ( किन्तु जब महिलाओं की बात होती है तब सेवा-भाव वाली बात आती ही क्यों है, उसके अपने अस्तित्व की बात क्यों नहीं की जाती। परिवार के सदस्य की बात क्यों नहीं आती?, पुरुषों के सन्दर्भ में तो इस तरह की बात कभी नहीं आती। इस विषय पर चर्चा को विराम देती हूँ, यह भिन्न चर्चा का विषय है।)
किन्तु पुरुषों के परिधान, वस्त्रों पर कभी कोई बात नहीं करता।
क्योंकि महिलाएं खुलेआम टिप्पणी नहीं कर पातीं इस कारण कहती नहीं।
सबसे बुरा लगता है जब पुरुष केवल अन्तर्वस्त्रों में अथवा तौलिए में प्रातःकाल बरामदे में घूमते दिखते हैं। गर्मियों में तो जैसे उनका अधिकार होता है अर्द्धनग्न रहना। मुझे नहीं पता कि उनके घर की महिलाएं उन्हें टोकती हैं अथवा नहीं।
मैं शिमला से हूँ। वहां हमने सदैव ही यही देखा है कि पुरुष भी महिलाओं की भांति स्नानागार से पूरे वस्त्रों में ही तैयार होकर निकलते हैं। किन्तु जब मैं यहां आई तो मुझे बहुत शर्म आती थी कि घर के बच्चे क्या, युवा, अधेड़, बुजुर्ग सब आधे-अधूरे कपड़ों में घूमते हैं। हमें यह अश्लील लगता है। अभिनेत्रियों के वस्त्रों पर भी बहुत कुछ लिखा जाता है किन्तु जब बड़े.बड़े मंचों पर बड़े नामी कलाकार नग्न प्रदर्शन करते हैं तब वह भव्यता होती है। इन नग्नता की तुलना हम किसी कार्य या खेल में पहने जाने वस्त्रों से नहीं कर सकते।
पुरुष की वस्त्रहीनता उसका सौन्दर्य है और स्त्री के देह-प्रदर्शनीय वस्त्र अश्लीलता।
सबसे बड़ी बात जो मुझे अचम्भित भी करती है और हमारे समाज की मानसिकता को भी प्रदर्शित करती है वह यह कि हमारे प्रायः सभी प्राचीन पात्रों के चित्रों में उपरि वस्त्र धारण नहीं दिखाये जाते। फिर वह चित्रकारी हो अथवा अभिनय। किसने देखा है वह काल कि ये लोग उपरि वस्त्र पहनते थे अथवा नहीं। क्यों यह अश्लीलता नहीं दिखती और कभी भी क्यों इस पर आपत्ति नहीं होती। निश्चित रूप से उस युग को तो किसी ने नहीं देखा, यह हमारी ही मानसिकता का प्रतिफल है। किसने देखा है कि पौराणिक, अथवा अनदेखे काल के लोग कैसे वस़्त्र पहनते थे, क्या पहनते थे। यह उस कलाकार की अथवा भक्त की मानसिकता है जो अपने आराध्य की सुन्दर, सुघड़ देहयष्टि दिखाना चाहता है।
महिलाएं पुरुषों के पहनावे से आहत होती हैं। प्रकृति ने पुरुष को छूट दी है, यह हमारी सोच है। मुझे आश्चर्य तब होता है जब हम महिलाएं भी उसी बनी.बनाई लीक पर चलती हैं।
एक अन्य तथ्य यह कि जब भी भारतीय संस्कृति, परम्पराओं, रीति-रिवाज़ों के अनुसार पहनावे की बात उठती है तब केवल महिलाओं के सन्दर्भ में ही चर्चा होती है, पुरुषों के पहरावे पर कोई बात नहीं की जाती।
इतना और कहना चाहूंगी कि कमी पुरुषों की मानसिकता में नहीं महिलाओं की मानसिकता में है जो पुरुष नग्नता का विरोध नहीं करतीं।
महिलाओं का सम्मान
जब मैं महिलाओं के सम्मान में कोई आलेख अथवा रचना पढ़ती हूं तो मेरा मन गद्गद् हो उठता है। कितना बता नहीं सकती। हमारा समाज महिलाओं के संस्कारों, संस्कृति, उनकी सुरक्षा, पवित्रता और ऐसे ही कितने शब्द जो मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहे, मेरा शब्दकोष संकुचित हो गया है, मेरे स्मृति-कक्ष में उभर आते हैं और मैं आनन्दित होने लगती हूं।
आप जानना चाहेंगे और न भी जानना चाहें तो भी मैं बताना चाहूंगी कि आज मेरा मन इतना आनन्दित क्यों है।
आज एक परम मित्र लेखक महोदय का ऐसा ही एक आलेख अथवा एक संक्षिप्त टिप्पणी पढ़ने के लिए मिली जो महिलाओं के बारे में बहुत विचारात्मक एवं उनके प्रति चिन्ता करते हुए लिखी गई थी। अब मैं तो मैं हूं, सीधी बात तो समझ ही नहीं आती।
======-======
उनका कथन है
नदियों अथवा पवित्र कुंड़ या सरोवरों पर स्नान के समय अपने परिवार की महिलाओं को पूरे वस्त्र के साथ स्नान करने हेतु कहें। महिलाएं स्वयं इस बात का संज्ञान लें और कम वस्त्र नहींए पूरे वस्त्र के साथ स्नान करें। अब सरकार या सामाजिक संस्थाओं द्वारा वस्त्र बदलने के लिए लगभग हर जगह सुविधाएं दी गई हैं। उनका उपयोग करें।
======-=====
दुर्भाग्यवश ही कह सकती हूं, मैं कुछ समय पूर्व ही दो बार हरिद्वार गई। दोनों ही बार एक तो शनिवार अथवा रविवार था और साथ ही एक बार अमावस्या थी और दूसरी बार गंगा-दशहरा। अर्थात भीड़ ही भीड़, लाखों लोग। पहली बार हमने अपने गंतव्य से बहुत दूर गाड़ी पार्क कर दी जिस कारण हमें हर की पौड़ी पर पैदल ही बहुत चलना पड़ा। मुख्य स्थल जहां स्नान की व्यवस्था है, वहां हमारा जाना हुआ। हम लोग वहां लगभग एक घंटा अथवा उससे भी अधिक समय रहे। मैंने किसी भी महिला को निर्वस्त्र अथवा कम वस्त्रों में स्नान करते नहीं देखा। सभी महिलाएं पूरे वस्त्रों में गिन कर कुछ डुबकियां लगातीं थीं और बाहर आ जाती थीं, प्रायः साड़ी पहने महिलाएं केवल साड़ी फैलाकर, झाड़कर हवा ले रही थीं न कि वस्त्र उतार रही थीं अथवा खुले में बदल रही थीं। अथवा वे अपनी गाड़ी में आकर वस़्त्र परिवर्तन कर रही थीं। पूरी हर की पौड़ी तक जो न जाने कितने मीलों तक फैली है मुझे केवल दो स्थान दिखे महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के लिए।
सम्भव है मेरे भीतर भारतीय संस्कृति, परम्पराओं की समझ का अभाव हो, किन्तु गंगा में स्नान विशेषकर, महिलाओं का , मुझे कभी भी समझ नहीं आया। गंगा किनारे अस्थियां प्रवाहित हो रही थीं, लोग पिंड-दान करवा रहे थे, पूजा-सामग्री जल में तिरोहित हो रही थी, और न जाने क्या-क्या। मटमैला जल था, उसमें स्नान प्रक्रिया चल रही थी।
लौटती हूं मुख्य विषय पर।
किन्तु पुरुष, पूर्ण नग्न होकर ही जल में उतर रहे थे और बाहर आकर साथी से तौलिया मांगकर फैलाकर लपेट रहे थे। वे जल में निरन्तर किलोल कर रहे थे। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि ऐसी भाषा लिख रही हूं किन्तु यही शाश्वत सत्य है कि पुरुष कभी भी सामाजिक, पारिवारिक अथवा कहीं भी कोई संकोच नहीं करते। इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाएं आधुनिक वेशभूषा पहनने लगी हैं, देह प्रदर्शनीय वस्त्र। किन्तु अकारण ही केवल लिखने के लिए लिख देना कदापि शोभा नहीं देता।
मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा
एक पुरानी कहावत है : मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है, चलिए आज इस मुहावरे की चीर-फ़ाड़ करते हैं।
मित्र कौन है? मेरी समझ में मित्र वह है जो हमारी अच्छाईयों-बुराईयों के साथ हमें स्वीकार करता है। जिससे हम निःसंकोच अपना सुख-दुख, परेशानी बांट सकते हैं और उससे सामाजिक, मानसिक सहयोग की आशा रखते हैं। जो हमें, हमारे परिवार के साथ हमें स्वीकार करता है, जो हमें हमारी कमियों के साथ तो स्वीकार करता ही है और हमारी गलतियों के लिए हमें डांटने, मना करने, रोकने का भी साहस रखता है, वही मित्र कहलाता है और यही अपेक्षाएॅं वह हमसे भी करता है।
किन्तु शत्रु की हमारे मन में एक सीधी-सी व्याख्या है कि यह व्यक्ति हमारे लिए जो भी करेगा, बुरा ही करेगा।
किन्तु हम शत्रु किसे मानें और क्यों मानें। मित्र शब्द को परिभाषित करना जितना सरल और शत्रु शब्द को परिभाषित करना उतना ही कठिन। दूरियाॅं, अनबन, नाराज़गी जैसे भाव सरल होते हैं किन्तु शत्रु शब्द बहुत ही गहरा एवं नकारात्मक है जहाॅं अच्छाई और सच्चाई के लिए कोई जगह ही नहीं रह जाती।
मेरी समझ तो यह कहती है कि यदि शत्रु बुद्धिमान होगा तब तो उससे और भी सावधान रहने की आवश्यकता है। मूर्ख मित्र से भी ज़्यादा। मूर्ख मित्र भूल कर सकता है, नादानी कर सकता है किन्तु धोखा, छल-कपट, धूर्तता, प्रवंचना नहीं कर सकता।
यह ज़रूरी नहीं है कि पुरानी सभी कहावतें, मुहावरे ठीक ही हों।
शत्रु तो शत्रु ही रहेगा, बुद्धिमान हो अथवा मूर्ख।
मित्र स्वीकार हैं, और जो वास्तव में मित्र होते हैं वे मित्रों के लिए कभी भी मूर्ख हो ही नहीं सकते। और यदि हैं भी तो भी स्वीकार्य हैं। और शत्रुओं की तो वैसे ही जीवन में कमी नहीं है, बुद्धिमान, मूर्ख सबकी लाईन लगी है, एक ढूॅंढने निकलो, हज़ार मिलते हैं।
वर्तमान में दुनिया आभासी मित्रों एवं शत्रुओं से ज़्यादा बौखलाई दिखती है।
मित्रता
मैं नहीं जानती कि मैं क्यों मित्र नहीं बना पाती थी। जहॉं मैं स्वभाव की बहुत बड़बोली मानी जाती थी वहॉं व्यक्तिगत रूप से बहुत संकोची थी। अर्थात मन की बात किसी से कह देना मेरे स्वभाव में कभी नहीं रहा। और जब हम मित्रों से अपने बारे में छुपाने लगते हैं और झूठ बोलने लगते हैं तो वे दूर हो जाते हैं क्योंकि हर कोई इतना तो समझदार होता ही है कि वह वास्तविकता और छुपाव में अन्तर कर लेता है।
किन्तु कवि गोष्ठियों एवं समारोहों में मेरी एक मित्र बनी मीरा दीक्षित। यह शायद 1994-95 के आस-पास की बात है। हम प्रायः मिलते, घर भी आते-जाते और परस्पर खुलकर बातें भी करते। यद्यपि मैं यहॉं इस रूप में संकोची ही रही किन्तु मीरा शायद मेरे इस स्वभाव को जान गई थी और इसे उसने सहज लिया और हमारी मित्रता अच्छी रही।
किन्तु सन् 2000 के आस-पास मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएॅं-दुर्घटनाएॅं घटीं कि हम शहर छोड़कर सारी स्मृतियॉं पीछे छोड़कर बहुत दूर निकल गये। नया शहर, नये लोग, नई परिस्थितियॉं, नये संघर्ष, पिछला कुछ तो मिट गया, कुछ छूट गया। स्मृतियॉं विश्रृंखलित हो गईं।
इस बीच 2011 में मैं फ़ेसबुक से जुड़ी और मेरा लेखन पुनः आरम्भ हुआ। 2016 में मेरी एक रचना पर मेरी मित्र मीरा का संदेश आया कि कविता कहॉं हो। मुझे याद ही नहीं आया। फिर संदेश बाक्स में बात होती रही, वे पूछती रहीं और मैं अनुमान लगाती रही। बाद में उन्होंने कुछ संकेत दिये तो मैं पहचान पाई। जितनी प्रसन्नता हुई उतना ही दुख कि मैं अपनी ऐसी मित्र को कैसे भूल सकती थी। फिर बीच-बीच में कभी बातचीत, विचारों का आदान-प्रदान, रचनाओं पर प्रतिक्रियाएॅं।
किन्तु मेरे लिए वह एक बहुत ही सुन्दर दिन था जब मेरा एक साहित्यिक समारोह में लखनउ जाने का कार्यक्रम बना। मीरा लखनउ में ही थीं। मैंने उन्हें तत्काल फ़ोन किया और मिलने का कार्यक्रम बनाया। मेरे पास समय कम था, 26 मई को मैं समारोह के लिए पहुॅची और 27 दोपहर की मेरी वापसी थी।
लगभग 24 साल बाद हम मिले। मीरा मुझसे मिलने प्रातः 8 बजे मेरे होटल आईं। हमने मात्र दो घंटे साथ बिताए, किन्तु वे दो घंटे मेरे लिए अविस्मरणीय रहे। इतना आनन्द, सुखानुभूति, लिखना असम्भव है।
हमने यही कहा, यदि ईश्वर ने यह अवसर दिया है तो आगे भी ज़रूर मिलेंगे।
संकुचित मानसिकता आज क्यों बढती जा रही है
यह बात बिल्कुल सत्य है कि आज संकुचित मानसिकता बढ़ती जा रही है। यह सामाजिक, पारिवारिक तौर पर चिन्ता का विषय है।
संकुचित मानसिकता के भी कई रूप हैं। धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक। मेरी दृष्टि में इस समय हमारी सर्वाधिक संकुचित मानसिकता धार्मिक है। दूसरे स्थान पर सामाजिक है, जो धार्मिकता से ही प्रभावित है।
धर्म से जुड़े रहना अच्छी बात है किन्तु अंध-धार्मिकता मनुष्य को पीछे ले जाती है। वर्तमान में शिक्षा, रोज़गार, आत्मनिर्भरता, चिकित्सा सुविधाओं से अधिक चर्चा हम धर्म पर करने लगे हैं। आज अनेक तथाकथित धर्म-प्रचारक आॅन-लाईन बैठे हैं और हम लोग चाहे-अनचाहे उन्हें सुनने लगते हैं, रील्ज़ देखने लगते हैं, जो एक धीमे ज़हर के रूप में हमारे मन-मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं और हमारी सोच अपने-आप ही बदलने लगती है और इस परिवर्तन को हम समझ ही नहीं पाते।
चिन्तनीय यह कि पढ़े-लिखे लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। एक ओर हम विज्ञान में चाॅंद को छू रहे हैं दूसरी ओर हम अंधविश्वासों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। इसका एक कारण आज के समाज में प्रदर्शन, दिखावा बढ़ता जा रहा है। हम अपने-आपको हर समय दूसरों से बेहतर सिद्ध करने के प्रयास में लगे रहते हैं। किन्तु यह बेहतरी रहन-सहन, व्यवहार की नहीं, अपने आपको अकारण श्रेष्ठ सिद्ध करने की भावना को लेकर है। धर्म, संस्कृति, पूजा-पाठ, पर्वों पर अकारण दिखावा भी संकुचित मानसिकता का ही प्रतीक है, क्योंकि हम सहज-सरल जीवन से दूर होकर प्रदर्शनों की दुनिया में जीने लगे हैं।
आदर-सूचक शब्द
किसी का नाम लिखते समय हमें कितने आदर-सूचक शब्द आगे-पीछे लगाने चाहिए। आदरणीय, श्री, परम श्रद्धेय, आचार्य, गुरुवर, पूज्य, चरणवन्दनीय, प्रातः स्मरणीय, ऋषिवर, -परमादरणीय जी आदि-इत्यादि।
आजकल कुछ महान लेखन अपने से महान लेखकों के नाम के साथ एकाधिक ऐसे ही सम्बोधन कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि किसी के नाम के साथ केवल एक ही आदरसूचक शब्द का प्रयोग होना चाहिए चाहे वह नाम से पहले हो अथवा नाम के बाद।
और यदि किसी के नाम के साथ डा., प्रो. आदि हों तो उससे पूर्व भी किसी सम्मानसूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।
सम्मानजनक शब्दों के प्रयोग की भी एक सीमा होती है, इतने भी नहीं लिखे जाने चाहिए कि वे हास्यास्पद प्रतीत होने लगें अथवा चाटुकारिता।
आप क्या-क्या लिखते हैं।
निर्जला-एकादशी
मुझे कुछ बातें समझ नहीं आतीं, आपको आतीं हो तो मुझे अवश्य बताईएगा।
निर्जला एकादशी के दिन जगह-जगह छबील लगी थी।
पानी में कच्चा दूध, रूह-अफ़जाह और बर्फ़ से ठण्डा कर आने-जाने वालों को रोक-रोक कर यह जल पिलाया जा रहा था। अधिकांश महिलाएॅं और छोटे-छोटे बच्चे ही वहाॅं पर सेवा-भाव से काम कर रहे थे। गर्मी इतनी कि लगभग सभी आने-जाने वाले पानी पी रहे थे। अच्छा लगा।
किन्तु आज ही सभी लोग निर्जलाएकादशी के कारण छबील लगा रहे थे। क्योंकि यह पुण्य का कार्य माना जाता है, न कि वास्तव में प्यासे लोगों को पानी पिलाने की सोच। यह भी देखने में आया कि दस-दस, बीस-बीस गज़ की दूरी पर छबील लगी हुई थीं। प्रातः 9 बजे से चल रही छबील 12 बजे तक सिमटने लगीं और जब सूर्य आकाश पर आकर तपने लगा तब तक अधिकांश छबील सिमटकर जा चुकी थीं। क्या ऐसा नहीं कर सकते थे कि आपस में तालमेल कर लेते और एक छबील समाप्त होने पर दूसरी फिर तीसरी और इस तरह लगाते तो आने-जाने वाले लोगों को शाम तक ठण्डा पानी मिल पाता।
यह भी ज्ञात हुआ कि आज के दिन पंखी, खरबूजे और घड़ों का दान किया जाता है जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। अर्थात् यह दान भी जरूरतमंदों के लिए नहीं, अपने पुण्य के लिए करना है। पहले यह दान ज़रूरतमंदों को दिया जाता था अब मन्दिरों में देने की प्रथा बन गई है।
इतनी गर्मी में भी मन्दिरों के आगे भारी भीड़ देखने को मिली। और अधिकांश महिलाएॅं अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ वहाॅं लाईन में लगी हुई थीं। मन्दिरों में पंखियों, घड़ों और खरबूजों के ढेर लग रहे थे।
मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वहाॅं इनका क्या उपयोग हुआ होगा।
निर्जला एकादशी के दिन छबील लगाना और दान देना पुण्य का काम है किन्तु इतनी गर्मी में लोग तो हर रोज़ ही गर्मी और प्यास से त्रस्त हैं। जो लोग दान एकत्र करके केवल एक दिन के लिए छबील लगाते हैं वे क्या कहीं मार्गों पर स्थायी रूप से आने जाने वालों के लिए पीने के पानी की स्थायी व्यवस्था नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं किन्तु क्यों करें और पहल कौन करे। मुझे तो आज करना था क्योंकि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है।
मैं फिर भटक कर गूगल पर चली गई। वहाॅं से प्राप्त ज्ञान भी आपसे बाॅंटना चाहूॅंगी।
यह सारे कथन व्यास जी के हैं, मेरे नहीं।
निर्जला एकादशी पर गरीबों को दान देने, पानी पिलाने एवं जल भरा मटका दान करने से आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है, इससे मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, जीवन में सुख-समृद्धि की प्राप्ति भी होती है।
विष्णु पुराण के अनुसार ज्येष्ठ के महीने में सूर्य की बढ़ती गर्मी से हर जीव परेशान हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप किसी प्यासे को जल भरे मटके का दान देते हैं, तो उसकी आत्मा जल पीकर तृप्त हो जाती है और उस मनुष्य के मुख से निकली हुई कामना ईश्वर की वाणी होती है।
जो ज्येष्ठ के शुक्लपक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे, वे परमपद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है, ये ब्रह्महत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं।
जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है, यह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चाण्डाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है।
जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई सौ पीढ़ियों को और आने वाली सौ पीढ़ियों को भगवान् वासुदेव के परम धाम में पहुँचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शय्या, सुन्दर आसन, कमण्डलु तथा छाता दान करने चाहिये। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है।
इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन प्राप्तियों के लिए आप भी निर्जला एकादशी का व्रत, दान आदि अवश्य करें।
रक्षा बंधन
रक्षा-बन्धन का पर्व भाई-बहन के अपनत्व का पर्व है। इस पर्व में अन्य कोई भी रिश्ता समाहित नहीं है। सम्भवतः इसी कारण इस पर्व में सदैव एक सादगी रही है। हमारे समय में बाज़ार में सुन्दर आकर्षक, सादगीपूर्ण राखियाॅं मिलती थीं। राखियों के साथ लाल रंग की मौली अथवा कंगना बांधा जाता था। टीका लगाकर बहन राखी बांधती थी, घर में बने मिष्ठान्न से बहन भाई का मुॅंह मीठा करवाती थी और भाई शगुन के रूप में बहन के हाथ में अपनी क्षमतानुसार कुछ राशि देता था।
यह मानने में कोई संकोच नहीं कि वर्तमान में सभी रिश्तों की गहराई में परिवर्तन आया है। वर्तमान में भाई अथवा बहन के विवाहित होने पर इस पर्व में प्रर्दशन और भी बढ़ गया है। बहन क्या लेकर आई है, भाई क्या देकर जायेगा, बात होती है। वैसी सादगी व अपनापन कहीं खो गया है। रिश्तों पर आधुनिकता की कलई चढ़ गई है। लाल मौली या कंगना की जगह चांदी-सोने की राखियाॅं लाई जाती हैं और भाई शगुन न देकर उपहार देने लगे हैं। शेष हमारे विज्ञापन जगत, टीवी धारावाहिकों एवं व्यापार ने रिश्तों को बदल दिया है और हम अनचाहे ही उसमें उलझकर रह गये हैं।
कविता सूद 19.8.2024
दण्ड विधान
आज तक मैंने कभी भी किसी रिश्वत देने वाले को दण्डित किये जाने का समाचार नहीं पढ़ा। यदि ऐसा हो कि रिश्वत लेने वाले से पहले देने वाले को दण्डित किया जाये तो शायद किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार पर अधिक रोक लग पायेगी।
========
हम बच्चों की शिक्षा पर बहुत बात करते हैं।
किन्तु आज प्रतियोगी परीक्षाओं की जो स्थिति सामने आ रही है केवल इस पीढ़ी का ही नहीं, अगली पीढ़ी भी चिन्ताओं में घिरी बैठी है। अभी तीन परीक्षाएॅं पेपर लीक होने के कारण निरस्त कर दी गईं। केवल एक ही प्रतियोगी परीक्षा में लगभग 24 लाख विद्यार्थी बैठे थे और स्थान केवल एक लाख 10 हज़ार थे। इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी 10वीं के बाद दो वर्ष तैयारी करते हैं और साथ ही प्लस 1 और प्लस 2 की भी परीक्षाएॅं देते हैं। कोचिंग पर ही लाखों रुपये लग जाते हैं। इस धांधली में कितने लोग पकड़े गये, कितने नहीं, सच्चाई आम आदमी तक पहुॅंचती ही नहीं। पुर्नपरीक्षा कब होगी कोई नहीं जानता और पुनर्परीक्षा होने तक विद्यार्थी किस मनःस्थिति में रहेंगे , चिन्तनीय विषय है।
सबसे चिन्ता की बात यह कि वे कौन अभिभावक हैं जो अपने अयोग्य बच्चों को धन-बल से डाक्टर, इंजीनियर आदि बनाना चाहते हैं। आज हमारी चिन्ता यह तो है ही कि पेपर लीक हुए और बच्चों का भविष्य अधर में लटका। इस धांधली में लगे लोगों को दण्डित किया ही जाना चाहिए। किन्तु इतनी ही चिन्ता यह भी होनी चाहिए कि अयोग्य विद्यार्थियों के अभिभावक भी उतने ही दोषी हैं। यदि अभिभावक अपने बच्चों के लिए गलत राहें न चुनें तो यह अपराध अपने-आप ही कम होने लगेंगे, और धन देने वालों के लिए भी दण्ड का प्रावधान हो ।
कविता सूद 25.6.2024
विडम्बना
मैं अपने-आपको नास्तिक मानती हूॅं । क्योंकि मूर्ति-पूजा, मन्दिर जाना, प्रवचन, धार्मिक आख्यानों, व्रत-उपवास, साधु-संतों में मेरा विश्वास नहीं बनता। किन्तु जो मानते हैं मैं उनकी भी विरोधी नहीं हूॅं। किन्तु वर्तमान में आख्यानक, मंचों से धार्मिक भाषण परोसने वाले बाबा और बेबियाॅं मुझे कभी समझ नहीं आते। वे क्या समझाना चाहते हैं और लोगों की लाखों की भीड़ अपने जीवन में उनके भाषण से क्या समझना चाहती है, जो वे स्वयॅं नहीं जानते। उनकी भाषा, उनकी बातें, सब अद्भुत होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानों हमारा जन्म ही व्यर्थ है और हम नितान्त मूर्ख, अज्ञानी हैं। परिवार, समाज, सम्बन्ध सब लालसाएॅं हैं। वे मनोवैज्ञानिक अथवा मनोविश्लेषक भी नहीं होते किन्तु लोगों को इस रूप में भ्रमित अवश्य करते हैं। घंटों भीड़ में बैठकर, अपना पूरा दिन भूखे-प्यासे, घरों से दूर, क्या उपलब्ध होता है लोगों को। इन लोगों की अधकचरी ज्ञान से सनी धार्मिक ग्रंथों की मन से गढ़ी कथाएॅं क्या दे पाती हैं लोगों को, समझ नहीं आता। वास्तव में यह वैसा ही भीेड़-तंत्र है जैसे आजकल सड़कों पर होता है। जब लोग बिना जाने-समझे, किसी को पिटता देख उसे पीटने में हाथ आजमाने लग जाते हैं। वैसे ही, यहाॅं भी होता है कि भीड़ में घुसकर देखें तो यहाॅं क्या हो रहा है।
किन्तु भीड़ में घुसकर, हाथ आजमाने में कब जान चली जाती है कब अपने खो जाते हैं, कब क्या लुट जाता है, कौन समझ पाता है।
किन्तु यहाॅं भी तो यही कहा जाता है कि चलो ऐसे स्थान पर जान गई, सीधे स्वर्ग पहुॅच गये।
किसी ने लिखा था कि देह यहाॅं जल जाती है, आत्मा अजर-अमर है तो नर्क और स्वर्ग का कैसे पता।
ऐसे हादसों में कोई अपराधी नहीं होता। किसी को दण्ड नहीं मिलता। वैसे भी हमारे भारत में दण्ड व्यवस्था बहुत विनम्र है। जीवन बीत जाता है किसी अपराधी को पकड़ने में और दण्डित करने में, और निरपराध कारागार में जीवन बिता देते हैं।
मृतकों को दो-दो लाख, घायलों को दस-बीस हज़ार, हमारा कर्तव्य पूरा। यह और बात है कि यह घोषित राशि वास्तव में मिलेगी भी या नहीं।
हाथरस की घटना से हम कोई सबक तो लेंगे नहीं।
तो तैयार रहिए अगली दुर्घटना की बात सुनने के लिए।
समाधान या हार
कोई भी समस्या आने पर उसका समाधान ढूॅंढने की अपेक्षा हम हार मानने लगे हैं।
आजकल समाचारों में आत्महत्याओं के समाचार विचलित करते हैं। अंक कम आने पर, नौकरी न मिलने पर, परिवार में थोड़ी-सी कहा-सुनी पर बड़े क्या, बच्चे भी आत्महत्या करने लगे हैं। इसके कारण की ओर कभी हमारा ध्यान गया क्या?
मुझे लगता है आज की पीढ़ी अपने-आप में जीने लगी है। वह केवल अपने आप ही सोचती है, स्वयं निर्णय लेती है और असफ़ल होने पर तत्काल हार मान लेती है। परिवार से दूरियाॅं इसका एक कारण हो सकता है। परिवार एकल हैं और कोई भी अपनी समस्याओं को बाॅंटने के लिए किसी को अपने आस-पास नहीं देख पाता। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि वर्तमान में अपेक्षाएॅं बहुत अधिक हैं और विकल्प कम। वैसे विकल्प कम तो नहीं हैं किन्तु हमने ही विकल्प सीमित कर लिए हैं। यदि किसी मार्ग पर हम सहज रूप से नहीं चल पा रहे हैं तो राहें बदलने के बहुत से विकल्प होते हैं किन्तु वर्तमान में इसे सहजता से नहीं लिया जाता और गलत कदम उठा लिये जाते हैं। प्रथम आने का दबाव, अच्छी नौकरी, खर्चीली जीवन-शैली, प्रदर्शन, कहीं न कहीं मानसिक तनाव पैदा करती हैं।
एक और कारण जो मुझे प्रतीत होता है कि पुरुष जब किसी क्षेत्र में असफ़ल होता है तो वह हीन-भावना से ग्रस्त हो जाता है और अपनी हार किसी के समक्ष स्वीकार नहीं कर पाता विशेषकर पत्नी के समक्ष अपने को हारा हुआ आदमी नहीं दिखा सकता। उसकी यह भावना उसे पहले मानसिक तनाव , उपरान्त आत्महत्या तक ले जाती है।
कोई भी समस्या आने पर उसका समाधान ढूॅंढने की अपेक्षा हम हार मानने लगे हैं। इस समस्या का एक ही समाधान है कि हम परिवार, मित्रों के साथ जुड़ें, अपने हितचिन्तकों को पहचानें और कोई भी कठोर निर्णय लेने से पहले अच्छे से विचार करें।
मौसम मौसम
जब हम छोटे थे, वैसे बहुत बड़ा तो अपने-आपको मैं अभी भी नहीं मानती, आप मानते हों तो मुझे बता दीजिएगा।
हांॅं, तो जब हम छोटे थे, तो तीन ही मौसम जानते थे, गर्मी, सर्दी और बरसात। और शुद्ध हिन्दी में बरसात के मौसम को मानसून कहा जाता था। ये सावन-भादों जैसे शब्द तो कभी सुने ही नहीं थे। तब बसन्त ऋतु भी नहीं हुआ करती थी। पुस्तकों में अवश्य चार ऋतुओं वर्णित थी, शीत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु। हिन्दी की कविताओं में सावन और बसन्त शब्द आये होंगे कभी, किन्तु इनका महत्व नहीं था। पन्त, दिनकर आदि छायावादी कवियों ने अवश्य सावन एवं बसन्त पर कविताएॅं लिखीं, पंजाबी गीतों में भी इनका वर्णन है, फ़िल्मी गीतों में भी बसन्त और सावन की झड़ी लगती रही है किन्तु इन्हें कभी इतना महत्व नहीं मिला था। महत्व था तो बस बरसात और सर्दी के मौसम का।
शिमला में एक अगस्त से 15 अगस्त तक बरसात की, और 1 जनवरी से 28 फ़रवरी तक सर्दी की छुट्टियाॅं मिलती थीं, इस कारण हमारे लिए यही ऋतुएॅं महत्व रखती थीं। वहाॅं तो गर्मियों में भी बरसात चली ही रहती थी। हम तो बस इतना जानते थे कि बरसात है तो चाय-पकौड़े, समोसे, गर्मागरम जलेबी, बरसात में भीगना। और सर्दी है तो मूंगफली, गचक, रेवड़ी अंगीठियाॅं और बर्फ़ के मौसम का आनन्द लेना।
यह सावन कब आया, वर्षा ऋतु या बरसात अथवा मानसून सावन में कब बदल गया, कुछ पता ही नहीं लगा। अब सावन का अति शुद्ध महीना, पूजा, व्रत, सोमवार को विशेष पूजा-विधि, खान-पान कुछ नहीं जानते थे हम। शिवरात्रि का ज्ञान भी फ़रवरी-मार्च में आने वाली शिवरात्रि का ही था। सावन की शिवरात्रि तो कभी सुनी ही नहीं थी। हम यात्राओें के बारे में भी नहीं जानते थे। अब जब से फ़ेसबक पर सावन आया तभी से यह ज्ञानवृद्धि भी हुई। हम तो बस हर मौसम का बेधड़क, बेझिझक आनन्द ही लेते थे।
मेरा अध्ययन मुझे यह बताता है कि जबसे फ़ेसबुक का आगमन हुआ तब से सावन और बसन्त शब्दों को महत्व मिला। ये महीने नहीं रह गये, उत्सव बन गये। और उत्सव भी बने तो प्रेम, श्रृंगार, मिलन, विरह, झूले, सखियाॅं। हमारे समय भी झूले होते थे। एक मोटी रस्सी छत से अथवा किसी वृक्ष की मज़बूत डाली पर लटकाकर, उपर तकिया या कोई मोटी चादर तह करके रख दी और बन गया झूला। अब ये रंग-बिरंगे झूले, फूलों से सजे, रंग-बिरंगे परिधान पहने मोहक युवतियाॅं, पता नहीं किस देश से आई हैं।
इसके बाद तीज का पर्व। हमारे समय में भी होता था लेकिन घर के भीतर तक ही। माॅं व्रत रखती थी और छोटी-सी पूजा करती थी। और अरे ! राधा-कृष्ण को मैं कैसे भूल सकती हूॅं। कवियों के पास लिखने के लिए विषयों की झड़ी लग गई। अब पूरा महीना फ़ेसबुक सावनी और प्रेममयी रहेगी।
बहुत अज्ञानी थे हम।
मन की बात तो कहनी ही रह गई। यह एक चिन्तन का विषय है कि हमारा अध्ययन-क्षेत्र आज फ़ेसबुक की रचनाओं तक सीमित रह गया है। और हम अथवा मैं उसी माध्यम से सोचने-समझने लगे हैं।
अब सावन की बात करें तो, फ़ेसबुक पर तो सावन की बौछारें, प्रेम, श्रृंगार, राधा-कृष्ण, झूले, तीज मनाती, गीत गातीं श्रृंगारित महिलाएॅं, और वास्तविक जीवन में उमस, भरी रसोई में रोटी पकातीं स्त्रियाॅं, आती-जाती बिजली से परेशान ज़िन्दगियाॅं, बन्द रास्तों में जाम में उलझते लोग , सड़कों पर भरता पानी, तालाब बनते घर, बेसमैंट में डूबकर मरते बच्चे, गिरते-टूटते पुल, फ़टते बादल, दरकते पहाड़।
=========-==
कहते हैं सावन जलता है, यहां तो गली-गली पानी बहता है
प्यार की पींगे चढ़ती हैं, यहां सड़कों पर सैलाब बहता है
जो घर से निकला पता नहीं किस राह लौटेगा बहते-बहते
इश्क-मुहब्बत कहने की बातें, छत से पानी टपका रहता है
क्यों आज की पीढ़ी परम्पराओं से विमुख हो रही है
वर्तमान में सामान्य तौर पर वर्तमान पीढ़ी पर यह आरोप है कि वह पारिवारिक व अन्य परम्पराओं से विमुख होती जा रही है, क्या यह सत्य है और यदि है तो क्यों, विचारणीय प्रश्न है।
इस प्रश्न को मैं दो रूपों में समझने का प्रयास करती हूॅं।
जी हाॅं, आज की पीढ़ी अपनी पारिवारिक प्राचीन परम्पराओं से विमुख हो रही है। और मैं इसमें आज की पीढ़ी को बिल्कुल दोषी नहीं मानती। समय बदलता है, शिक्षा बदली है, रहन-सहन बदले हैं, आवश्यकताएॅं और पारिवारिक, सामाजिक व्यवस्था सब बदल गये हैं।
इसके अनेक कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है हम अपनी अधिकांश पारिवारिक परम्पराओं के गहन निहितार्थ से परिचित ही नहीं हैं। बहुत सी परम्पराओं के पीछे कौन से पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कारण थे हम समय के साथ भूल चुके हैं, अथवा अल्प ज्ञान के साथ ही निभाने का प्रयास करते हैं। पिछले समय में अधिकांश महिलाएॅं घर में ही रहती थीं और संयुक्त एवं बड़े परिवार हुआ करते थे। इस कारण पारिवारिक परम्पराओं के बारे में जानकारी भी रहती थी और परस्पर मिलकर निभाने का आनन्द भी मिलता था। वर्तमान पीढ़ी तक ये परम्पराएॅं विश्रृंखलित होकर पहुॅंची हैं अतः उन्हें जो परम्पराएॅं निभाने में सुविधाजनक एवं मनोरंजक प्रतीत होती हैं उन्हें निभा लेते हैं, शेष की उपेक्षा कर जाते हैं।
फिर वर्तमान में परम्पराओं का भी बाज़ारीकरण हो चुका है। हमारी परम्पराएॅं घर के भीतर से निकलकर बाज़ार का हिस्सा बन चुकी हैं। और आज जो बाज़ार में बिकता है और दिखता है वही परम्परा बनता जा रहा है। ऐसी स्थितियों को सम्भवतः कोई नहीं रोक पाता अथवा बदल पाता है, केवल स्वीकोरक्ति ही इसका हल है।
रिश्तों को पैसे के तराजू में तोलना कहाॅं तक उचित है?
बात उचित-अनुचित की नहीं है, हमारी मानसिकता की है।
दुखद किन्तु सत्य यही है कि रिश्ते सदैव ही पैसों के तराजू में तोले जाते रहे हैं। यह कांेई आज की बात नहीं है, सदियों से ही यही होता आया है। मैंने अपने जीवन में यही सब समझा और देखा है। बहुत कम लोग हैं जो अपने सम्बन्धों को धन-दौलत से अलग, मन से निभाते हैं। कहावत भी है कि पैसा पैसे को खींचता है। यह बात केवल व्यवसाय अथवा धन-निवेश की नहीं है, सम्बन्धों, मैत्री की भी है। जब कोई धनवान किसी निर्धन से व्यवहार करता है तो उसकी बहुत सराहना की जाती है कि देखो, गरीब-अमीर में अन्तर नहीं करता। समाज द्वारा की जाने वाली यह सराहना ही बताती है कि रिश्ते पैसों के तराजू में तोले जाते हैं। यदि ऐसा न होता तो सम्बन्धों में निर्धन-धनी की बात ही न उठती। जब कभी किसी नये रिश्ते की ओर बढ़ना हो तो भी यही कहा जाता है कि भई, अपने बराबर का देखना।
यह बात आज की नहीं है, सदा से ही यही रीति रही है। कहाॅं राजा भोज कहाॅं गंगू तेली जैसी कहावतें इस सोच को चरितार्थ करती हैं। मैंने अपने आस-पास कितने ही व्यवहार देखे हैं। डूबते व्यक्ति को कोई सहारा नहीं देता, यदि देता है तो बस इतना कि ये लो और निकलो, लौटकर मत आना। यही इस समाज की सच्चाई है।
भ्रष्टाचारी सांसद विधायक के चुने जाने पर पार्टी जिम्मेदार हैं या आम आदमी
चुनाव में जो भी लोग खड़े होते हैं, उनका चयन पार्टी ही करती है न कि आम आदमी। सबसे बड़ी बात यह कि जिस व्यक्ति को पार्टी प्रत्याशी के रूप में चुनती है, उसके बारे में कभी भी कोई जानकारी नहीं दी जाती, और आम आदमी भी केवल पार्टी का नाम देखकर ही वोट दे देता है न कि व्यक्ति-विशेष की जानकारी लेना चाहता है कि वह कैसा है। किन्तु, इसमें कोई संदेह नहीं कि पार्टी तो अपने प्रत्येक उम्मीदवार के बारे में जानती ही है। पार्टी एवं आम आदमी के अतिरिक्त चुनाव आयोग की भी भूमिका रहती है, जहाॅं दूध का दूध एवं पानी का पानी सम्भव है किन्तु होता नहीं।
वास्तव में पार्टियों के अपने स्वार्थ रहते हैं और आम आदमी दिशाहीन एवं असंलिप्त। अतः पार्टी का दायित्व प्रथम है। और आम आदमी का दोष यह कि वह अपने ही अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है कि जब उसके पास वोट मांगने के लिए प्रत्याशी आता है तो वे उससे उसकी आधिकारिक पूरा जानकारी लें। आम आदमी ऐसी किसी भी समस्या से बचकर निकलना चाहता है। उसे किसी झंझट में नहीं पड़ना। किन्तु सर्वाधिक दायित्व चुनाव आयोग का है जिसके पास प्रत्येक प्रत्याशी का पूरा विवरण जाता है और वहां से उसे चुनाव में खड़े होने के अधिकार मिलते हैं। वास्तविकता यह कि 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में जहाॅं आज भी धनबल पर वोट लिये जाते हैं, मतदान केन्द्र लूटे जाते हैं, अशिक्षा चरम पर है, वहाॅं आम आदमी के हाथ में कुछ नहीं है। अतः मेरी समझ में दायित्व पार्टियों का एवं चुनाव आयोग का है कि भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को टिकट ही न मिले।
क्या समाज ने अंतर्जातीय विवाह को स्वीकार कर लिया है
हमारा समाज बहुत विखण्डित है। हमारे समाज में लाखों-लाखों जातियाॅं हैं। लोगों की सोच में परिवर्तन शिक्षा, आर्थिक स्थिति, निवास-स्थान एवं कार्य-क्षेत्र पर बहुत निर्भर करता है। आज भी हम लोग जाति की सोच से बाहर नहीं निकल पाये। आज भी जब कोई हम लोगों से नाम पूछता है तो हम बिना जाति के नाम नहीं बताते। और यदि केवल नाम बताएॅं तो सामने वाले की आॅंखों में एक प्रश्नचिन्ह होता है कि अगले ने पता नहीं क्यों ‘‘जात’’ नहीं बताई। 140 करोड़ जनसंख्या वाले हमारे आस-पास, परिचितों, सम्बन्धियों में अन्तर्जातीय विवाह हो रहे हैं, और उन्हें मान्यता मिल जाती है अथवा विवशता में दे दी जाती है। किन्तु क्या यह स्थिति पूरे देश में है ? सभी जातियों, प्रान्तों, गांवों में है ? शायद , नहीं।
वास्तविकता यह है कि हम आज भी उन्हीं रूढ़ियों में जी रहे हैं। किन्तु अन्तर्जातीय विवाह का विरोध करने के और भी अनेक कारण हैं।
हमारे देश में जाति, स्थान, वर्ग, प्रदेश, गांव, आदि के अलग-अलक रीति-रिवाज़, परम्पराएॅं, लेन-देन, खान-पान, भाषा-भिन्नताएॅं हैं जिस कारण परिवारों में सामंजस्य बहुत कठिन होता है। इस कारण आज भी लोग अन्तर्जातीय विवाह करने में संकोच करते हैं।
अतः मेरे विचार में हमारे समाज ने अन्तर्जातीय विवाह को स्वीकार नहीं किया है।
श्मशान घाट
कौन कहता है कि श्मशान घाट से कोई लौटकर नहीं आता। जाता तो केवल एक है, शेष सब तो लौट ही आते हैं, डरे, सहमे, घबराये, अतीत की अमिट परछाईयों के साथ, जीवन के प्रति एक ऐसे नये चिन्तन एवं दृष्टिकोण के साथ जिसे हम न तो कभी सोच पाये थे और न ही समझ पाये थे। अपने-परायों, सम्बन्धों की उधेड़-बुन के साथ। जो गया, क्यों चला गया, कौन था, कितना अपना था, क्यों चला गया। सबसे कठिन होता है, जब हम जाने वाले के लिए तैयारी करने लगते हैं, सामान, सामग्री जुटाते हैं, समय निर्धारित करते हैं। सबको सूचित करने लगते हैं। आहत करती हैं ये स्थितियाँ, तोड़ती हैं, पूछती हैं, क्या कर लोगे तुम, कैसे करोगे। एक लम्बी कहानी रह जाती है, सम्बन्धों की, स्मृतियों की, अनुभवों की, और सबसे विशेष उन कथाओं की जो हमारे आस-पास बुनी जाने लगती हैं। जीवन के न जाने कितने नये पृष्ठ खुल जाते हैं। एक जीवन समाप्त होता है तो एक नया शुरु भी होता है। कुछ साथ देती हैं और कुछ उपेक्षा, कुछ मरहम लगाती हैं और कुछ कुरेदती हैं। यही जीवन के आने-जाने की वास्तविकता है।
एक पाती भाव भरी
अब हम सत्तर वर्ष के हो गये, एक क्या हज़ारों भाव भरी पाती स्मृति में उभर कर आ गईं। किस-किसकी बात करें आपसे। कभी तीन पैसे का पोस्ट कार्ड आता था, पांच पैसे का अन्तर्देशीय और बन्द लिफ़ाफ़े पर दस पैसे का टिकट लगता था। जब घर में बन्द लिफ़ाफ़ा आता था तो पूरा घर चैकन्ना हो जाता था कि किसी का अत्यन्त महत्वपूर्ण पत्र आया है जो बन्द लिफ़ाफ़े में आया है।
मेरी पहली भावभरी पाती वह थी जो किसी पत्रिका में मेरी पहली कविता प्रकाशित होने पर एक पाठक ने प्रशंसा पत्र भेजा था। पोस्टकार्ड था । उस समय तक पोस्ट कार्ड का मूल्य बढ़ चुका थाः दस पैसे। मेरे जीवन का वह पहली भाव भरी पाती थी जो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। दिनों-दिनों तक मैं उस पोस्ट कार्ड को छुपा-छुपाकर पढ़ती रहती थी। उसके बाद ऐसी कितनी ही भाव-भरी पाती आईं और मैं आह्लादित होती थी ऐसी पाती से। ऐसे पत्र पाठक के मन से लिखे होते थे, और उनका मैं उत्तर भी अवश्य देती थी। आज की तरह नहीं कि गूगल ने कुछ बने-बनाये शब्द दे दिये और हम उन्हें ही काॅपी-पेस्ट किये जा रहे हैं।
मेरे प्रिय हिन्दी साहित्यकार : हज़ारी प्रसाद द्विवेदी
हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य से मैं बहुत गहरे तक जुड़ी हुई हूं। अपने अध्ययन काल में अनेक कवि, लेखक, उपन्यासकार, इतिहासकार रहे जिनकी पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया किन्तु हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन मुझे बहुत गहरे तक जोड़ता रहा है।
हज़ारी प्रसाद द्विवेदी (19 अगस्त 1907 - 19 मई 1979) हिन्दी निबन्धकार, आलोचक, उपन्यासकार थे। कलाओं के प्रति इनके दृष्टिकोण ने प्राचीन एवं मध्यकालीन हिन्दी साहित्य के अध्ययन के नवीन द्वार उन्मुक्त किये। साहित्य की प्रत्येक विधा में वे पारंगत थे। वे हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत और बाङ्ला भाषाओं के विद्वान थे।
द्विवेदीजी ने शांति निकेतन में बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष, उपरान्त पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष, पुनः काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष बने। उनकी
विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर नियुक्ति हुई। कुछ समय के लिए हिन्दी का ऐतिहासिक व्याकरण योजना के निदेशक भी बने। कालान्तर में उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के अध्यक्ष तथा 1972 से आजीवन उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ के उपाध्यक्ष पद पर रहे। 1973 में आलोक पर्व निबन्ध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।1957 में पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किये गये। 1997 में इनके चित्र का डाक टिकट भी जारी हुआ।
हिन्दी साहित्य पर इनका लेखन पठनीय एवं अप्रतिम है। मुझे इनकी संस्कृतनिष्ठ भाषा बहुत आकर्षित एवं प्रभावित करती रही है। हिन्दी साहित्य को इन्होंने एक नई पहचान दी। रामचन्द्र शुक्ल के बाद इनकी हिन्दी साहित्य एवं इतिहास पर लिखी गई पुस्तकों ने हिन्दी साहित्य के पाठकों को एक नवीन, चिन्तनपूर्ण दृष्टि प्रदान की। मध्यकालीन हिन्दी साहित्य एवं प्राचीन एवं अर्चाचीन साहित्य पर इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें एक नवीन चिन्तन प्रदान करती हैं। सांस्कृतिक एवं पौराणिक पृष्ठभूमि पर रचित उपन्यास गहन चिन्तन की ओर ले जाते हैं। विषय विविधता इनके लेखन की विशेषता रही है। अगस्त 1981 में आचार्य द्विवेदी की उपलब्ध सम्पूर्ण रचनाओं का संकलन 11 खंडों में हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली के नाम से प्रकाशित हुआ।
नई पीढ़ी और हिन्दी
नई पीढ़ी की हिन्दी आजकल स्टैंडअप कामेडियन बनकर रह गई है।
बात कटु किन्तु है सत्य कि नई पीढ़ी के पास हिन्दी नहीं है। वे केवल बोल-चाल में हीए उतनी ही हिन्दी जानते हैं जितनी आवश्यक है। और आज की पीढ़ी की हिन्दी, हिन्दी न होकर एक अद्भुत- मिश्रितए खिचड़ी भाषा है, अपशब्दों की भरमार रहती है।
इसके लिए हम नई पीढ़ी को दोष नहीं दे सकते। उनको जो मिल रहा है वही वे परोस रहे हैं और खा-खिला रहे हैं।
इसके अनेक कारण हैं।
आज सारे देश में समान भाषा पद्धति नहीं है, है तो केवल अंग्रेज़ी के लिए। हिन्दी देश के कुछ ही राज्यों में अनिवार्य है वह भी केवल दसवीं तक। अनेक राज्यों में यहां भी अन्य स्थानीय भाषाओं के लिए विकल्प दे दिया जाता है। प्रत्येक विषय का माध्यम अंग्रेज़ी ही रहता है। इसके अतिरिक्त CBSE, ICSE के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य के अपने शिक्षा बोर्ड हैं जो अपने राज्य के अनुसार भाषा का चयन करने के लिए स्वतन्त्र हैं।
सबसे बड़ी बात यह कि दसवीं के बाद हिन्दी का विकल्प ही नहीं है। यदि आप विभिन्न शिक्षा बोर्ड के विषयों को देखें तब वहां आपको हिन्दी का विकल्प दिखाई तो देगा किन्तु अधिकांश विद्यालय इसके लिए अध्यापक ही नियुक्त नहीं करते और हिन्दी का विकल्प ही नहीं देते।
इंजीनियरिंग, चिकित्सा, IT आदि सब अंग्रेज़ी आधारित ही हैं। यदि दसवीं तक अच्छी हिन्दी पढ़ाई भी जाये तो भी यहां तक आते-आते सब छूट जाती है।
कहने को हिन्दी समाचार-पत्र एवं टी वी समाचार पत्र हिन्दी में प्रसारित होते हैं किन्तु कैसी हिन्दी होती है यह तो हम जानते ही हैं। सरलता के नाम पर अभद्र भाषा का प्रयोग एवं निरर्थक अंग्रेज़ी शब्दों का ही प्रयोग होता है ।
एक अन्य कारण यह कि हम आज वैश्विक स्तर पर अंग्रेज़ी माध्यम से ही जुड़ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि अनेक देश आज भी अपनी भाषा से वैश्विक स्तर से जुड़े हुए हैं तो हम क्यों नहीं। इसका सीधा-सा कारण यह है कि जब हम 70 वर्षों में हिन्दी को उस स्तर पर स्थापित नहीं कर पाये तो अब यह असम्भव प्रायः ही प्रतीत होता है।
हमें स्वीकार करना ही होगा कि नई पीढ़ी हिन्दी के साथ नहीं है। केवल चलती हिन्दी बोल लेना अथवा लिख लेना हिन्दी नहीं है। व्याकरण कहीं खो गया है। शब्द अनर्थ होने लगे हैं, वर्णमाला ध्वस्त है। वाक्य संरचना का कोई अर्थ नहीं रह गया है।
ये आँखें
ये आँखें भी बहुत बड़ी चीज़ हैं। ये तो सब ही जानते हैं कि देखने के काम आती हैं किन्तु दिखाने के भी बहुत काम आती हैं, बस आपको दिखानी आनी चाहिए। आज सब सोचने लगी, आँखों के मुहावरों पर तो न जाने कितने मुहावरे सामने आ गये।
आँखों ही आँखों में हँसना, आँख मारना, आँखों में धूल झोंकना, आँखें बिछाना, आँख का कांटा, आँख का तारा, आँख लगना, आँख लड़ना, आँखें चुराना और न जाने कितने ही।
किन्तु कुछ मुहावरे तो बिल्कुल मेरे काम के निकले। जैसे
आँख धुंधलाना, आँख दिखाना, आँखों पर चरबी चढ़ना, आँख पर पर्दा पड़ना, आँखें बन्द होना, सीधी आँख न देखना और अन्त में आँख खुलना।
नववर्ष का उपहार लेकर आईं हमारी आँखें हमारे लिए। आँख धुंधलाने लगी। आँख देखने वाले को आँख दिखाई। किन्तु वे कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने हमें ही आँख दिखा दी। बोले, आँखों पर चरबी चढ़ गई है, आँखों पर पर्दा पड़ गया है।
और नववर्ष में उन्होंने हमारी एक आँख बन्द कर दी। अब न सीधी आँख देखना, न आँख मारना, न आँख लड़ना न लड़ाना। वाह! आँख के भीतर एक लैंस, एक चश्मा भी उपहार में मिला। मोबाईल, टी. वी., पी. सी. सब बन्द। और अन्त में जब ठीक से आँख खुली तब भी ठीक से अनुभव करने में दो-तीन दिन तो लग ही गये।
इसे कहते हैं cataract
अब एक आँख तो सुधर गई, दूसरी भी पीछे नहीं। तो चलिए उसके लिए भी ये सारे मुहावरे याद रखते हैं, अगले सप्ताह के लिए।
पहली मुलाकात
अजीब-सा लगा उसे वह युवक। बिखरे-से बाल, टी-शर्ट, मटमैले जूते, कंधे पर फीते वाला पुराना बैग, लेकिन है तो आकर्षक-सुन्दर, उसके मन ने कहा। उसकी टेढ़ी-सी निश्छल मुस्कान ने उसे जैसे बांध लिया। कौन है यह ? है तो अजनबी किन्तु कहीं अपना-सा लग रहा है। अहंहं, उसके मन ने उस पर ही उपहास कर डाला। अपनी उम्र देख, 30 की हो रही है और यह बच्चा-सा युवक उसे आकर्षक-सुन्दर लग रहा है।
यह उनकी पहली मुलाकात थी।
वह द्वार खोले खड़ी उसे देखती रही और वह युवक हँस दिया, घर के अन्दर भी आने देगी या नहीं?
अचानक उसके भीतर की अक्खड़ लड़की जाग उठी, ‘‘लेकिन आप हैं कौन उसने पूछा’’।
‘‘तू नीतू है न लड़ाकी-सी, संतोष की ननद’’।
अरे, ये तो मेरा घर का नाम जानता है, कौन है यह।
उसने रास्ता छोड़ दिया और वह युवक अधिकार से घर के भीतर चला आया।
तो यह उसकी भाभी का भाई। दिल में कहीं झंकार हुई।
दो दिन रुका। उससे बात की, कहा कि उसके ही लिए आया है यहाँ। सोचकर बताना, फिर आऊँगा।
और फिर वह उसकी ज़िन्दगी में सदा के लिए ही आ गया। किन्तु वह पहली मुलाकात आज तक नहीं भूलती।
शिमला की यादें
आज सौ कदम पैदल चलना पड़े तो वह कहते हैं न कि नानी याद आ गई। किन्तु स्मरण करती हूँ बचपन के वे दिन जब हम दिन-भर में 10-12 किलोमीटर तो प्रतिदिन चलते ही थे।
शिमला !
घर से लगभग पाँच किलोमीटर दूर स्कूल। सर्दी हो अथवा गर्मी, बरसात हो अथवा बर्फ़वारी, पूरा बस्ता उठाकर पैदल स्कूल। कोई आवागमन का साधन नहीं, बस पैदल जिसे हम ग्यारह नम्बर बस कहा करते थे। क्या मस्ती भरे दिन थे वे। जेबखर्च पाँच पैसे मिलते थे। और उन पाँच पैसे में पाँच-सात चीज़ें तो खरीद ही लेते थे। स्कूल से लौटते समय सड़क पर पकड़म-पकड़ाई, दौड़, रस्सी सब खेल लेते थे। उन दिनों कोई पीटीएम नहीं होती थी, न गृहकार्य की चिन्ता, न ट्यूशन, न माता-पिता को कोई तनाव कि बच्चे पढ़ रहे हैं अथवा नहीं। सब अपने-आप ही चलता रहता था। सबसे आनन्ददायक होता थी शीत ऋतु। इतने कपड़े पहनते थे कि गिनती ही नहीं हो पाती थी। दो-दो रजाईयाँ लेकर सोना। बर्फ़ में सानन्द घूमते। न बीमार होने की चिन्ता, न भीगने का डर। बर्फ़ खाना, गोले बनाना, बुत बनाना, खूब आनन्द लेते थे। अंगीठियों को घेरकर बैठे सारा दिन मूंगफ़ली खाना। पानी की कमी हो जाती थी, और यदि पानी आता भी था तो नलों में बर्तनों में जम जाता था स्लेट की तरह। कई-कई दिन नहाने की छुट्टी, वे दिन सबसे अच्छे लगते थे। हा हा।
बड़ी याद आती है शिमला तेरी और तेरे साथ बिताये दिनों की।
क्रोध एक सहज विकार
हम प्रायः देखते हैं कि एक से वातावरण में रहने वाले लोग, एक परिवार के सदस्य, एक ही कार्यालय में कार्य करने वाले लोगों के स्वभाव में ज़मीन-आसमान का अन्तर रहता है। एक ही वातावरण में पले-बढ़े बच्चे भी भिन्न स्वभाव के होते हैं। एक क्रोधी स्वभाव का हो सकता है और दूसरा प्रत्येक स्थिति में शांत, सहनशील। ऐसा क्यों होता है? ं
मैंने यह भी देखा है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, जैसे लोगों के बीच समय व्यतीत करते हैं, हम कितना भी बचने का प्रयास कर लें, हमारे स्वभाव में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता ही है। मुझे बहुत बार लगता है कि मानसिक शांति पाना और खोना हमारे हाथ में नहीं रह जाता।
क्रोध एक सहज विकार है। यदि हम अपने साथ होने वाले अन्याय का विरोध नहीं करते और उसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे मन को शांति कैसे मिलेगी।
मैं इस बात से कदापि सहमत नहीं हूं कि सकारात्मक सोच से मन को सदैव शांति मिल सकती है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे चारों ओर सकारात्मकता ही है। इतना कुछ है कि उसे शब्द देना कठिन है। कितना भी चाहें हम सदैव सकारात्मक नहीं हो सकते, यह सहज स्वाभाविक है। और यदि हम अपने मन के वास्तविक भाव को मार कर आरोपित शांत होने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा भाव कभी भी स्थाई शांति प्रदान नहीं कर सकता।
नकारात्मक तथ्य को इग्नोर करने अथवा उपेक्षा करने का अर्थ आज यह है कि हम बुराई को स्वीकृति दे रहे हैं। एक उक्ति है कि आज दुनिया में बुराई इसलिए नहीं बढ़ी है कि बुरे लोग अधिक हो गये हैं, इसलिए बढ़ी है क्योंकि सहने वाले लोग अधिक हो गये हैं। यदि हमारे आस-पास कुछ गलत हो रहा है तो उसकी उपेक्षा करके मन को शांति कैसे मिल सकती है? मन को शांति तो उसका विरोध अथवा निराकरण करके ही मिलेगी।
आज फ़ेसबुक पर ही एक पोस्ट पढ़ने को मिली थी, अमेरिका के किसी शोध का उल्लेख था कि जो महिलाएं अपने पतियों के साथ लड़ती हैं वे दीर्घायु होती हैं और जो तथाकथित सहनशील, शांत होती हैं उनको हृदयाघात अधिक होते हैं। क्योंकि जो लड़ लेती हैं वे अपने मन की भड़ास निकाल लेती हैं और उनके मन को शांति मिलती है किन्तु जो विरोध नहीं करती, मन में रख लेती है, दूसरे शब्दों में भीतर ही भीतर घुटती हैं वे मानसिक संताप में जीवन व्यतीत करती हैं।
मुझे तो यह पोस्ट बहुत ही अच्छी लगी, निश्चित है कि मुझे कभी भी हृदयाघात नहीं हो सकता।
आज तीन दिन बाद ज्वरमुक्त होने पर जब फ़ेसबुक खोली तो आपके इस आलेख ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। हमारे आस-पास ऐसे कुछ शब्द इस तरह बेहिचक प्रयोग किये जाते हैं और हम विरोध भी नहीं कर सकते। रोकने पर, टोकने पर यही सुनने को मिलता है कि तुझे ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तू ज़्यादा बनती है, तेरे रोकने से कोई बोलना तो बन्द नहीं कर देगा। avoid करना चाहिए। किन्तु मैं क्यों avoid करूं। क्योंकि अधिकांश गालियों में तो महिलाओं से सम्बन्धित शब्द होते हैं, न भी हों तब भी। एक रोचक अनुभव लिखने से नहीं रोक पा रही। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के लोग बहुत अच्छी हिन्दी बोलते हैंै । किन्तु मेरा अनुभव यह है कि जितनी गालियों का प्रयोग उत्तर प्रदेश के लोग अपनी भाषा में करते हैं, शायद कहीं पर नहीं होता। कुछ समय के लिए मैं बैंक में यू. पी. में थी। पूरी शाखा में मैं अकेली महिलाकर्मी थी। एक महिला की एफ. डी. का भुगतान तकनीकी कारणों से नहीं हो पा रहा था। मैं उसे समझाने का प्रयास कर ही थी, किन्तु वह बैंक के विरूद्ध गालियां जोड़कर बोलती जा रही थी। मैंने उसे रोका, गाली क्यों दे रही हो, कर तो रही हूं तुम्हारा काम। फिर चिल्लाकर वही गाली देते हुए बोली, मैंने किसे दी गाली, कब दी। प्रत्येक वाक्य में वही गाली दो-चार बार। मैं उसे रोकूं, वह बोले मैंने कब दी गाली, मैं शर्मिंदी से परेशान और सारे कर्मचारी हंस-हंसकर आनन्द ले रहे।
पुस्तक अध्ययन
समय के साथ पुस्तकों की उपलब्धता भी कम है। आज किसी भी पुस्तक-विक्रेता के पास आपको हिन्दी साहित्य की पठनीय पुस्तकें नहीं मिलेंगी। पहले अनेक पुस्तक-विक्रेताओं के पास हिन्दी साहित्य की पुस्तकें उपलब्ध होती थीं और हम बाज़ार में घूमते -फिरते ऐसी दुकानों पर जाकर पुस्तकों का अवलोकन कर लेते थे और खरीद भी लेते थे, अब आप किसी भी पुस्तक-विक्रेता के पास चले जाईये कोई हिन्दी पुस्तक नहीं मिलेगी
मेरी समझ में एक समय भी होता है जब हमारी रूचियां इस तरह की होती हैं। कभी ऐसा ही समय था जब घर में कोई पुस्तक आती थी तो उसे पूरा पढ़कर ही रहते थे, यद्यपि, शायद आज से अधिक ही व्यस्त जीवन था। हिन्दी में प्राचीन-अर्वाचीन साहित्य, संस्कृति से सम्बन्धित श्रेष्ठ पुस्तकें उपलब्ध हैं, शोध कार्य के समय इतनी पुस्तकें पढ़ीं कि कोई गिनती ही नही। किन्तु अब ध्यान ही नहीं जाता कि पुस्तक खरीदी जाये या पढ़ी जाये, हां कभी जब मन होता है तब पुरानी पुस्तकों को ही देख-परख कर आनन्द ले लिया जाता है। यानी धूल झाड़कर मन आनन्दित हो जाता है, कि वाह ! मेरे पास यह पुस्तक भी है, यह भी है और यह भी है।
पुस्तकें , पत्रिकाएं, समाचार-पत्र पढ़ने का समय था वह अब टी.वी. धारावाहिक और पी. सी. में समा गया है।
राजकमल प्रकाशन की भी एक योजना थी, शायद 1975-80 तक मैं उसकी सदस्य रही, पेपर बैक में आधे मूल्य में श्रेष्ठ साहित्यिक पुस्तकें उपलब्ध होती थीं। मात्र बीस रूपये में दो पुस्तकें और वर्ष में एक निःशुल्क पुस्तक भेंट स्वरूप प्राप्त होती थी। उस समय आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास, हिन्दी साहित्य, और न जाने कितने उपन्यास, कहानी-संग्रह और अनेक शब्द कोष मेरे संग्रह का हिस्सा बने। प्रकाशक से निरन्तर नवीन प्रकाशित पुस्तकों की जानकारी भी मिलती रहती थी। फिर कार्यक्षेत्र बदला, पढ़ना-लिखना कम हुआ, जानकारी घटी, सब छूटता चला गया। तीन-चार वर्ष पूर्व मैंने राजकमल प्रकाशन से पुनः सम्पर्क किया कि क्या उनकी अब कोई ऐसी योजना है एवं पुस्तकों की सूची मंगवाई। योजना तो नहीं थी किन्तु पुस्तकों का मूल्य देखकर मैं चकरा गई। वही पुस्तक जो मैंने उस समय हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास जो उस समय मैंने मात्र 10-15-20 रूपये में मंगवाये थे उनका मूल्य 1500 -1800 रूपये तक था। किन्तु यह सोचकर मन आनन्दित हुआ कि मेरे पास उपलब्ध पुस्तकें इतनी मूल्यवान हो चुकी हैं।
क्या ऑनलाइन रिश्ते ऑफलाइन रिश्तों पर हावी हो रहे हैं
मेरी दृष्टि में ऑनलाइन रिश्ते ऑफलाइन रिश्तों पर हावी नहीं हो रहे हैं, दोनों का आज हमारे जीवन में अपना-अपना महत्व है। हर रिश्ते को साधकर रखना हमें आना चाहिए, फिर वह ऑनलाइन हो अथवा ऑफलाइन ।
वास्तव में ऑनलाइन रिश्तों ने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है जो कहीं भी ऑफलाइन रिश्तों पर हावी नहीं है।
अब वास्तविकता देखें तो ऑफलाइन रिश्ते रिश्तों में बंधे होते हैं, कुछ समस्याएं, कुछ विवशताएं, कुछ औपचारिकताएं। यहां हर रिश्ते की सीमाएं हैं, बन्धन हैं, लेनदारी, देनदारी है, आयु-वर्ग के अनुसार मान-सम्मान है, जो बहुत बार इच्छा न होते हुए भी, मन न होते हुए भी निभानी पड़ती हैं। यहां हर रिश्ते की अपनी मर्यादा है, जिसे हमें निभाना ही पड़ता है। ऐसा बहुत कम होता है कि ये रिश्ते बंधे रिश्तों से हटकर मैत्री-भाव बनते हों।
किन्तु ऑनलाइन रिश्तों में कोई किसी भी प्रकार का बन्धन नहीं है। एक नयापन प्रतीत होता है, एक सुलझापन, जहां मित्रता में आयु, वर्ग का बन्धन नहीं होता। बहुत बार हम समस्याओं से घिरे जो बात अपनों से नहीं कर पाते, इस रिश्ते में बात करके सुलझा लेते हैं। एक डर नहीं होता कि मेरी कही बात सार्वजनिक न हो जाये।
हां, इतना अवश्य है कि रिश्ते चाहे ऑनलाइन हों अथवा ऑफलाइन, सीमाएं दोनों में हैं, अतिक्रमण दोनों में ही नहीं होना चाहिए।
क्या शिक्षा उपभोक्तावाद का शिकार हो गई है
क्या शिक्षा उपभोक्तावाद की शिकार हो गई है, इस विषय पर बात करने से पूर्व हमें उपभोक्तावाद शब्द को समझना होगा। वास्तव में उपभोक्तावाद का अर्थ वस्तुओं के उपयोग करने वाला जिसे हम consumerism कह सकते हैं। अर्थात शिक्षा के लिए यदि हम उपभोक्तावाद शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम स्पष्टतः शिक्षा को एक वस्तु के रूप में प्रयोग करने की बात कर रहे हैं।
दूसरे अर्थ में इस शब्द का अभिप्राय व्यवसाय, पूंजीवाद, व्यावसायीकरण, उद्योगवाद भी लिया जा सकता है।
इस अर्थ में यह बात तार्किक प्रतीत होती है कि शिक्षा उपभोक्तावाद से की शिकार है।
भारत में शिक्षा की एकरूपता नहीं है, कोई नियन्त्रण नहीं है, कोई समानता नहीं है। जिसका मन करता है अपनी इच्छा से विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खोल लेते हैं, बड़ी-बड़ी शैक्षणिक संस्थाएं खोल लेते हैं, बस धन और बल चाहिए। पाठ्यक्रम में कहीं एकरूपता नहीं है, जो प्रकाशक कमीशन देता है उसकी पुस्तकें पाठ्यक्रम में लगा दी जाती हैं। एन.सी.आर.टी. की पुस्तकें केवल सरकारी विद्यालयों तक सीमित रह गई हैं जहां शिक्षकों को तो असीमित सुविधाएं, वेतन, अवकाश हैं किन्तु विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं। वहीं दूसरी ओर निजी शिक्षण संस्थाएं एक पंचसितारा व सात सितारा होटलों के समान हैं। दूसरी ओर प्राईवेट ट्यूशन।
इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम अर्थहीन होता जा रहा है, व्यवसायिक पाठ्यक्रम न के बराबर हैं और शिक्षा के वर्ष बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान शिक्षा कहीं भी रोज़गारोन्मुख नहीं है।
अर्थात जिसके पास धन है वह यहां खड़ा है शेष या तो बेरोज़गार होकर भटक रहे हैं, राहों से भटक रहे हैं ।
तो कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यवसाय, पूंजीवाद, व्यावसायीकरण, उद्योगवाद के रूप में उपभोक्तावाद की शिकार हो गई है।
उत्सव-खुशी और आतिशबाजी की तार्किकता
दीपावली के अवसर पर सदैव ही आतिशबाजी होती रही है। किन्तु आज आतिशबाजी से पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण इसे प्रतिबन्धित करने की बात की जाती है।
आतिशबाजी चलाने वाले इसे अपने घर नहीं बनाते । वे किसी छोटे दुकानदार से खरीद कर लाते हैं। छोटा दुकानदार किसी थोक व्यापारी से लाता है और थोक-व्यापारी आतिशबाजी बनाने वाली फ़ैक्ट्री से, और इस कार्य के लिए ये सरकार से लाईसेंस लेते हैं अथवा कुछ अवैध भी बनाते हैं। अर्थात शुरुआत आशिबाजी चलाने वालों की ओर से नहीं, सरकार की ओर से होती है।
फिर आजकल हरी आतिशबाजी का प्रदर्शन भी हो रहा है, क्रेता कहां जान पाता है कि आतिशबाजी हरी है, काली या नीली। जो मिलती है ले लेते हैं। हां, इतना अवश्य है कि हरी आशिबाजी के नाम पर खूब लूट हो रही है। ध्वनि प्रदूषण तो उससे भी होता ही होगा।
कहने का अभिप्राय यह कि हम मूल की ओर तो जाते ही नहीं, केवल आंखों देखी पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, बुराई करते हैं। यदि आतिशबाजी इतनी ही हानिकारक है तो इनकी फ़ैक्ट्रियों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहिए। कह सकते हैं कि इससे रोज़गार पर प्रभाव पड़ेगा, तो यह भी सरकार का ही कार्य है कि ऐसी फ़ैक्ट्रियों को किसी नवीन निर्माण सामग्री के लिए सहयोग प्रदान करे।
कोर्ट का आदेश जनता के लिए है सरकार के लिए क्यों नहीं। और उससे भी अधिक विचारणीय बात यह कि नेताओं की विजय पर भी खूब आतिशबाजी होती है, नववर्ष एवं कुछ अन्य धर्मों के गुरुओं के दिवस पर भी आतिशबाजी होती है, तब क्या प्रदूषण नहीं होता। मेरा यह अभिप्राय कदापि नहीं कि इस कारण हिन्दू पर्वों पर आतिशबाजी की छूट दी जाये, किन्तु नियन्त्रण हर रूप में किया जाना चाहिए।
अतः इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे आतिशबाज़ी का निर्माण ही बन्द हो, और समय की आवश्यकतानुसार इन्हें किसी नये काम के लिए सरकार की ओर से सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं।
यह बात बिल्कुल वैसी ही है कि प्लास्टिक के लिफ़ाफ़े प्रयोग करने पर सब्ज़ी बेचने वाले का 500 रुपये का चालान काटा जाता है किन्तु बनाने वाले बना रहे हैं, उन पर कोई रोक नहीं।