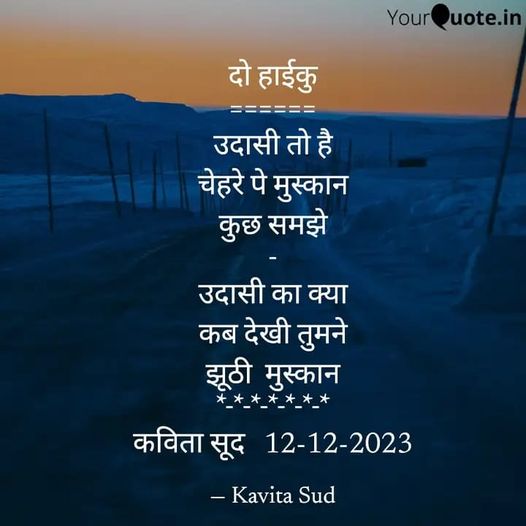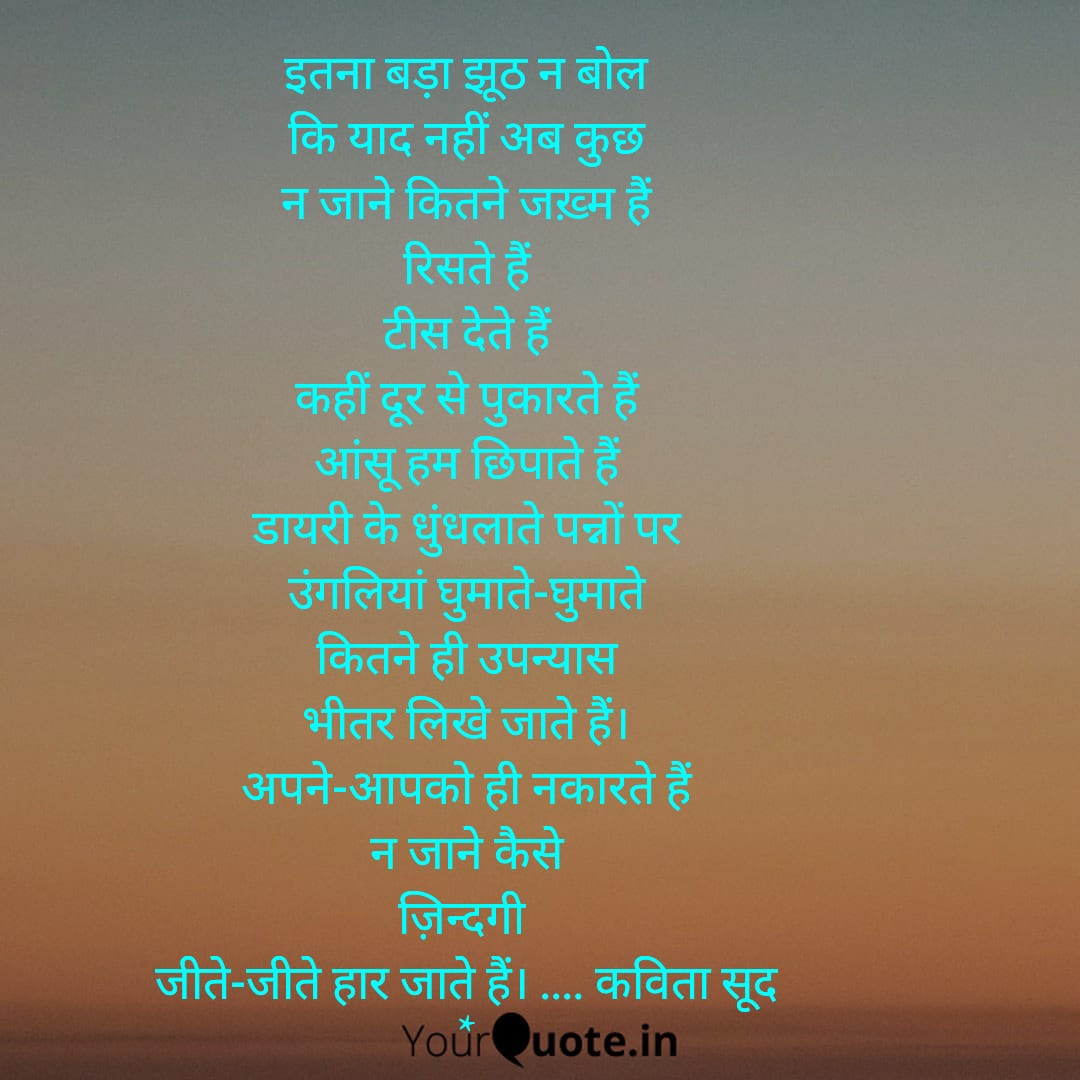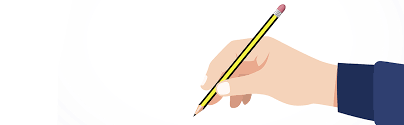अपनेपन की चाह
2-1-2023 को आँख के आपरेशन के बाद फ़ेसबुक से कुछ दिन की दूरी के बाद अब जैसे मन ही नहीं लग रहा लिखने और काम करने पर। न जाने क्यों।
मित्रों की मन से शुभकामनाएँ मिलीं, मन आह्लादित हुआ। मित्रों की चिन्ता, पुनः लिखने की प्रेरणा, मंच से जुड़ने का आग्रह, मन को छू गया।
विचारों में उथल-पुथल है, असमंजस है।
हाँ, यह बात तो सत्य है कि हमारी अनुपस्थिति प्रायः किसी के ध्यान में नहीं आती। किन्तु मैं भी यही सोच रही थी कि मेरे साथ अनेक मंचों पर और सीधे भी कितने ही मित्र जुड़े हैं, मैं भी तो किसी की अनुपस्थिति की ओर कभी ध्यान नहीं देती।
मेरे संदेश बाक्स, एवं वाट्सएप में भी प्रायः प्रतिदिन कुछ मित्रों के सुप्रभात, शुभकामना संदेश, वन्दन, शुभरात्रि के संदेश अक्सर प्राप्त होते हैं। मैं कभी उत्तर देती हूँ और कभी नहीं। ऐसा तो नहीं कि मेरे पास इतने दो पल भी नहीं होते कि मैं उनके अभिवादन का एक उत्तर भी न दे सकूँ। आज सोच रही हूँ कि मैं कैसे किसी से मिल रही शुभकामनाओं की उपेक्षा कर सकती हूँ, किसी भी दृष्टि से इसे उचित तो नहीं कहा जा सकता। तो मैं कैसे किसी से अपेक्षा करने का अधिकार रखती हूँ।
अब एक अन्य पक्ष है।
मैं प्रतिवर्ष होली, दीपावली एवं नववर्ष पर अपने अधिकाधिक मित्रों को बधाई संदेश भेजने का प्रयास करती ही हूँ। वे सभी मित्र, जो मेरे साथ अनेक मंचों पर जुड़े हैं, नियमित विचारों, प्रतिक्रियाओं का आदान-प्रदान है एवं कुछ मित्र जो सीधे फ़ेसबुक पटल पर मेरे साथ जुड़े हैं, कुछ पुराने सहकर्मी, सम्बन्धी, अन्य रूपों में परिचित, अथवा केवल फ़ेसबुकीय परिचय, जिनसे कहीं विचारों का आदान-प्रदान चलता रहता है, चाहे वह लाईक्स अथवा इमोज़ी के रूप में ही क्यों न हो। इसके अतिरिक्त मेरे पुराने सहकर्मी, जो मेरे साथ फ़ेसबुक पर हैं अथवा वाट्सएप पर हैं। मेरा प्रयास रहता है कि मैं इन सभी मित्रों को अवश्य ही इन पर्वों पर शुभकामना संदेश प्रेषित करुँ। पिछले अनेक वर्षों से मैं ऐसा करती रही हूँ। मैं वास्तविक संख्याबल तो नहीं जानती किन्तु सैंकड़ों में तो हैं ही, जिन्हें इन पर्वों पर शुभकामना संदेश भेजती आई हूँ, वर्षों से।
किन्तु इस बार मनःस्थिति अन्यमनस्क होने के कारण मैं सभी मित्रों को नववर्ष पर शुभकामना संदेश नहीं भेज पाई। किन्तु प्रतीक्षा तो थी कि जिन्हें मैं हरवर्ष स्मरण करती हूँ वे मुझे अवश्य ही स्मरण करेंगे, किन्तु ऐसा नहीं हुआ।
आश्चर्य मुझे किसी से प्रथमतः संदेश नहीं मिले।
बस दिल पर नहीं लिया, लिखने का मन था लिख दिया।
आप सभी मित्रों को पूरे वर्ष, प्रतिदिन के लिए अशेष शुभकामनाएँ।
निर्माण के जंगल
हम जब मुख्य शहर से कुछ बाहर, कुछ दूर निकलते हैं तो आपको societies एवं उनमें निर्माणाधीन Flats /Towers दिखाई देने लगते हैं। एक-एक society में 100-200 टॉवर, और 22-25 मंजिल तक, सभी निमार्णाधीन। और एक दो नहीं, सैंकड़ों-सैंकड़ों, जिन्हें आप न तो गिन सकते हैं न ही अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कोई बाढ़ आ गई हो, सुनामी हो Flats की, अथवा कोई पूरा जंगल। किन्तु इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह कि ये सब अधबने Flats हैं, केवल ढांचा अथवा कहीं-कहीं बाहर से बने दिखाई देते हैं किन्तु भीतर से केवल दीवारें ही होती हैं जिन्हें उनकी शब्दावली में Raw कहा जाता है। मीलों तक, पूरे-पूरे शहर के समान। इनके आस-पास निर्माणाधीन मॉल, बिसनेस टॉवर, सिटी सैंटर, बड़ी-बड़ी कम्पनियों के बोर्ड। मॉल भी इतने बड़े और उंचे कि आप नज़र उठाकर न देख सकें, कहॉं से आरम्भ हो रहे हैं और कहॉं कितनी दूर समाप्त, दृष्टि बोध ही नहीं बन पाता।
अब आप यहॉं Flat खरीदने के लिए देखने जायेंगे तो आपको society एवं Flats की विशेषताएं बताई जायेंगी।
society में swimming pool, park, fountains, power back up, parking area, party hall, community hall, community centre, high level security, religious places, plumber, mechanic, electrician सबकी सुविधाएं मिलती रहेंगी, वगैरह-वगैरह।
फिर आप मूल्य पूछेंगे।
छोटे-छोटे 3 BHK Flats का मूल्य मात्र 2 से ढाई करोड़ से आरम्भ होता है और ये अभी निर्माणाधीन हैं। केवल ढांचे खड़े हैं। आप 25 प्रतिशत राशि देकर बुक करवा सकते हैं, ज्यों-ज्यों निर्माण होता जायेगा, आपसे शेष राशि किश्तों में ली जाती रहेगी। तीन, चार अथवा पांच वर्षों में आपको तैयार Flat मिल जायेगा। ये बैंक से भी आपका ऋण स्वीकृत करवा देंगे।
और उपर बताई गई सुविधाओं के लिए आपसे मात्र 2 अथवा 3 प्रतिशत मासिक लिया जायेगा।
इन Flats को देखकर मेरे मन में दो-तीन प्रश्न उठते हैं।
इन लाखों Flats में बसने वाले लोग किस ग्रह से आयेंगे।
दूसरा भारत में क्या सत्य में ही इतने धन-सम्पन्न लोग हैं?
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यह कि मुझे इन societies में दूर-दूर तक किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शिक्षण संस्थान, व्यावसायिक संस्थान, अस्पताल, डिस्पैंसरी, क्लिीनिक की परिकल्पना नहीं दिखाई दी।
आप क्या सोचते हैं।
मेरे आस-पास की आम-सी नारी वो खास
कैसे लिखूँ किसी एक के बारे में। मेरे आस-पास की तो हर नारी खास है किसी न किसी रूप में। चाहे वह गृहिणी है, कामकाजी है, किसी ऊँचे पद पर अवस्थित है, मज़दूर है, सुशिक्षित है, अशिक्षित है, कम या ज़्यादा पढ़ी-लिखी है, हर नारी किसी न किसी रूप में खास ही है। किसी न किसी रूप में हर नारी मेरे लिए प्रेरणा का माध्यम बनती है।
मेरे परिचय में एक महिला जो स्वयं दिल की रोगी है, चिकित्सकों के अनुसार उसका दिल केवल 55 प्रतिशत कार्य करता है, पूरा घर सम्हालती है, पति भी अस्वस्थ रहते हैं उनकी पूरी देखभाल करती है। उन्हें कार में अस्पताल लाना, ले जाना आदि सब। बच्चे विदेश में हैं। किन्तु इस बात की कभी शिकायत नहीं करती।
मेरे घर काम करने वाली महिला अपने तीन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रही है, चार घरों में काम करती है, उपरान्त पति के काम में हाथ बंटाती है।
बस हम एक भ्रम में जीते हैं कि कोई नारी खास है। कहाँ खास हो पाती है कोई नारी। बस भुलावे में जीते हैं और भुलावों में सबको रखते हैं। कोई नारी किसी बड़े पद पर कार्यरत है, कोई बहुत पुरस्कारों से सम्मानित है, बड़ी लेखिका, कलाकार अथवा अन्य किसी क्षेत्र में जाना-पहचाना नाम है, किन्तु फिर भी खास कहाँ बन पाती हैं वे। अपने आस-पास मुझे एक भी ऐसी नारी कभी नहीं मिली जो अपने मन से, अपने अधिकार से, अपनी इच्छाओं से जीवन व्यतीत करती हो। फिर कोई नारी खास कैसे हो सकती है। मेरी इस बात पर आप शायद कहेंगे कि नारी को तो परिवार को भी देखना होता है, बच्चों का पालन-पोषण, बड़ों की सेवा, छोटों को संस्कार, भला कौन देगा, ऐसी ही नारी तो खास होती है। यह तो हर नारी का हमारी दृष्टि में कर्तव्य है, इसमें कोई खास बात कहाँ।
मुझे आज तक ऐसी कोई नारी नहीं मिली, जो अपने मन से जीती हो, अपनी इच्छाओं का दमन न करती हो, दोहरी ज़िन्दगी न जीती हो। संस्कारी भी बनकर रहना है और समय के साथ चलने के लिए आधुनिका भी बनना है। गृहस्थी तो उसका दायित्व है ही, किन्तु पढ़ी-लिखी है, तो नौकरी भी करे और बच्चों को भी पढ़ाए। आप कहेंगे यह तो नारी के कर्तव्य हैं। तो खास कैसे हुई। मैंने आज तक ऐसी कोई नारी नहीं देखी जो मन से स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र होने का अभिप्राय उच्छृंखलता, दायित्वों की उपेक्षा नहीं होता, इसका अभिप्राय होता है कि वह अपने मन से अपने लिए कोई निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र है। परिवार के प्रत्येक कार्य में वह भागीदार है, उसे हर कदम पर साथ लेकर चला जाता है, उसकी इच्छा-अनिच्छा का आदर किया जाता है।
माता-पिता आज भी लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ाते कि पढ़ाना चाहते हैं बल्कि इसलिए पढ़ाते हैं कि लड़के आजकल पढ़ी-लिखी लड़की ढूंढते हैं और अक्सर नौकरी वाली। किन्तु अगर किसी लड़के को लड़की तो पसन्द आ जाती है किन्तु परिवार कहता है कि हमें नौकरी नहीं करवानी तो लड़की के माता-पिता और स्वयं लड़की भी इसी दबाव में नौकरी न करना स्वीकार कर लेती है।
कौन-सी संस्कृति
जब भी कोई अनहोनी घटना होती है, युवा पीढ़ी के प्रेम-प्रसंगों की दुर्घटनाएँ होती हैं, किसी के घर से भागने, माता-पिता की अनुमति के बिना विवाह कर लेने, विवाहत्तेर सम्बन्धों के बो में, लिव-इन-रिलेशनशिप के बारे में, माता-पिता से अलगाव होने की स्थिति में, हम तत्काल एक आप्त वाक्य बोलने लग जाते हैं ‘‘पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से यह सब हो रहा है। हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। हम आधुनिकता के पीछे भाग रहे हैं। हम अपने संस्कारों, बड़े-बुज़ुर्गों का मान नहीं करते।’’ आदि-आदि।
मुझे विदेशी संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है। मैं कभी गई नहीं, मैं वहाँ की जीवन-शैली के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। हाँ, केवल इतना ज्ञान है कि विदेशों में बच्चे माता-पिता को घर से नहीं निकालते, अपितु माता-पिता बच्चों को एक निश्चित आयु के बाद स्वतन्त्र कर देते हैं, उनका अपना जीवन जीने के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए। अलग घर, अलग व्यवस्था। दोनों ही परस्पर निर्भर नहीं होते, स्वतः स्वतन्त्र होते हैं, किन्तु सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता। पुरुष-स्त्री सम्बन्धों में वहाँ खुलापन है जो सामाजिक तौर पर सहज स्वीकृत है। पारिवारिक व्यवस्था वहाँ भी है किन्तु सम्भवतः गान नहीं है। बस मुझे इतनी-सी ही जानकारी है।
मैं समझती हूँ कि इस बात पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए कि वह कौन सी विदेशी संस्कृति है जिससे हमारी युवा पीढ़ी इतनी पथभ्रट हो रही है अथवा हम अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसा कहने लग गये हैं। और मेरे मन में यह भी विचार आता है कि क्या सच में ही हमारी पीढ़ी पथभ्रष्ट है अथवा बस हमें लिखने के लिए मसाला चाहिए इस कारण हम ऐसा लिखने लगे हैं। सादर
प्रायः सब विचारक यह मानते हैं कि हमारे युवा पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से बिगड़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि कृपया विस्तार से बतायें कि किस देश की संस्कृति से हमारे युवा अधिक प्रभावित हैं और कौन सी ऐसी बुरी विदेशी संस्कृति है जिसने हमारे युवाओं को इतना पथभ्रष्ट कर दिया है।
कृपया मेरा ज्ञानवर्धन करें। अति कृपा होगी।
आप अकेली हैं
आप अकेली हैं?
सहयात्री का यह अटपटा-सा प्रश्न नीता को चकित कर गया।
दो सीट के कूपे में बैठी नीना ने सामने बैठे सहयात्री को फिर भी कुछ मुस्कुराकर और कुछ व्यंग्य से उत्तर दिया, जी हां, क्यों क्या हुआ, आपको कोई परेशानी ?
और नीना का कटु प्रतिप्रश्न, आपके साथ कौन है?
लगभग 45 वर्ष का वह सहयात्री अभी भी नीता को अलग-सी दृष्टि से देख रहा था, बोला, नहीं, नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि आप महिला होकर अकेली इतनी दूर जा रही हैं, किसी को साथ लेकर चलना चाहिए न आपको। फिर आपकी आयु और आजकल वैसे भी माहौल कहां ठीक है, 22 घंटे की यात्रा। कोई परेशानी हो तो आपको मुश्किल हो सकती है।
अब नीना का गुस्सा सदा की तरह सातवें आसमान पर था।
एकदम कटु स्वर में बोली, 22 घंटे की यात्रा तो आपके साथ है तो आपका कहने का अभिप्राय यह कि मुझे आपसे डरना चाहिए क्यों?
इससे पहले कि वह सहयात्री कुछ उत्तर दे, नीना वास्तव में फ़ट पड़ी, क्यों यही कह रहे हैं न आप कि मुझे आपसे डरना चाहिए।
आप तो एकदम ही नाराज़ हो गईं, मैं कोई ऐसा-वैसा नहीं हूॅं, मैं तो आपकी ही चिन्ता कर रहा था। महिलाओं की सुरक्षा की चिन्ता ही करते हैं हम तो। आप तो पता नहीं क्या गलत समझ बैठीं।
आप कौन लगते हैं मेरे जो मेरी चिन्ता कर रहे हैं?
वैसे आप भी तो अकेले ही हैं, आपके साथ कौन है? नीना ने पूछा।
नहीं, मुझे क्या परेशानी अकेले में। मैं तो अक्सर ही अकेले आता-जाता हूॅं, ।
अच्छा, जो परेशानी मुझे अकेली को हो सकती है, जिसके लिए आप मेरी इतनी चिन्ता कर रहे हैं क्या आपको नहीं हो सकती?
मुझे क्या परेशानी होगी मैडम। मैं तो आदमी हूॅं, परेशानी तो औरतों को होती है और उस अजनबी ने दांत निपोर दिये।
अब नीना असली मूड में आई और बड़ी सुन्दर मुस्कान से बोली, क्यों, आपको हार्ट अटैक, पैरालिसीस, ब्रेन हैमरेज, कहीं ठोकर, फ्ैक्चर नहीं हो सकता। और क्या आपके साथ कोई दुव्र्यवहार नहीं कर सकता।
और सर, मैं तो आपके कुछ किये बिना भी चिल्ला दूंगी कि यह व्यक्ति मेरे साथ दुव्र्यवहार कर रहा है , आपको अभी गाड़ी से नीचे उतार देंगे धक्के मारकर, किन्तु मैं आपके साथ कुछ भी करुॅं आपकी बात का तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा, बोलिए करुॅं कुछ?
इतने में वहां से टी टी निकला।
वह आदमी चिल्लाया, सुनिए, किसी दूसरे कूपे में कोई सीट खाली है क्या, मेरी बदल सकते हैं क्या?
टी टी, चकित-सा दोनों को देख रहा था।
इस बीच नीना बोली, महाशय, हम औरतों की आप लोग चिन्ता न करें तो हम ज़्यादा सुरक्षित और निश्चिंत रहती हैं, आप बस अपना देखिए।
बदलवा लीजिए सीट या गाड़ी ही बदल लीजिए। कहीं कुछ हो न जाये आपके साथ।
हमारी हिन्दी
हिन्दी सबसे प्यारी बोली
कहॉं मान रख पाये हम।
.
रोमन में लिखते हिन्दी को
वर्णमाला को भूल रहे हम।
मानक वर्णमाला कहीं खो गई है
42, 48, 52 के चक्कर में फ़ंसे हुए हैं हम।
वैज्ञानिक भाषा की बात करें तो
बच्चों को क्या समझाएॅं हम।
उच्चारण, लेखन का सम्बन्ध टूट गया
कुछ भी लिखते
कुछ भी बोल रहे हम।
चन्द्रबिन्दु गायब हो गये
अनुस्वर न जाने कहॉं खो गये
उच्चारण को भ्रष्ट किया,
सरलता के नाम पर
शुद्ध शब्दों से भाग रहे हम।
अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी को
सरल कहकर हिन्दी को
नकार रहे हम।
शिक्षा से दूर हो गई,
माध्यम भी न रह गई,
न जाने किस विवशता में
हिन्दी को ढो रहे हैं हम।
ऑनलाईन अंग्रेज़ी के माध्यम से
हिन्दी लिख-पढ़ सीख रहे हैं हम।
अंग्रेज़ी में अंग्रेज़ी लिखकर
उससे हिन्दी मॉंग रहे हम।
अनुवाद की भाषा बनकर रह गई है
इंग्लिश-विंग्लिश लिखकर
गूगल से कहते हिन्दी दे दो,
हिन्दी दे दो।
फिर कहते हैं
हिन्दी सबसे प्यारी बोली
हिन्दी सबसे न्यारी बोली।
जीना चाहती हूं
छोड़ आई हूं
पिछले वर्ष की कटु स्मृतियों को
पिछले ही वर्ष में।
जीना चाहती हूं
इस नये वर्ष में कुछ खुशियों
उमंग, आशाओं संग।
ज़िन्दगी कोई दौड़ नहीं
कि कभी हार गये
कभी जीत गये
बस मन में आशा लिए
भावनाओं का संसार बसता है।
जो छूट गया, सो छूट गया
नये की कल्पना में
अब मन रमता है।
द्वार खोल हवाएं परख रही हूं।
अंधेरे में रोशनियां ढूंढने लगी हूं।
अपने-आपको
अपने बन्धन से मुक्त करती हूं
नये जीवन की आस में
आगे बढ़ती हूं।
मेरे साहस से
दया भाव मत दिखलाना।
लड़की-लड़की कहकर मत जतलाना।
बेटियों के अधिकारों की बात मत उठाना।
हो सके तो सरकार को समझाना।
नित नई योजनाएं बनती हैं
उनको कभी तो लागू भी करवाना।
सुना है मैंने नदियों का देश है
एक नदी मेरे घर तक भी ले आना।
बोतलों में बन्द पानी की दुकानें लगी हैं
कभी मेरी गागर का पानी पीकर
अपनी प्यास बुझाना।
कभी तो हमारे साथ आकर
गागर उठवाना।
तुम पूछोगे
स्कूल नहीं जाती क्या
मेरे गांव में भी एक
बड़ा-सा स्कूल खुलवाना।
मेरा चित्र खींच-खींचकर
प्रदशर्नियों में धन कमाते हो,
कभी मेरी जगह खड़े होकर
गागर लेकर,
धूप, छांव, झडी में
नंगे पांव
कुएं तक चलकर जाना।
फिर मेरे साहस से
अपने साहस का मोल-भाव करवाना।
*-*-*-*-*-*
आओ अपने-आपसे बातें करें
आओ बातें करें
अपने-आपसे बातें करें।
इससे पहले
कि लोग हमसे
कुछ पूछें, कुछ कहें,
अपने-आपसे बात कर लें।
अपने-आपसे
कुछ पूछें, कुछ कहें।
न जाने कितने प्रश्न
अनुत्तरित हैं
मेरे भीतर।
न कह पाती हूं
न पूछ पाती हूं
बस उलझी-सी रहती हैं।
चलो,
आज उलझनों को सुलझा लें।
चाहो,
तो बैठ सकते हो मेरे साथ,
सुन सकते हो मेरी बात,
चल सकते हो मेरे साथ
पर बस
उतना ही समझना
जो मैं समझना चाहती हूं
उतना ही कहना
जो मैं कहना चाहती हूं
वही कहना
जो मैं कहना चाहती हूं
मुझसे बस
मेरी बात करना,
आज बस इतना ही करना।
आवरण से समस्याएं नहीं सुलझतीं
समझ नहीं आया मुझे,
किसके विरोध में
तीर-तलवार लिए खड़ी हो तुम।
या इंस्टा, फ़ेसबुक पर
लाईक लेने के लिए
सजी-धजी चली हो तुम।
साड़ी, कुंडल, करघनी, तीर
मैचिंग-वैचिंग पहन चली,
लगता है
किसी पार्लर से सीधी आ रही हो
कैट-वाॅक करती
अपने-आपको
रानी झांसी समझ रही हो तुम।
तिरछी कमान, नयनों के तीर से
किसे घायल करने के लिए
ये नौटंकी रूप धरकर
चली आ रही हो तुम।
.
लगता है
ज़िन्दगी से पाला नहीं पड़ा तुम्हारा।
तुम्हें बता दूं
ज़िन्दगी की लड़ाईयां
तीर-तलवार से नहीं लड़ी जातीं
क्या नहीं जानती हो तुम।
ज़िन्दगी तो आप ही दोधारी तलवार है
शायद आज तक चली नहीं हो तुम।
कभी झंझावात, कभी आंधी
कभी घाम तीखी,
शायद झेली नहीं हो तुम।
.
कल्पनाओं से ज़िन्दगी नहीं चलती।
आवरण से समस्याएं नहीं सुलझतीं।
भेष बदलने से पहचान नहीं छुपती।
अपनी पहचान से गरिमा नहीं घटती।
इतना समझ लो बस तुम।
दर्द सच न बोल बैठे
रहने दो मत छेड़ो दर्द को
कहीं सच न बोल बैठे।
राहों में फूल थे
न जाने कांटे कैसे चुभे।
चांद-सितारों से सजा था आंगन
न जाने कैसे शूल बन बैठे।
हरी-भरी थी सारी दुनिया
न जाने कैसे सूखे पल्लव बन बैठे।
सदानीरा थी नदियां
न जाने कैसे हृदय के भाव रीत गये।
रिश्तों की भीड़ थी मेरे आस-पास
न जाने कैसे सब मुझसे दूर हो गये।
स्मृतियों का अथाह सागर उमड़ता था
न जाने कैसे सब पन्ने सूख गये।
सूरज-चंदा की रोशनी से
आंखें चुंधिया जाती थीं
न जाने कैसे सब अंधेरे में खो गये।
बंद आंखों में हज़ारों सपने सजाये बैठी थी
न जाने कैसे आंख खुली, सब ओझल हो गये।
नहीं चाहा था कभी बहुत कुछ
पर जो चाहा वह भी आप लेकर चले गये।
कल से डर-डरकर जीते हैं हम
आज को समझ नहीं पाते
और कल में जीने लगते हैं हम।
कल किसने देखा
कौन रहेगा, कौन मरेगा
कहां जान पाते हैं हम।
कल की चिन्ता में नींद नहीं आती
आज में जाग नहीं पाते हैं हम।
कल के दुख-सुख की चिन्ता करते
आज को पीड़ा से भर लेते हैं हम।
बोये तो फूलों के पौधे थे
पता नहीं फूल आयेंगे या कांटे
चिन्ता में
सर पर हाथ धरे बैठे रहते हैं हम।
धूप खिली है, चमक रही है चांदनी
फूलों से घर महक रहा
नहीं देखते हम।
कल किसी ने न देखा
पर कल से डर-डरकर जीते हैं हम।
.
कल किसी ने न देखा
लेकिन कल में ही जी रहे हैं हम।
दो हाईकु
उदासी तो है
चेहरे पे मुस्कान
कुछ समझे
-
उदासी का क्या
कब देखी तुमने
झूठी मुस्कान
आगमन बसन्त का
बसन्त
यूं ही नहीं आ जाता
कि वर्ष बदले,
तिथि बदली,
दिन बदले
और लीजिए
आ गया बसन्त।
मन के उपवन में
सुमधुर भावों की रिमझिम
कहीं धूप, कहीं छाया निखरी।
पल्ल्व मचल रहे
ओस की बूंदे बिखरीं,
कलियां फूल बनीं
रंगों में रंग खिले।
कहीं कोयल कूकी,
कुछ खुशबू
कुछ रंगों के संग
महका-बहका मन
मन का इन्द्रधनुष
कौन समझ पाया है
मन के रंगों को
मन की तरंगों को।
अपना ही मन
अपने ही रंगों को
संवारता है
बिखेरता है
उलझता है
और कभी उलझाता है।
मन का इन्द्रधनुष
रंगों की आभा को
निरखता है,
निखारता है,
तूलिका से
किसी पटल पर उकेरता है।
एक रूप देने का प्रयास
करती हूं
भावों को, विचारों को।
मन विभोर होता है।
आनन्द लेती हूं
रंगों से मन सराबोर होता है।
झूठ न बोल
इतना बड़ा झूठ न बोल
कि याद नहीं अब कुछ
न जाने कितने जख़्म हैं
रिसते हैं
टीस देते हैं
कहीं दूर से पुकारते हैं
आंसू हम छिपाते हैं
डायरी के धुंधलाते पन्नों पर
उंगलियां घुमाते-घुमाते
कितने ही उपन्यास
भीतर लिखे जाते हैं।
अपने-आपको ही नकारते हैं
न जाने कैसे
ज़िन्दगी
जीते-जीते हार जाते हैं।
आस लगाई
जिस-जिससे आस लगाई
उस-उसने बोला भाई।
-
मैं लेकर आया था
हार सुनहरा
बाद में वो बहुत पछताई।
फिर वो लौट-लौटकर आई
बार-बार हमसे आंख मिलाई।
हमने भी आंखें टेढ़ी कर लीं,
फिर वो लेकर राखी आई।
हमने भी धमकाया उसको
हम न तेरे भाई, हम न तेरे साईं।
बोले, अगर फिर लौटकर आई
तो बुला लायेंगे तेरी माई।
ज़िन्दगी की पूरी कहानी
लिखने को तो
ज़िन्दगी की
पूरी कहानी लिख दूं
दो शब्दों में।
लेकिन नयनों में आये भाव
तुम नहीं समझते।
चेहरे पर लिखीं
लकीरें तुम नहीं पढ़ते।
भावनाओं का ज्वार
तुम नहीं पकड़ते।
तो क्या आस करूं तुमसे
कि मेरी ज़िन्दगी की कहानी
दो शब्दों की ज़बानी
तुम कहां समझोगे।
ये कैसा सावन ये कैसा पानी
सावन की बरसे बदरिया
सोच-सोच मन घबराये।
बूंदें कब
जल-प्लावन बन जायेंगी
कब बहेगी धारा
सोच-सोच मन डर जाये।
-
नदिया का पानी
तट-बन्धों से जब टकराए
कब टूटेंगी सीमाएं
रात-रात नींद न आये।
-
बिजली चमके
देख रहे, लाखों घर डूबे
कितनी गई जानें
मन सहम-सहम जाये।
-
कब आसमान से आयेगी विपदा
कौन रहेगा, कौन जायेगा
हाथों से हाथ छूट रहे
न जाने ये कैसे दिन आये।
.
पुल टूटू, राहें बिखर गईं
खेतों में सागर लहराया
सूनी आंखों से ताक रहा किसान
देख-देख मन भर आये।
.
न सिर पर छत रही
न पैरों के नीचे धरा रही
कहां जा रहे, कहां आ रहे
कंधों पर लादे ज़िन्दगी
न जाने हम किस राह निकल आये।
-
कैसी विपदा ये आई
हाथ बांध हम खड़े रह गये
लूट ले गया घर-घर को
जल का तांडव,
कब निकलेगा पानी
कब लौटेंगे जीवन में
नहीं, नहीं, नहीं, हम समझ पाये।
होली पर्व
जीवन को रंगीन बनाओ
कहती आई है होली
जीवन-संगीत सुनाओ
कहती आई है होली
आनन्द के ढोल बजाओ
कहती आई है होली
जीवन का राग
सुनाती आई है होली
मन में आनन्द के भाव
जगाती है होली
रंगों और रंगीनियों का नाम
है होली
कोई एक ही दिन क्यों
मन चाहे तो रोज़ मनाओ होली।
जीवन में
हर रोज ही आती है होली।
-
कहते हैं
आई है होली।
क्या हो ली,
कैसे हो ली?
अपनी तो समझ ही न आई
क्या-क्या हो ली।
क्या किसी से मुहब्बत होली?
किसके साथ किसकी होली
किस-किसके घर होली
मुझसे पूछे बिना
कैसे होली
किसके दम पर होली।
सच बोलो
लगता है
तुमने खा ली भांग की गोली।
तेरा साथ
तेरा साथ
न छूटे कभी हाथ।
सोचती थी मैं,
पर
कब दिन ढला
कब रात हुई,
डूबे चंदा-तारे
ऐसी ही कुछ बात हुई।
*-*
तेरा साथ
हाथों में हाथ।
न कांटों की चुभन
न मन में कोई शूल
ऐसी ही ज़िन्दगी
सरगम
न टूटे कभी,
होगा क्या ऐसा।
औरत का गुणगान करें
चलो,
आज फिर
औरत का गुणगान करें।
चूल्हे पर
पकती रोटी का
रसपान करें।
कितनी सरल-सीधी
संस्कारी है ये औरत
घूँघट काढ़े बैठी है
आधुनिकता से परे
शील की चादर ओढ़े बैठी है।
लकड़ी का धुआँ
आँखों में चुभता है
मन में घुटता है।
पर तुमको
बहुत भाता है
संसार भर में
मेरी मासूमियत के
गीत गाता है।
आधुनिकता में जीता है
आधुनिकता का खाता है
पर समझ नहीं पाती
कि तुमको
मेरा यही रूप क्यों सुहाता है।
मौसम बदलता है या मन
मौसम बदलता है या मन
समझ नहीं पाते हैं हम।
कभी शीत ऋतु में भी
मन चहकता है
कभी बसन्त भी
बहार लेकर नहीं आता।
ग्रीष्म में मन में
कोमल-कोमल भाव
करवट लेने लगते हैं
तब तपन का
एहसास नहीं होता
और शीत ऋतु में
मन जलता है।
मौसम बदलता है या मन
समझ नहीं पाते हैं हम।
सृजनकर्ता का आभार
उस सृजनकर्ता का
आभार व्यक्त नहीं कर पाती मैं
जिसने इतने सुन्दर,
मोहक संसार की रचना की।
उस आनन्द को
व्यक्त नहीं कर सकती मैं
जो इस सृष्टिकर्ता ने
हमें दिया।
उससे ही मिले
आकाश को विस्तार देकर
गर्वोन्नत होने लगते हैं हम।
उससे मिली अमूल्य धरोहर को
अपना कहकर
अधिकार जमाने लगते हैं हम।
भूल जाते हैं उसे।
-
किन्तु नहीं जानते
कब जीवन में सब
उलट-पुलट हो जायेगा,
खाली हो जायेंगे हाथ।
और ये खाली हाथ
जुड़ जायेंगे
उसकी सत्ता स्वीकार करते हुए।
पानी के बुलबुलों सी ज़िन्दगी
जल के चिन्ह
कभी ठहरते नहीं
पलभर में
अपना रूप बदलकर
भाग जाते हैं
बिखर जाते हैं
तो कभी कुछ
नया बना जाते हैं।
छलक-छलक कर
बहुत कुछ कह जाते हैं
हाथों से छूने पर
बुलबुलों से
भाग जाते हैं।
लेकिन कभी-कभी
जल की बूंदें भी
बहुत गहरे
निशान बना जाती हैं
जीवन में,
बस हम अर्थ
ढूंढते रह जाते हैं।
और ज़िन्दगी
जब
कदम-ताल करती है,
तब हमारी समझ भी
पानी के बुलबुलों-सी
बिखर-बिखर जाती है।
मेरी प्रार्थनाएं
मैं नहीं जानती
प्रार्थनाएं कैसे करते हैं
क्यों करते हैं,
और किसके सामने करते हैं।
मैं तो यह भी नहीं जानती
कि प्रार्थनाएं करने से
क्या मिल पाता है
और क्या मांगना चाहिए।
सूरज को देखती हूं।
चांद को निरखती हूं।
बाहर निकलती हूं
तो प्रकृति से मिलती हूं।
पत्तों-फूलों को छूकर
कुछ एहसास
जोड़ती हूं।
गगन को आंखों में
बसाती हूं
धरा से नेह पाती हूं।
लौटकर बच्चों के माथे पर
स्नेह-भाव अंकित करती हूं,
वे मुझे गले से लगा लेते हैं
इस तरह मैं
ज़िन्दगी से जुड़ जाती हूं।
मेरी प्रार्थनाएं
पूरी हो जाती हैं।
वो हमारे बाप बन गये
छोटा-सा बच्चा कब बाप बन गया।
बहू आई तब बच्ची-सी।
प्यारी-दुलारी-न्यारी पोती आई
जीवन में बहार छाई।
बेटे ने घर-बार सम्हाला,
डाँट-डपटकर हमें समझाते।
चिन्ता में हर दम घुलते रहते।
हारी-बीमारी में
भागे-भागे चिन्ता करते।
ये खालो, वो खा लो
मीठा छीनकर ले जाते।
आराम करो, आराम करो
हरदम बस ये ही कहते रहते।
हर सुविधा देकर भी
चैन से न बैठ पाते।
हम हो गये बच्चों से
वो हमारे बाप बन गये।
अंधविश्वास अथवा विश्वास
अंधविश्वास पर बात करना एक बहुत ही विशद, गम्भीर एवं मनन का विषय है जिसे कुछ शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। कल तक जो विश्वास था, परम्पराएँ थीं, रीति-नीति थे, सिद्धान्त थे, काल परिवर्तन के साथ रूढ़ियाँ और अंधविश्वास बन जाते हैं। तो क्या हमारे पूर्वज रूढ़िवादी, अंधविश्वासी थे अथवा हम कुछ ज़्यादा ही आधुनिक हो रहे हैं और अपनी परम्पराओं की उपेक्षा करने लगे हैं?
मेरी ओर से दोनों ही का उत्तर नहीं में हैं।
अंधविश्वास और विश्वास में कितना अन्तर है? केवल एक महीन-सी रेखा का। विश्वास और अंधविश्वास दोनों को ही किसी तराजू में तोलकर अथवा किसी मापनी द्वारा सही-गलत नहीं सिद्ध किया जा सकता। यदि हम अंधविश्वास पर बात करते हैं तो विश्वास पर तो बात करनी ही होगी। वास्तव में मेरे विचार में विश्वास एवं अंधविश्वास एक मनोभाव हैं, स्वचिन्तन हैं, अनुभूत सत्य है और कुछ सुनी-सुनाई, जिनके कारण हमारे विचारों एवं चिन्तन का विकास होता है।
विश्वास और अंधविश्वास दोनों ही काल, आवश्यकता, विकास, प्रगति, एवं जीवनचर्या के अनुसार बदलते हैं। इनके साथ एक सामान्य ज्ञान, अनुभूत सत्य बहुत महत्व रखते हैं।
एक-दो उदाहरणों द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूँगी।
जैसे हमारी माँ रात्रि में झाड़ू लगाने के लिए मना करती थी, कारण कि अपशकुन होता है। कभी सफ़ाई करनी ही पड़े तो कपड़े से कचरा समेटा जाता था और बाहर नहीं फ़ेंका जाता था। हमारे लिए यह अंधविश्वास था। किन्तु इसके पीछे उस समय एक ठोस कारण था कि बिजली नहीं होती थी और अंधेरे में कोई काम की वस्तु जा सकती है इसलिए या तो झाड़ू ही न लगाया जाये और यदि सफ़ाई करनी ही पड़े तो एक कोने में कचरा समेट दें, सुबह फ़ेंके।
उस समय अनेक गम्भीर रोगों की चिकित्सा उपलब्ध नहीं थी, घरेलू उपचार ही होते थे। रोग संक्रामक होते थे। तब लोग इन रोगों से बचने के लिए हवन करवाते थे जो हमें आज अंधविश्वास लगते हैं। किन्तु वास्तव में हवन-सामग्री में ऐसी वस्तुएँ एवं समिधा में ऐसे गुण रहते थे जो कीटाणुनाशक होते थे और घर में कीटाणुओं का नाश होने से परिवार के अन्य सदस्यों को उस संक्रामक रोग से बचाने का प्रयास होता था। आज ऐसी शुद्ध सामग्री ही उपलब्ध नहीं है और चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हैं अतः यह आज हमारी दृष्टि में अंधविश्वास है।
शंख-ध्वनि से अदृश्य जीवाणुओं का भी नाश होता है, इसी कारण हवन में एवं शव के साथ शंख बजाया जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि शव के साथ अदृश्य जीवाणु उत्पन्न होने लगते हैं जिनका अन्यथा नाश सम्भव ही नहीं है। आज हमारी दृष्टि में यह अंधविश्वास हो सकता है किन्तु यह वैज्ञानिक सत्य भी है।
अंगूठियाँ, धागे, तावीज़, कान, नाक, पैरों में आभूषण: यह सब हमारे रक्त प्रवाह एवं नाड़ी तंत्र को प्रभावित करते हैं जिस कारण रोग-प्रतिरोधक क्षमता बनती है किन्तु वर्तमान में हमें यह अंधविश्वास ही लगते हैं क्योंकि हम इनके नियमों का पालन नहीं करते इस कारण ये अप्रभावी रहते हैं एवं शुद्ध रूप में उपलब्ध भी नहीं होते।
अतः कह सकते हैं कि अंधविश्वास भी एक विश्वास ही है बस जैसा हम मान लें, न कुछ गलत न ठीक। बस हमारे विश्वास अथवा अंधविश्वास से किसी की हानि न हो।
कोरोना ने नहीं छोड़ा कोई कोना
कोरोना ने नहीं छोड़ा कोई कोना, अब क्या-क्या रोना, और क्या कोरो-ना और क्या न कोरो-ना। किसी न किसी रूप में सबके घर में, मन में, वस्तुओं में पसर ही गया है।
खांसी, बुखार, गले में खराश। बस इनसे बचकर रहना होगा।
पहले कहते थे, खांसी आ रही है, जा बाहर हवा में जा।
अब कहते हैं बाहर मत जाना कोई खांसी की आवाज़ न सुन ले।
प्रत्येक वर्ष अप्रैल में घूमने जाने का कार्यक्रम बनाते हैं, बच्चों की छुट्टियां होती हैं चार-पांच दिन की। अभी सोच ही रहे थे कि बुकिंग करवा ले, कि कोरोना की आहट होने लगी। बच गये, पैसे भी और हम भी।
एकदम से एक भय व्याप्त हुआ, राशन है क्या, दूध का कैसे होगा, सब्ज़ियां मिलेंगी क्या, छोटी-सी पोती के दूध का कैसे करेंगे?
भाग्यवश बच्चे तो पहले ही वर्क फ्राम होम थे, पति सेवा-निवृत्त, अब हम भी हो गये घर में ही।
लगभग दो महीने विद्यालय बन्द हो गये। 23 मार्च से लेकर पूरा अप्रैल और मई घर में ही बन्द होकर निकल गया, एक महीना तो सील बन्द रहे। 5 दिन सब्जी, फल, दूध कुछ नहीं। किन्तु समय कैसे बीत गया, पता ही नहीं लगा।
जून में धीरे-धीरे विद्यालय के द्वार उन्मुक्त होने लगे। एक-एक करके गैरशैक्षणिक कर्मचारियों को बुलाया जाने लगा। अब मै। 65 वर्ष की, 66वें प्रवेश कर चुकी। इसलिए मुझे ज़रा देर से आवाज़ लगी। 2 जून को विद्यालय जाने लगी, सप्ताह में पांच दिन कार्यदिवस, मात्र चार घंटे के लिए। किन्तु मन नहीं मान रहा था। न तो दूरी का ध्यान रखा जा रहा था और न ही सैनिटाईज़ेशन का, एक लापरवाही दिख रही थी मुझे। जिसे कहो वही रूष्ट। अब संस्थाएं वेतन का एक हिस्सा तो दे रही थीं, तो काम भी लेना था।
सरकार ने कहा आप 66 के हो अतः घर बैठो, घर से काम करो। अब घर से तो काम नहीं हो सकते सारे। विद्यालय के कम्पयूटर पर, साफ्टवेयर और डाटा तो वहीं रहेगा, पुस्तकें तो घर नहीं आयेंगी। कहना अलग बात है किन्तु कार्यालयों में 6 फ़ीट की दूरी से काम चल ही नहीं सकता।
अब जुलाई में किये जाने काम वाले हावी होने लगे थे, परीक्षा परिणाम, नये विद्यार्थियों का प्रवेश, वार्षिक मिलान और पता नहीं क्या-क्या।
हमारे सैक्टर में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे, हम सब डरने लगे।
तो क्या पलायन करना होगा अथवा इसे सावधानी और एक सही निर्णय कहा जायेगा, पता नहीं।
किन्तु निर्णय लिया और भारी मन से 18 वर्ष की नौकरी सकारण या अकारण अनायास ही छोड़ दी।
सब कहते हैं मैं तो भवन से निकल आई, भवन मेरे भीतर से कभी नहीं निकलेगा।
संयुक्त परिवार या एकल परिवार
समाज में, जीवन में एवं परिवारों में कुछ परिवर्तन सहज होते हैं किन्तु हम उन्हें उतनी सहजता से स्वीकार नहीं करते। इसका सबसे बड़ा कारण यह कि हमारे मन-मस्तिष्क में प्राचीनता बहुत गहरे से पहरा डालकर बैठी है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि संयुक्त परिवार समाप्त होते जा रहे हैं। मेरी दृष्टि में यह पारिवारिक जीवन में परिवर्तन की एक सहज स्थिति है जिस पर हमारा वश नहीं है।
हाँ, इस पर हमारा वश अवश्य है कि यदि हम वयोवृद्ध हैं तो नई पीढ़ी पर सारा आरोप थोप देते हैं कि युवा पीढ़ी दिशा भटक गई है, बुज़ुर्गों को बोझ समझती है, उन्हें पसन्द नहीं करती, उसकी देखभाल नहीं करती, श्रवण कुमार नहीं है। संस्कृति, परम्पराओं, नैतिक मूल्यों का सम्मान नहीं करती, बड़ों का आदर नहीं करती।
मैंने आज तक युवा पीढ़ी में किसी को यह कहते नहीं सुना कि हमारे माता-पिता हमारे बच्चों यानी अपने नाती-पोतियों का ध्यान नहीं रखते, उनसे प्यार नहीं करते अथवा उनकी देखभाल में समय नहीं देते। सारी की सारी शिकायत गुज़री हुई पीढ़ी को ही है।
यदि हम, हमसे भी पिछली पीढ़ी की बात करें तब पूर्णतया संयुक्त परिवार ही होते थे। अर्थात् प्रायः पूरी तीन पीढ़ियाँ एक साथ रहती थीं। यदि चार भाई हैं तो वे भी एक ही छत और व्यवस्था के भीतर साथ ही रहते थे। और प्रायः सभी परिवारों में पाँच-सात बच्चे तो होते ही थे। उस समय अधिकांश परिवार व्यवसाय-आधारित अथवा कृषि पर ही आश्रित हुआ करते थे। और यदि किसी परिवार से कोई एक सदस्य नौकरी करने जाता भी था तो ‘‘दूर देस’’ जाता था, उसका अपना परिवार अर्थात् पत्नी और बच्चे वहीं रहते थे। वह एक व्यवस्था थी। अपने घर, खुले स्थान, घर की दाल-रोटी एवं कार्यों का अनकहा बंटवारा हुआ करता था फिर वह घर से बाहर पुरुषों का कार्यक्षेत्र हो अथवा घर के भीतर महिलाओं का।
फिर परिवर्तन का दौर शुरु हुआ। परिवार छोटे होने लगे। दो या तीन बच्चे। व्यवसाय एवं कृषि से परिवारों का पालन कठिन होने लगा और पुरुष नौकरी करने लगे। नारी शिक्षा आरम्भ हुई और महिलाओं के जीवन में एक गहरा परिवर्तन आया। शिक्षा का विस्तार होने लगा और माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए शहरों की ओर बढ़ने लगे। यह विकास का एक सहज-स्वाभाविक रूप था। अपने घर एवं स्थान से जुड़े माता-पिता अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहते, नवीनता एवं आधुनिकता को सहजता से स्वीकार नहीं करते और युवा अपनी नौकरी, कार्य-स्थल, प्रगति, शिक्षा के अवसरों के कारण शहरों में बसने लगी। इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। समाधान है तो केवल इतना कि इस परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार किया जाये और जितना सामंजस्य बिठाया जा सके, बिठाया जाये न कि दोषारोपण पद्धति पर चला जाये। प्रश्न संयुक्त परिवार के पक्ष-विपक्ष का है ही नहीं, बदली जीवन-शैली का है, शिक्षा के बदले स्वरूप का है, वैश्विक दौर का है, विकास की गति का है, जिसे हम कदापि दोष नहीं दे सकते।
अब हम आज भी कहें कि गाँवों की जीवन-शैली बहुत अच्छी थी, भारत की गुरुकुल शिक्षा जैसी कोई पद्धति नहीं थी, निःसंदेह नहीं थी किन्तु आज तो सम्भव नहीं है ये सब। तो जो आज सम्भव है उसमें सन्तोष करें और अकारण पीढ़ियों, संस्कारों, परम्पराओं को कोसना और राग अलापना बन्द करें।