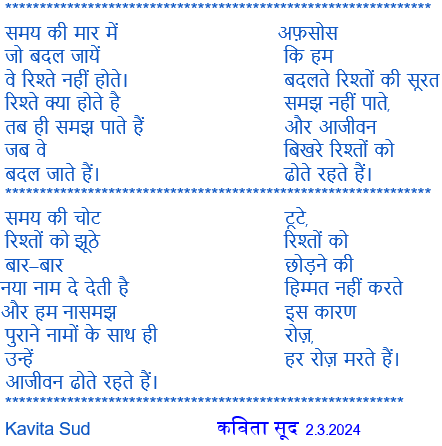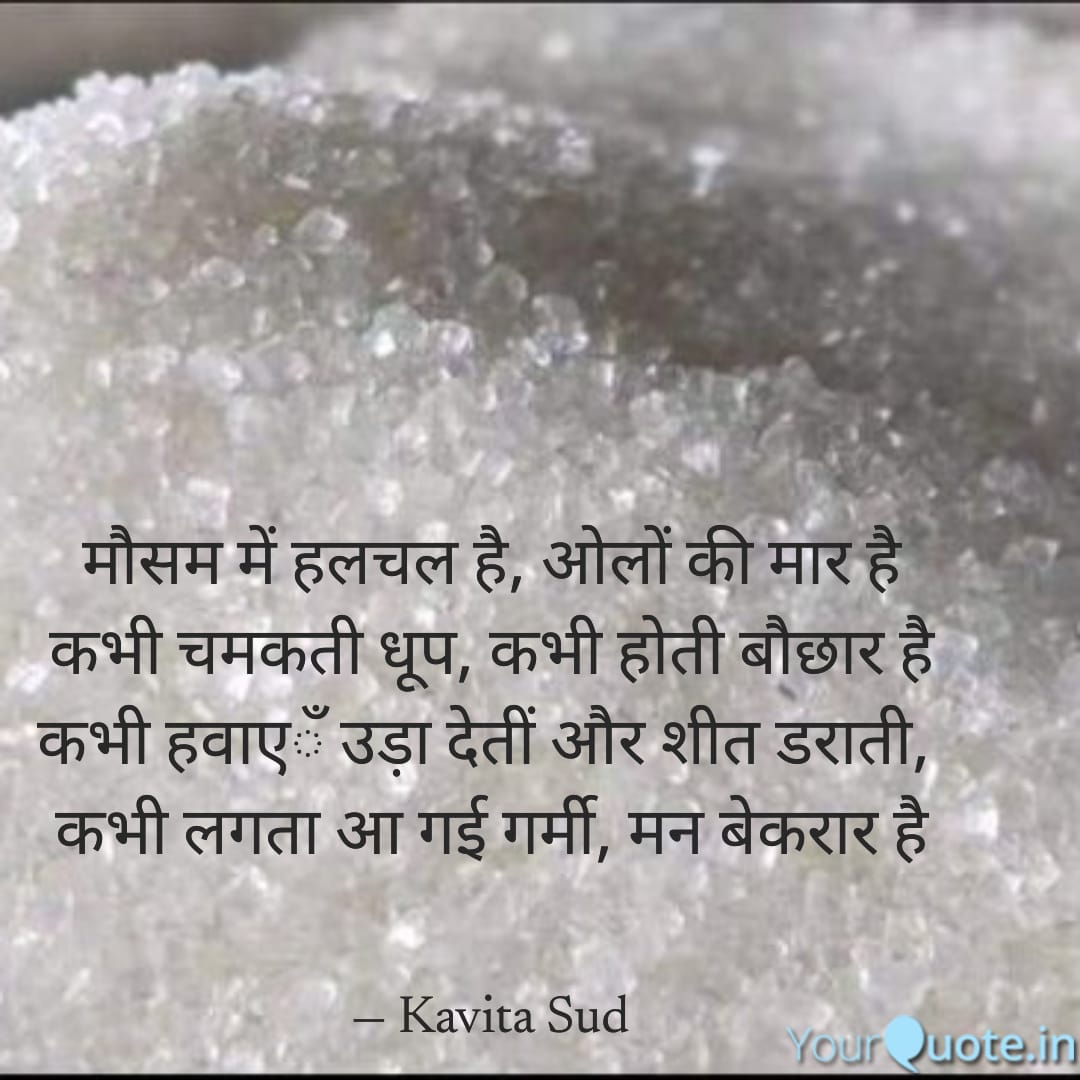मेरे प्रिय हिन्दी साहित्यकार : हज़ारी प्रसाद द्विवेदी
हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य से मैं बहुत गहरे तक जुड़ी हुई हूं। अपने अध्ययन काल में अनेक कवि, लेखक, उपन्यासकार, इतिहासकार रहे जिनकी पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया किन्तु हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन मुझे बहुत गहरे तक जोड़ता रहा है।
हज़ारी प्रसाद द्विवेदी (19 अगस्त 1907 - 19 मई 1979) हिन्दी निबन्धकार, आलोचक, उपन्यासकार थे। कलाओं के प्रति इनके दृष्टिकोण ने प्राचीन एवं मध्यकालीन हिन्दी साहित्य के अध्ययन के नवीन द्वार उन्मुक्त किये। साहित्य की प्रत्येक विधा में वे पारंगत थे। वे हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत और बाङ्ला भाषाओं के विद्वान थे।
द्विवेदीजी ने शांति निकेतन में बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष, उपरान्त पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष, पुनः काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष बने। उनकी
विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर नियुक्ति हुई। कुछ समय के लिए हिन्दी का ऐतिहासिक व्याकरण योजना के निदेशक भी बने। कालान्तर में उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के अध्यक्ष तथा 1972 से आजीवन उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ के उपाध्यक्ष पद पर रहे। 1973 में आलोक पर्व निबन्ध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।1957 में पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किये गये। 1997 में इनके चित्र का डाक टिकट भी जारी हुआ।
हिन्दी साहित्य पर इनका लेखन पठनीय एवं अप्रतिम है। मुझे इनकी संस्कृतनिष्ठ भाषा बहुत आकर्षित एवं प्रभावित करती रही है। हिन्दी साहित्य को इन्होंने एक नई पहचान दी। रामचन्द्र शुक्ल के बाद इनकी हिन्दी साहित्य एवं इतिहास पर लिखी गई पुस्तकों ने हिन्दी साहित्य के पाठकों को एक नवीन, चिन्तनपूर्ण दृष्टि प्रदान की। मध्यकालीन हिन्दी साहित्य एवं प्राचीन एवं अर्चाचीन साहित्य पर इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें एक नवीन चिन्तन प्रदान करती हैं। सांस्कृतिक एवं पौराणिक पृष्ठभूमि पर रचित उपन्यास गहन चिन्तन की ओर ले जाते हैं। विषय विविधता इनके लेखन की विशेषता रही है। अगस्त 1981 में आचार्य द्विवेदी की उपलब्ध सम्पूर्ण रचनाओं का संकलन 11 खंडों में हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली के नाम से प्रकाशित हुआ।
नई पीढ़ी और हिन्दी
नई पीढ़ी की हिन्दी आजकल स्टैंडअप कामेडियन बनकर रह गई है।
बात कटु किन्तु है सत्य कि नई पीढ़ी के पास हिन्दी नहीं है। वे केवल बोल-चाल में हीए उतनी ही हिन्दी जानते हैं जितनी आवश्यक है। और आज की पीढ़ी की हिन्दी, हिन्दी न होकर एक अद्भुत- मिश्रितए खिचड़ी भाषा है, अपशब्दों की भरमार रहती है।
इसके लिए हम नई पीढ़ी को दोष नहीं दे सकते। उनको जो मिल रहा है वही वे परोस रहे हैं और खा-खिला रहे हैं।
इसके अनेक कारण हैं।
आज सारे देश में समान भाषा पद्धति नहीं है, है तो केवल अंग्रेज़ी के लिए। हिन्दी देश के कुछ ही राज्यों में अनिवार्य है वह भी केवल दसवीं तक। अनेक राज्यों में यहां भी अन्य स्थानीय भाषाओं के लिए विकल्प दे दिया जाता है। प्रत्येक विषय का माध्यम अंग्रेज़ी ही रहता है। इसके अतिरिक्त CBSE, ICSE के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य के अपने शिक्षा बोर्ड हैं जो अपने राज्य के अनुसार भाषा का चयन करने के लिए स्वतन्त्र हैं।
सबसे बड़ी बात यह कि दसवीं के बाद हिन्दी का विकल्प ही नहीं है। यदि आप विभिन्न शिक्षा बोर्ड के विषयों को देखें तब वहां आपको हिन्दी का विकल्प दिखाई तो देगा किन्तु अधिकांश विद्यालय इसके लिए अध्यापक ही नियुक्त नहीं करते और हिन्दी का विकल्प ही नहीं देते।
इंजीनियरिंग, चिकित्सा, IT आदि सब अंग्रेज़ी आधारित ही हैं। यदि दसवीं तक अच्छी हिन्दी पढ़ाई भी जाये तो भी यहां तक आते-आते सब छूट जाती है।
कहने को हिन्दी समाचार-पत्र एवं टी वी समाचार पत्र हिन्दी में प्रसारित होते हैं किन्तु कैसी हिन्दी होती है यह तो हम जानते ही हैं। सरलता के नाम पर अभद्र भाषा का प्रयोग एवं निरर्थक अंग्रेज़ी शब्दों का ही प्रयोग होता है ।
एक अन्य कारण यह कि हम आज वैश्विक स्तर पर अंग्रेज़ी माध्यम से ही जुड़ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि अनेक देश आज भी अपनी भाषा से वैश्विक स्तर से जुड़े हुए हैं तो हम क्यों नहीं। इसका सीधा-सा कारण यह है कि जब हम 70 वर्षों में हिन्दी को उस स्तर पर स्थापित नहीं कर पाये तो अब यह असम्भव प्रायः ही प्रतीत होता है।
हमें स्वीकार करना ही होगा कि नई पीढ़ी हिन्दी के साथ नहीं है। केवल चलती हिन्दी बोल लेना अथवा लिख लेना हिन्दी नहीं है। व्याकरण कहीं खो गया है। शब्द अनर्थ होने लगे हैं, वर्णमाला ध्वस्त है। वाक्य संरचना का कोई अर्थ नहीं रह गया है।
ये आँखें
ये आँखें भी बहुत बड़ी चीज़ हैं। ये तो सब ही जानते हैं कि देखने के काम आती हैं किन्तु दिखाने के भी बहुत काम आती हैं, बस आपको दिखानी आनी चाहिए। आज सब सोचने लगी, आँखों के मुहावरों पर तो न जाने कितने मुहावरे सामने आ गये।
आँखों ही आँखों में हँसना, आँख मारना, आँखों में धूल झोंकना, आँखें बिछाना, आँख का कांटा, आँख का तारा, आँख लगना, आँख लड़ना, आँखें चुराना और न जाने कितने ही।
किन्तु कुछ मुहावरे तो बिल्कुल मेरे काम के निकले। जैसे
आँख धुंधलाना, आँख दिखाना, आँखों पर चरबी चढ़ना, आँख पर पर्दा पड़ना, आँखें बन्द होना, सीधी आँख न देखना और अन्त में आँख खुलना।
नववर्ष का उपहार लेकर आईं हमारी आँखें हमारे लिए। आँख धुंधलाने लगी। आँख देखने वाले को आँख दिखाई। किन्तु वे कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने हमें ही आँख दिखा दी। बोले, आँखों पर चरबी चढ़ गई है, आँखों पर पर्दा पड़ गया है।
और नववर्ष में उन्होंने हमारी एक आँख बन्द कर दी। अब न सीधी आँख देखना, न आँख मारना, न आँख लड़ना न लड़ाना। वाह! आँख के भीतर एक लैंस, एक चश्मा भी उपहार में मिला। मोबाईल, टी. वी., पी. सी. सब बन्द। और अन्त में जब ठीक से आँख खुली तब भी ठीक से अनुभव करने में दो-तीन दिन तो लग ही गये।
इसे कहते हैं cataract
अब एक आँख तो सुधर गई, दूसरी भी पीछे नहीं। तो चलिए उसके लिए भी ये सारे मुहावरे याद रखते हैं, अगले सप्ताह के लिए।
पहली मुलाकात
अजीब-सा लगा उसे वह युवक। बिखरे-से बाल, टी-शर्ट, मटमैले जूते, कंधे पर फीते वाला पुराना बैग, लेकिन है तो आकर्षक-सुन्दर, उसके मन ने कहा। उसकी टेढ़ी-सी निश्छल मुस्कान ने उसे जैसे बांध लिया। कौन है यह ? है तो अजनबी किन्तु कहीं अपना-सा लग रहा है। अहंहं, उसके मन ने उस पर ही उपहास कर डाला। अपनी उम्र देख, 30 की हो रही है और यह बच्चा-सा युवक उसे आकर्षक-सुन्दर लग रहा है।
यह उनकी पहली मुलाकात थी।
वह द्वार खोले खड़ी उसे देखती रही और वह युवक हँस दिया, घर के अन्दर भी आने देगी या नहीं?
अचानक उसके भीतर की अक्खड़ लड़की जाग उठी, ‘‘लेकिन आप हैं कौन उसने पूछा’’।
‘‘तू नीतू है न लड़ाकी-सी, संतोष की ननद’’।
अरे, ये तो मेरा घर का नाम जानता है, कौन है यह।
उसने रास्ता छोड़ दिया और वह युवक अधिकार से घर के भीतर चला आया।
तो यह उसकी भाभी का भाई। दिल में कहीं झंकार हुई।
दो दिन रुका। उससे बात की, कहा कि उसके ही लिए आया है यहाँ। सोचकर बताना, फिर आऊँगा।
और फिर वह उसकी ज़िन्दगी में सदा के लिए ही आ गया। किन्तु वह पहली मुलाकात आज तक नहीं भूलती।
शिमला की यादें
आज सौ कदम पैदल चलना पड़े तो वह कहते हैं न कि नानी याद आ गई। किन्तु स्मरण करती हूँ बचपन के वे दिन जब हम दिन-भर में 10-12 किलोमीटर तो प्रतिदिन चलते ही थे।
शिमला !
घर से लगभग पाँच किलोमीटर दूर स्कूल। सर्दी हो अथवा गर्मी, बरसात हो अथवा बर्फ़वारी, पूरा बस्ता उठाकर पैदल स्कूल। कोई आवागमन का साधन नहीं, बस पैदल जिसे हम ग्यारह नम्बर बस कहा करते थे। क्या मस्ती भरे दिन थे वे। जेबखर्च पाँच पैसे मिलते थे। और उन पाँच पैसे में पाँच-सात चीज़ें तो खरीद ही लेते थे। स्कूल से लौटते समय सड़क पर पकड़म-पकड़ाई, दौड़, रस्सी सब खेल लेते थे। उन दिनों कोई पीटीएम नहीं होती थी, न गृहकार्य की चिन्ता, न ट्यूशन, न माता-पिता को कोई तनाव कि बच्चे पढ़ रहे हैं अथवा नहीं। सब अपने-आप ही चलता रहता था। सबसे आनन्ददायक होता थी शीत ऋतु। इतने कपड़े पहनते थे कि गिनती ही नहीं हो पाती थी। दो-दो रजाईयाँ लेकर सोना। बर्फ़ में सानन्द घूमते। न बीमार होने की चिन्ता, न भीगने का डर। बर्फ़ खाना, गोले बनाना, बुत बनाना, खूब आनन्द लेते थे। अंगीठियों को घेरकर बैठे सारा दिन मूंगफ़ली खाना। पानी की कमी हो जाती थी, और यदि पानी आता भी था तो नलों में बर्तनों में जम जाता था स्लेट की तरह। कई-कई दिन नहाने की छुट्टी, वे दिन सबसे अच्छे लगते थे। हा हा।
बड़ी याद आती है शिमला तेरी और तेरे साथ बिताये दिनों की।
बचपन के खेल
विष-अमृत
बचपन में खेले गये अनेक खेल आज भी हमें याद आते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि यह सारे खेल प्रायः खुले स्थानों पर, सामूहिक एवं परस्पर सम्भाव बनाये रखने वाले होते थे।
ऐसा ही एक खेल हम खेलते थे ‘‘विष-अमृत’’। इस खेल को विभिन्न आयु-वर्ग के बच्चे साथ खेल लेते थे। यह खेल पकड़म-पकड़ाई का ही एक रूप है।
इस खेल में एक बच्चा विष देने वाला बनता है और शेष सब उससे बचते भागते हैं। जैसे ही विष देने वाला बच्चा किसी को छूकर विष बोल देता है पकड़े गये बच्चे को उसी स्थान पर बिना हिले बैठ जाना पड़ता है जब तक कि कोई दूसरा खिलाड़ी आकर उसे छूकर अमृत कह कर जीवित नहीं कर देता।
इस तरह जब तक सारे खिलाड़ियों को विष नहीं दे दिया जाता खेल चलता रहता है। और जिसे सबसे पहले विष मिला होता है वह अब पकड़ने वाला बन जाता है।
बचपन के खेल -2
ऊँच-नीच
संध्या समय हमारा बाहर खुले मैदान में ऐसे ही खेलों में बीतता था जिसमें एक साथ बहुत से बच्चे साथ मिलकर खेल लेते थे।
ऊँच-नीच में खेलने के लिए ऐसा स्थान चुना जाता था जहाँ ऊँचाई-निचाई हो, जैसे सीढ़ियाँ आदि। एक बच्चा पकड़़ने वाला, जिसे हम लोग चोर ही कहा करते थे, बन जाता है उससे सब एक स्वर में गाकर पूछते हैं ‘‘ ऊँच मांगी नीच’’। चोर यदि कहता है कि ‘‘ऊँच’’ तो सब बच्चे उससे बचने के लिए नीचे आ जाते हैं। चोर के दूर जाते ही और बच्चे ऊँचाई वाले स्थान पर जाकर बैठकर उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं ‘‘हम तुम्हारी ऊँच पर रोटियाँ बनायेंगे’’। जब तक चोर पहुँचता है वे भाग जाते हैं। ऐसे करते-करते जो बच्चा पकड़ा जाता है वह अगला चोर बनता था।
इन खेलों में कब समय बीत जाता था पता ही नहीं लगता था। जब तक सब बच्चों की माँएं कान से पकड़कर खींचकर नहीं ले जाती थीं, ऐसे खेल कभी समाप्त ही नहीं होते थे। यही सब हमारी एक्टीविटी हुआ करती थीं, निःशुल्क एवं स्वस्थ रखने वाली।
क्रोध एक सहज विकार
हम प्रायः देखते हैं कि एक से वातावरण में रहने वाले लोग, एक परिवार के सदस्य, एक ही कार्यालय में कार्य करने वाले लोगों के स्वभाव में ज़मीन-आसमान का अन्तर रहता है। एक ही वातावरण में पले-बढ़े बच्चे भी भिन्न स्वभाव के होते हैं। एक क्रोधी स्वभाव का हो सकता है और दूसरा प्रत्येक स्थिति में शांत, सहनशील। ऐसा क्यों होता है? ं
मैंने यह भी देखा है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, जैसे लोगों के बीच समय व्यतीत करते हैं, हम कितना भी बचने का प्रयास कर लें, हमारे स्वभाव में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता ही है। मुझे बहुत बार लगता है कि मानसिक शांति पाना और खोना हमारे हाथ में नहीं रह जाता।
क्रोध एक सहज विकार है। यदि हम अपने साथ होने वाले अन्याय का विरोध नहीं करते और उसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे मन को शांति कैसे मिलेगी।
मैं इस बात से कदापि सहमत नहीं हूं कि सकारात्मक सोच से मन को सदैव शांति मिल सकती है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे चारों ओर सकारात्मकता ही है। इतना कुछ है कि उसे शब्द देना कठिन है। कितना भी चाहें हम सदैव सकारात्मक नहीं हो सकते, यह सहज स्वाभाविक है। और यदि हम अपने मन के वास्तविक भाव को मार कर आरोपित शांत होने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा भाव कभी भी स्थाई शांति प्रदान नहीं कर सकता।
नकारात्मक तथ्य को इग्नोर करने अथवा उपेक्षा करने का अर्थ आज यह है कि हम बुराई को स्वीकृति दे रहे हैं। एक उक्ति है कि आज दुनिया में बुराई इसलिए नहीं बढ़ी है कि बुरे लोग अधिक हो गये हैं, इसलिए बढ़ी है क्योंकि सहने वाले लोग अधिक हो गये हैं। यदि हमारे आस-पास कुछ गलत हो रहा है तो उसकी उपेक्षा करके मन को शांति कैसे मिल सकती है? मन को शांति तो उसका विरोध अथवा निराकरण करके ही मिलेगी।
आज फ़ेसबुक पर ही एक पोस्ट पढ़ने को मिली थी, अमेरिका के किसी शोध का उल्लेख था कि जो महिलाएं अपने पतियों के साथ लड़ती हैं वे दीर्घायु होती हैं और जो तथाकथित सहनशील, शांत होती हैं उनको हृदयाघात अधिक होते हैं। क्योंकि जो लड़ लेती हैं वे अपने मन की भड़ास निकाल लेती हैं और उनके मन को शांति मिलती है किन्तु जो विरोध नहीं करती, मन में रख लेती है, दूसरे शब्दों में भीतर ही भीतर घुटती हैं वे मानसिक संताप में जीवन व्यतीत करती हैं।
मुझे तो यह पोस्ट बहुत ही अच्छी लगी, निश्चित है कि मुझे कभी भी हृदयाघात नहीं हो सकता।
आज तीन दिन बाद ज्वरमुक्त होने पर जब फ़ेसबुक खोली तो आपके इस आलेख ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। हमारे आस-पास ऐसे कुछ शब्द इस तरह बेहिचक प्रयोग किये जाते हैं और हम विरोध भी नहीं कर सकते। रोकने पर, टोकने पर यही सुनने को मिलता है कि तुझे ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तू ज़्यादा बनती है, तेरे रोकने से कोई बोलना तो बन्द नहीं कर देगा। avoid करना चाहिए। किन्तु मैं क्यों avoid करूं। क्योंकि अधिकांश गालियों में तो महिलाओं से सम्बन्धित शब्द होते हैं, न भी हों तब भी। एक रोचक अनुभव लिखने से नहीं रोक पा रही। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के लोग बहुत अच्छी हिन्दी बोलते हैंै । किन्तु मेरा अनुभव यह है कि जितनी गालियों का प्रयोग उत्तर प्रदेश के लोग अपनी भाषा में करते हैं, शायद कहीं पर नहीं होता। कुछ समय के लिए मैं बैंक में यू. पी. में थी। पूरी शाखा में मैं अकेली महिलाकर्मी थी। एक महिला की एफ. डी. का भुगतान तकनीकी कारणों से नहीं हो पा रहा था। मैं उसे समझाने का प्रयास कर ही थी, किन्तु वह बैंक के विरूद्ध गालियां जोड़कर बोलती जा रही थी। मैंने उसे रोका, गाली क्यों दे रही हो, कर तो रही हूं तुम्हारा काम। फिर चिल्लाकर वही गाली देते हुए बोली, मैंने किसे दी गाली, कब दी। प्रत्येक वाक्य में वही गाली दो-चार बार। मैं उसे रोकूं, वह बोले मैंने कब दी गाली, मैं शर्मिंदी से परेशान और सारे कर्मचारी हंस-हंसकर आनन्द ले रहे।
पुस्तक अध्ययन
समय के साथ पुस्तकों की उपलब्धता भी कम है। आज किसी भी पुस्तक-विक्रेता के पास आपको हिन्दी साहित्य की पठनीय पुस्तकें नहीं मिलेंगी। पहले अनेक पुस्तक-विक्रेताओं के पास हिन्दी साहित्य की पुस्तकें उपलब्ध होती थीं और हम बाज़ार में घूमते -फिरते ऐसी दुकानों पर जाकर पुस्तकों का अवलोकन कर लेते थे और खरीद भी लेते थे, अब आप किसी भी पुस्तक-विक्रेता के पास चले जाईये कोई हिन्दी पुस्तक नहीं मिलेगी
मेरी समझ में एक समय भी होता है जब हमारी रूचियां इस तरह की होती हैं। कभी ऐसा ही समय था जब घर में कोई पुस्तक आती थी तो उसे पूरा पढ़कर ही रहते थे, यद्यपि, शायद आज से अधिक ही व्यस्त जीवन था। हिन्दी में प्राचीन-अर्वाचीन साहित्य, संस्कृति से सम्बन्धित श्रेष्ठ पुस्तकें उपलब्ध हैं, शोध कार्य के समय इतनी पुस्तकें पढ़ीं कि कोई गिनती ही नही। किन्तु अब ध्यान ही नहीं जाता कि पुस्तक खरीदी जाये या पढ़ी जाये, हां कभी जब मन होता है तब पुरानी पुस्तकों को ही देख-परख कर आनन्द ले लिया जाता है। यानी धूल झाड़कर मन आनन्दित हो जाता है, कि वाह ! मेरे पास यह पुस्तक भी है, यह भी है और यह भी है।
पुस्तकें , पत्रिकाएं, समाचार-पत्र पढ़ने का समय था वह अब टी.वी. धारावाहिक और पी. सी. में समा गया है।
राजकमल प्रकाशन की भी एक योजना थी, शायद 1975-80 तक मैं उसकी सदस्य रही, पेपर बैक में आधे मूल्य में श्रेष्ठ साहित्यिक पुस्तकें उपलब्ध होती थीं। मात्र बीस रूपये में दो पुस्तकें और वर्ष में एक निःशुल्क पुस्तक भेंट स्वरूप प्राप्त होती थी। उस समय आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास, हिन्दी साहित्य, और न जाने कितने उपन्यास, कहानी-संग्रह और अनेक शब्द कोष मेरे संग्रह का हिस्सा बने। प्रकाशक से निरन्तर नवीन प्रकाशित पुस्तकों की जानकारी भी मिलती रहती थी। फिर कार्यक्षेत्र बदला, पढ़ना-लिखना कम हुआ, जानकारी घटी, सब छूटता चला गया। तीन-चार वर्ष पूर्व मैंने राजकमल प्रकाशन से पुनः सम्पर्क किया कि क्या उनकी अब कोई ऐसी योजना है एवं पुस्तकों की सूची मंगवाई। योजना तो नहीं थी किन्तु पुस्तकों का मूल्य देखकर मैं चकरा गई। वही पुस्तक जो मैंने उस समय हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास जो उस समय मैंने मात्र 10-15-20 रूपये में मंगवाये थे उनका मूल्य 1500 -1800 रूपये तक था। किन्तु यह सोचकर मन आनन्दित हुआ कि मेरे पास उपलब्ध पुस्तकें इतनी मूल्यवान हो चुकी हैं।
दीपावली पर्व
दीपावली एक ऐसा पर्व जिसकी बात करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मन में उल्लास। न जाने कितने पर्व मनाए जाते हैं हमारे देश में, किन्तु सर्वाधिक आकर्षण एवं सौन्दर्य का यह पर्व जीवन में रंग भर देता है।
वर्तमान में दीपावली के साथ आने वाले अन्य पर्वों को मिलाकर पंचदिवसीय पर्व के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। पहले धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और अन्त में भाई-दूज। पर्वों की यह श्रृंखला केवल परिवार में ही नहीं, समाज में भी सम्बन्धों एवं नेह की श्रृंखला बन जाती है। पर्व से पूर्व भी और उपरान्त भी, लम्बे समय तक इन पर्वों की स्मृतियां, सम्बन्धों की मधुरता और नयेपन का भाव जीवन को मुखरित रखते हैं।
दीपावली क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, पूजन विधि कैसी होती है, सब जानते हैं। हम इतना कह सकते हैं कि आधुनिकता ने जहां हमारा परिवेश, वेशभूषा, खान-पान एवं सामाजिकता को प्रभावित किया है वहां ये महत्वपूर्ण पर्व भी इस परिवर्तन से अछूते नहीं रह पाये। हां, यह कह सकते हैं कि धर्म, पूजा, विश्वास, परम्पराएं सभी आज भी जीवन्त हैं, केवल व्यवहार में परिवर्तन आया है।
पहले समय में जहां सयुंक्त परिवारों में दीपावली की तैयारी महीनों पहले ही आरम्भ हो जाती थी, अब बाज़ार पर आश्रित हो गई है।
कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला यह पर्व भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। वास्तव में दीपावली (संस्कृत दीपावलिः दीप $ आवलि = पंक्ति अर्थात् पंक्ति में रखे हुए दीपक उत्तरी गोलार्ध में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पौराणिक सनातन उत्सव है। आध्यात्मिक रूप से यह अन्धकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है।
भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी पर्वों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात (हे भगवान! मुझे अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। यह उपनिषदों की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बन्दी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है।
भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदैव जीत होती है और असत्य का नाश होता है। दीपावली यही चरितार्थ करती है- असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है।
हमारे अधिकांश पर्व बदलते मौसम के सूचक हैं। दीपावली भी ऐसी ही पर्व है। ग्रीष्म एवं वर्षा के समापन के साथ शीत ऋतु की आहट यह पर्व अपने साथ लेकर आता है।
इस रूप में घरों में स्वच्छता के साथ ऋतु-परिवर्तन की तैयारी भी हो जाती है। पुराने का निष्पादन एवं नवीनता का आग्रह इस पर्व की बहुत बड़ी विशेषता है। परिवार पूरे वर्ष प्रतीक्षा करते हैं कि इस वर्ष नया क्या लाना है और दीपावली पर ही लाना है। कपड़े, घर का सामान एवं साज-सज्जा विशेष आकर्षण का केन्द्र रहते हैं। अपनों को उपहार एवं मिष्ठान्न देकर हम सम्बन्धों को नया रूप देने का प्रयास करते हैं।
इस पर्व की एक अन्य विशेषता यह कि यह पर्व हमारी तीन-तीन पीढ़ियों की भावनाओं को संजोकर चलता है। भारतीयता का यह रंग जो इस पर्व में देखने को मिलता है वह है संयुक्त परिवार का आनन्द और मिलन। आज के समय में बच्चे अक्सर घरों से दूर पराये शहरों में काम एवं व्यवसाय के लिए बस जाते हैं किन्तु दीपावली के अवसर पर सब अपने घरों को लौट आते हैं। वास्तविक उत्सव यही होता है जहां तीन पीढ़ियां एक साथ इस उत्सव को मनाती हैं और पर्वों में तीन ही रंग देखने को मिलते हैं। माता-पिता प्राचीन परम्पराओं के पालन की ओर ध्यान देते हैं, घी के दीपक, लक्ष्मी-गणेश-पूजन, रंगोली से घर को सजाना, पूजा की विविध सामग्री से मन्दिर की शोभा, विविध मिष्ठान्न, शगुन का लेन-देन, परिचितों को उपहार, बच्चों को नये कपड़े एवं उनकी पसन्द के खिलौने और अन्य उपहार, अपनी प्राचीन परम्पराओें के महत्व से बच्चों को परिचित करवाना, परिवारों में कई दिन तक आनन्द का वातावरण बना रहता है। बेटे-बहुएं उनकी इच्छानुसार पूजा-विधि करते हुए, आधुनिकता के साथ उन्हें जोड़ते हैं और बच्चे प्राचीनता के प्रति उत्सुक नवीनता के आग्रही, आकर्षक लड़ियों, नये तरह के पटाखों, मिठाई के साथ-साथ चाॅकलेट, तरह-तरह के घर के बने और बाहर के भोजन का आनन्द लेते हैं।
यही वास्तविक भारतीयता और भारतीय पर्वों की पहचान है।
वर्तमान में धनतेरस एवं दीपावली के शुभ अवसर पर वाहन एवं स्वर्ण की खरीददारी सबसे अधिक की जाती है। बाज़ारीकरण, व्यवसायीकरण एवं विज्ञापनों की दुनिया ने हमारे पर्वों को एक नये रंग में बदल दिया है। दिनों दिन की तैयारी अब पलभर में हो जाती है। मिट्टी के दीपक का स्थान डिज़ाईनर मोमबत्तियों एवं विद्युत लड़ियों ने ले लिया है।
यह हमारे लिए गर्व की बात है कि विदेशों में भी दीपावली पर्व अत्यन्त हर्षोल्लास एवं धार्मिक रीति से मनाया जाता है एवं अनेक देशों में भारत की ही भांति सरकारी अवकाश भी होता है।
दीपावली के दिन नेपाल, भारत,, श्रीलंका, म्यांमार, मारीशस, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी, पाकिस्तान और औस्ट्रेलिया की बाहरी सीमा पर क्रिसमस द्वीप पर एक सरकारी अवकाश होता है।
क्या ऑनलाइन रिश्ते ऑफलाइन रिश्तों पर हावी हो रहे हैं
मेरी दृष्टि में ऑनलाइन रिश्ते ऑफलाइन रिश्तों पर हावी नहीं हो रहे हैं, दोनों का आज हमारे जीवन में अपना-अपना महत्व है। हर रिश्ते को साधकर रखना हमें आना चाहिए, फिर वह ऑनलाइन हो अथवा ऑफलाइन ।
वास्तव में ऑनलाइन रिश्तों ने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी है जो कहीं भी ऑफलाइन रिश्तों पर हावी नहीं है।
अब वास्तविकता देखें तो ऑफलाइन रिश्ते रिश्तों में बंधे होते हैं, कुछ समस्याएं, कुछ विवशताएं, कुछ औपचारिकताएं। यहां हर रिश्ते की सीमाएं हैं, बन्धन हैं, लेनदारी, देनदारी है, आयु-वर्ग के अनुसार मान-सम्मान है, जो बहुत बार इच्छा न होते हुए भी, मन न होते हुए भी निभानी पड़ती हैं। यहां हर रिश्ते की अपनी मर्यादा है, जिसे हमें निभाना ही पड़ता है। ऐसा बहुत कम होता है कि ये रिश्ते बंधे रिश्तों से हटकर मैत्री-भाव बनते हों।
किन्तु ऑनलाइन रिश्तों में कोई किसी भी प्रकार का बन्धन नहीं है। एक नयापन प्रतीत होता है, एक सुलझापन, जहां मित्रता में आयु, वर्ग का बन्धन नहीं होता। बहुत बार हम समस्याओं से घिरे जो बात अपनों से नहीं कर पाते, इस रिश्ते में बात करके सुलझा लेते हैं। एक डर नहीं होता कि मेरी कही बात सार्वजनिक न हो जाये।
हां, इतना अवश्य है कि रिश्ते चाहे ऑनलाइन हों अथवा ऑफलाइन, सीमाएं दोनों में हैं, अतिक्रमण दोनों में ही नहीं होना चाहिए।
क्या शिक्षा उपभोक्तावाद का शिकार हो गई है
क्या शिक्षा उपभोक्तावाद की शिकार हो गई है, इस विषय पर बात करने से पूर्व हमें उपभोक्तावाद शब्द को समझना होगा। वास्तव में उपभोक्तावाद का अर्थ वस्तुओं के उपयोग करने वाला जिसे हम consumerism कह सकते हैं। अर्थात शिक्षा के लिए यदि हम उपभोक्तावाद शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम स्पष्टतः शिक्षा को एक वस्तु के रूप में प्रयोग करने की बात कर रहे हैं।
दूसरे अर्थ में इस शब्द का अभिप्राय व्यवसाय, पूंजीवाद, व्यावसायीकरण, उद्योगवाद भी लिया जा सकता है।
इस अर्थ में यह बात तार्किक प्रतीत होती है कि शिक्षा उपभोक्तावाद से की शिकार है।
भारत में शिक्षा की एकरूपता नहीं है, कोई नियन्त्रण नहीं है, कोई समानता नहीं है। जिसका मन करता है अपनी इच्छा से विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खोल लेते हैं, बड़ी-बड़ी शैक्षणिक संस्थाएं खोल लेते हैं, बस धन और बल चाहिए। पाठ्यक्रम में कहीं एकरूपता नहीं है, जो प्रकाशक कमीशन देता है उसकी पुस्तकें पाठ्यक्रम में लगा दी जाती हैं। एन.सी.आर.टी. की पुस्तकें केवल सरकारी विद्यालयों तक सीमित रह गई हैं जहां शिक्षकों को तो असीमित सुविधाएं, वेतन, अवकाश हैं किन्तु विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं। वहीं दूसरी ओर निजी शिक्षण संस्थाएं एक पंचसितारा व सात सितारा होटलों के समान हैं। दूसरी ओर प्राईवेट ट्यूशन।
इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम अर्थहीन होता जा रहा है, व्यवसायिक पाठ्यक्रम न के बराबर हैं और शिक्षा के वर्ष बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान शिक्षा कहीं भी रोज़गारोन्मुख नहीं है।
अर्थात जिसके पास धन है वह यहां खड़ा है शेष या तो बेरोज़गार होकर भटक रहे हैं, राहों से भटक रहे हैं ।
तो कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यवसाय, पूंजीवाद, व्यावसायीकरण, उद्योगवाद के रूप में उपभोक्तावाद की शिकार हो गई है।
उत्सव-खुशी और आतिशबाजी की तार्किकता
दीपावली के अवसर पर सदैव ही आतिशबाजी होती रही है। किन्तु आज आतिशबाजी से पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण इसे प्रतिबन्धित करने की बात की जाती है।
आतिशबाजी चलाने वाले इसे अपने घर नहीं बनाते । वे किसी छोटे दुकानदार से खरीद कर लाते हैं। छोटा दुकानदार किसी थोक व्यापारी से लाता है और थोक-व्यापारी आतिशबाजी बनाने वाली फ़ैक्ट्री से, और इस कार्य के लिए ये सरकार से लाईसेंस लेते हैं अथवा कुछ अवैध भी बनाते हैं। अर्थात शुरुआत आशिबाजी चलाने वालों की ओर से नहीं, सरकार की ओर से होती है।
फिर आजकल हरी आतिशबाजी का प्रदर्शन भी हो रहा है, क्रेता कहां जान पाता है कि आतिशबाजी हरी है, काली या नीली। जो मिलती है ले लेते हैं। हां, इतना अवश्य है कि हरी आशिबाजी के नाम पर खूब लूट हो रही है। ध्वनि प्रदूषण तो उससे भी होता ही होगा।
कहने का अभिप्राय यह कि हम मूल की ओर तो जाते ही नहीं, केवल आंखों देखी पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, बुराई करते हैं। यदि आतिशबाजी इतनी ही हानिकारक है तो इनकी फ़ैक्ट्रियों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहिए। कह सकते हैं कि इससे रोज़गार पर प्रभाव पड़ेगा, तो यह भी सरकार का ही कार्य है कि ऐसी फ़ैक्ट्रियों को किसी नवीन निर्माण सामग्री के लिए सहयोग प्रदान करे।
कोर्ट का आदेश जनता के लिए है सरकार के लिए क्यों नहीं। और उससे भी अधिक विचारणीय बात यह कि नेताओं की विजय पर भी खूब आतिशबाजी होती है, नववर्ष एवं कुछ अन्य धर्मों के गुरुओं के दिवस पर भी आतिशबाजी होती है, तब क्या प्रदूषण नहीं होता। मेरा यह अभिप्राय कदापि नहीं कि इस कारण हिन्दू पर्वों पर आतिशबाजी की छूट दी जाये, किन्तु नियन्त्रण हर रूप में किया जाना चाहिए।
अतः इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे आतिशबाज़ी का निर्माण ही बन्द हो, और समय की आवश्यकतानुसार इन्हें किसी नये काम के लिए सरकार की ओर से सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं।
यह बात बिल्कुल वैसी ही है कि प्लास्टिक के लिफ़ाफ़े प्रयोग करने पर सब्ज़ी बेचने वाले का 500 रुपये का चालान काटा जाता है किन्तु बनाने वाले बना रहे हैं, उन पर कोई रोक नहीं।
छायावाद
छायावादी साहित्य को हिन्दी का स्वर्ण युग कहा जाता है। @ब्रज भाषा से निकलकर हिन्दी खड़ी बोली, द्विवेदी काल की इतिवृत्तात्मकता स्थूलता और नैतिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप से बाहर आकर छायावादी काल ने हिन्दी साहित्य को एक नवीन चिन्तन, भाषा एवं स्वच्छन्दता प्रदान की।
साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं जो इस काल में विकसित न हुई हो। भाषा की प्रांजलता, नवीन भावों की अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक चेतना की लहर, कालानुसार विषय, काव्य-रूढ़ियों से मुक्ति, प्रेम, प्रकृति प्रेम, राष्ट्रवाद, एक नवीन सौन्दर्यबोध को रूपायित करती, रहस्यवाद, प्रगतिवाद एवं नई कविता की ओर बढ़ते कदम, छायावादी कविता ने साहित्य लेखन की दिशा ही बदल दी। इस काल में काव्य विधा ही प्रधान रही, यद्यपि नाटक, संस्मरण, निबन्ध, उपन्यास एवं अन्य गद्य विधाओं में भी उत्कृष्ट साहित्य का सृजन हुआ।
1918 से 1936 तक का काल छायावादी काल माना जाता है। वर्ष 1921 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित लेख ‘हिन्दी में छायावाद’से ही इस काल के साहित्य को छायावाद नाम मिला, यह माना जाता है। मुकुटधर पाण्डेय को ही इस नामकरण का श्रेय दिया गया है। छायावाद के चार प्रमुख स्तम्भ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद (30 जनवरी 1889-15 नवंबर 1937) सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (21 फ़रवरीए 1896- 15 अक्टूबर 1961) सुमित्रानंदन पंत (20 मई 1900 28 दिसंबर 1977) महादेवी वर्मा (26 मार्चए 1907-11 सितम्बर 1987)
हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में इन चारों में वैयक्तिक आवेगों की आयासहीन अभिव्यक्ति है, चारों की कविताओं में कल्पना अविरल प्रवाह से घन-संश्लिष्ट आवेगों की उमड़ती हुई भावधारा का प्राबल्य है।, जयशंकर प्रसाद की संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली, प्रवाह, अद्भुत सौन्दर्यात्मक प्रकृति चित्रण, सुमित्रानन्दन पन्त की कोमलकान्त पदावली, प्रेम व सौन्दर्य की अभिव्यक्ति, महादेवी वर्मा की कोमल भावों से परिपूर्ण मन को छूती रचनाएं और सूर्यकान्त त्रिपाठी की नवीन भाषा-शैली, बेबाक लेखन, भावों का खुलापन, नई कविता की ओर बढ़ते कदम एवं छन्दमुक्त रचनाएं पूर्ण छायावाद युग को सार्थक करते हैं।
छायावादी काव्य को प्रसाद ने प्रकृति-तत्व दिया, निराला ने मुक्त छन्द दिया, पन्त ने सरसता एवं कोमलता दी तो महादेवी ने उसे सप्राणता एवं भावात्मकता देकर सम्पन्न किया।
छायावाद को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न आलोचकों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं एवं व्याख्यायित किया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ दो रूपों में बताया है : प्रथम रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के अर्थ में । महादेवी वर्मा ने छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद माना है।
बाबू गुलाबराय, डा. रामकुमार वर्मा, शान्तिप्रिय द्विवेदी छायावाद और रहस्यवाद में कोई विशेष भेद नहीं मानते। उनके अनुसार छायावाद और रहस्यवाद दोनों ही मानव और प्रकृति का एक आध्यात्मिक आधार बनाकर एकात्मवाद की पुष्टि करते हैं। उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग्विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद है। आचार्य नन्दुलारे वाजपेयी के शब्दों में मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किन्तु व्यक्त सौन्दर्य में आध्यात्मिक छाया का भान छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। गंगाप्रसाद पाण्डेय के शब्दों में छायावाद नाम से ही उसकी छायात्मकता स्पष्ट है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को अपने ढंग से स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश-विदेश की सुन्दरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिन्दी में उसे छायावद के नाम से अभिहित किया गया। डा. देवराज छायावाद को आधुनिक पौराणिक धार्मिक चेतना के विरुद्ध आधुनिक लौकिक चेतना का विद्रोह स्वीकार करते हैं। डा. नगेन्द्र के शब्दों में छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव-पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है।
छायावाद अपने युग की राजनीतिक, स्वतन्त्रता आन्दोलन, धार्मिक और दार्शनिक परिस्थितियों से भी प्रभावित हुआ। छायावाद पर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, गांधी, टैगोर एवं अरविन्द जैसे महापुरुषों की भी छाप है। दर्शन के क्षेत्र में भी इन कवियों की रचनाओं में अद्वैतवाद एवं सर्वात्मवाद के भाव दृष्टिगत होते हैं। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था, जिनमें मानवीय आचारों, क्रियाओं, चेष्टाओं और विश्वासों के बदले हुए और बदलते हुए मूल्यों को अंगीकार करने की प्रवृत्ति थी, जिनमें छंद, अलंकार, रस, ताल, लय आदि सभी विषयों में गतानुगतिकता से बचने का प्रयत्न था, शास्त्रीय रूढ़ियों के प्रति कोई आस्था नहीं दिखाई गई थी।
निर्विवाद रूप से सभी समीक्षक जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। 1913-14 के आस-पास प्रसाद की कविताएं इन्दु पत्रिका में प्रतिमास प्रकाशित हो रही थीं जो बाद में कानन-कुसुम पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुईं। यद्यपि कुछ समीक्षक सुमित्रानन्दन पन्त को भी छायावाद का प्रवर्तक कवि मानते हैं किन्तु इस विषय में स्पष्ट कहा जा सकता है कि प्रसाद काव्य क्षेत्र में पन्त से पहले आये और उनकी रचनाओं में आरम्भ से ही छायावाद की मूलभूल प्रवृत्तियां-आत्मनिष्ठता, अन्तर्मुखी दृष्टि, प्रकृति के प्रति नवीन दृष्टिकोण, अभिव्यक्ति की नूतन शैली आदि मिलती है, इस कारण प्रसाद को ही निर्विवाद रूप से छायावाद के प्रवर्तक कवि के रूप में स्वीकार किया गया है।
हिन्दी के प्रमुख छायावादी कवि
-------.---------
जयशंकर प्रसाद
============
प्रसाद की रचनाओं में छायावाद का उत्तम स्वरूप मिलता है। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न साहित्यकार थे। वे कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबन्ध लेखन सभी विधाओं में पारंगत थे, किन्तु उनका कवि-रूप उनकी समस्त कृतियों में विद्यमान है। नौ वर्ष की आयु में उन्होंने कलाधर उपनाम से अत्यन्त मनोहर और सरस छन्द की रचना की। सत्रह वर्ष की आयु में इनकी रचनाएं इन्दु पत्रिका में प्रकाशित होने लगीं। उपरान्त ये कविताएं चित्राधार और कानन-कुसुम संग्रहों में प्रकाशित हुईं।
प्रेम तत्व की व्यंजना प्रसाद काव्य की प्रथम और प्रमुख प्रवृत्ति है। उनके द्वारा अभिव्यक्त प्रेम लौकिक होकर भी आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख है। नारी सौन्दर्य को सुन्दर रूप में प्रस्तुत करने में प्रसाद की लेखनी सर्वोत्तम है। उनका सौन्दर्य चित्रण स्थूल न होकर सूक्ष्म है। कामायनी में चित्रित श्रद्धा का सौन्दर्य हमें आकृष्ट करता है।
इसके अतिरिक्त काव्य और दर्शन का विलक्षण समन्वय प्रसाद की रचनाओं में मिलता है। दर्शन में भी प्रसाद वेदान्त दर्शन से ज़्यादा प्रभावित हैं। किन्तु कामायनी में उन्होंने जिस आनन्दवाद का प्रतिपादन किया है वह शैव दर्शन से प्रभावित है। कामायनी महाकाव्य कला की दृष्टि से छायावाद का सर्वोत्तम प्रतीक है एवं आंसू प्रसाद की अन्यतम कृतियां हैं।
भारतीय इतिहास, संस्कृति, के प्रति प्रेम, वैभवमय अतीत के प्रति आग्रह, मानवतावाद एवं प्रकृति का एक नये स्वरूप में चित्रण प्रसाद की रचनाओं की एक अन्य विशेषता है। प्रकृति का मानवीकरण, नवीन बिम्ब एवं प्रतीकों के माध्यम से प्रसाद की रचनाओं में प्रकृति सौन्दर्य मुखरित होकर बोलता है। उनकी भाषा में लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता, चित्रमयता एवं उच्च कोटि की प्रतीकात्मकता है। उन्होंने हिन्दी साहित्य को नूतन भावराशि, नूतन अभिव्यंजना, नूतन भाषा शैली एवं कला-कौशल से समृद्ध किया है।
प्रसाद के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं जिनमें राष्ट्रप्रेम की भावना बहुत गहरे से है। नाटकों की कविताएं भी उनके देश-प्रेम, प्रकृति की अन्यतम अभिव्यक्ति, सौन्दर्य भाव को व्याख्यायित करती हैं
सुमित्रानन्दन पन्त
=========
पन्त का प्रथम काव्य-संग्रह पल्लव नवीन काव्य गुणों को लेकर हिन्दी साहित्य जगत में आया। पन्त की रचनाओं में सौन्दर्य के प्रति अत्यन्त कोमल मनोभाव हैं। पल्लव की भूमिका में ही कवि की सम्पूर्ण छायावादी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में इस भूमिका में समस्त छायावादी कविता के लिए क्षेत्र प्रस्तुत किया। इस भूमिका से पन्त की उस महत्वपूर्ण बौद्धिक क्षमता का पता लगता है जिसके द्वारा उन्होंने शब्दों की प्रकृति, उनकी अर्थबोधन क्षमता, उनके अर्थों के भेदक पहलुओं की विशिष्टता, छन्दों की प्रकृति, तुक और ताल का महत्व समझा था और समझने के बाद काव्य में प्रयोग किया था।
पन्त का छन्द-प्रवाह अत्यन्त शक्तिशाली है। प्रकृति और मानव-सौन्दर्य के सम्मिलन से उनकी रचनाओं में अद्भुत सौन्दर्य की सृष्टि होती है । कवि बंधी रूढ़ियों के प्रति कठोर नहीं है। मनुष्य के कोमल स्वभाव, अकृत्रिम प्रीति स्निग्ध हृदय और प्रकृति के विराट् और विपुल रूपों में अन्तर्निहित शोभा का ऐसा मनोहारी हृदयकारी चित्रण छायावादी काव्य में अन्यत्र नहीं देखा गया।
पन्त मूलतः गीतिकाव्य के एवं रोमांटिक कवि हैं। ज्योत्सना आदि नाटकों के सभी पात्र गीतिकाव्यात्मक एवं रोमांटिक हैं। उन्होंने कभी कथाकाव्य लिखने का प्रयास नहीं किया। उनके काव्य के तीन उत्थान हैं। प्रथम में वे छायावादी कवि हैं, द्वितीय में वे समाजवादी आदर्शों से चालित हैं और तीसरे में आध्यात्मिक। पन्त अरविन्द के आध्यात्मिक तत्वदर्शन से भी प्रभावित हैं। किन्तु पन्त वस्तुतः सौन्दर्य की महिमा के अनासक्त साक्षी कवि हैं। छायावाद को स्थापित करने में पन्त की रचनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।
सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला
=============
निराला छायावादी कवियों में प्रमुख होते हुए भी एक नवीन विचारधारा लेकर चले। वे आरम्भ से ही विद्रोही कवि के रूप में दिखाई दिये। गतानुगतिका के प्रति तीव्र विद्रोह इनकी कविताओं में आदि से अन्त तक बना रहा। निराला की प्रतिभा बहुमुखी है। निबन्ध, आलोचना, उपन्यास भी निराला की लेखनी से लिखे गये हैं। व्यंग्य और कटाक्ष उनकी प्रायः सभी रचनाओं में देखा जा सकता है। निराला का छन्दों के प्रति विद्रोह छन्दों का विरोध नहीं था, वे भावों की , व्यक्तिगत अनुभूति के भावों को स्वछन्द अभिव्यक्ति को महत्व देना चाहते थे। उनके मुक्त छन्द में एक प्रकार का झंकार और ताल विद्यमान है। इनकी रचनाओं में कथाकाव्य के प्रति झुकाव देखा जा सकता है।
उनकी आरम्भिक रचनाओं में ही उनकी स्वच्छन्दतावादी प्रकृति पूरे वेग से मिलती है। वस्तुतः निराला से बढ़कर हिन्दी में स्वच्छन्दतावादी कवि नहीं है। उनकी तुम और मैं, जूही की कली जैसी कविताओं में कल्पनाओं का आवेग है जिस कारण यह रचनाएं अत्यन्त लोकप्रिय हुईं। तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा एवं सरोज-स्मृति जैसी कथात्मक रचनाएं निराला की सर्वोत्तम कृतियां हैं।
महादेवी वर्मा
===========
महादेवी वर्मा एक संवेदनशील कवियत्री हैं।उनकी रचनाएं गीतिकाव्यात्मक हैं लाक्षणिक वक्रता एवं मनोवृत्तियों की मूर्त योजना उनकी रचनाओं में विद्यमान है। महादेवी अपनी रचनाओं में अत्यधिक संवेदनशील हैं अतः उनकी रचनाओं में अनुभूति की गहन तीव्रता है। नीहार के बाद की रचनाओं में उनकी रचनाओं में रहस्यवादी प्रवृत्ति देखी जा सकती है। वेदनाभाव महादेवी की रचनाओं की प्रमुख विशेषता है। यद्यपि यह वेदनाभाव प्रियतम के अद्वैत का साधन रूप ही है तथापि महादेवी ने वेदना को आनन्द से सर्वथा उंचा स्थान दिया है। दुखानुभूति को लेकर महादेवी अज्ञात सत्ता की ओर उन्मुख हुई हैं। इस सत्ता को उन्होंने अपने प्रियतम के रूप में स्वीकार किया। प्रकृति का महादेवी के काव्य में भी प्रमुख स्थान है।
महादेवी के भाव एवं कला पक्ष दोनों ही सबल एवं समृद्ध हैं। भाषा अत्यन्त परिष्कृत, सरस एवं कोमल है। इनकी भाषा में लाक्षणिकता अधिक एवं अनुभूतियां अन्तर्मुखी हैं। तन्मयता, अनुभूति की तीव्रता तथा माधुर्य महादेवी के गीतों की प्रमुख विशेषताएं हैं।
यद्यपि छायावाद के ये ही चार कवि स्तम्भ माने जाते हैं किन्तु इस काल में अन्य अनेक कवियों ने उत्कृष्ट रचनाएं लिखीं जो तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, एवं कालिक चेतना से प्रभावित एवं छायावादी प्रवृत्तियों से भी प्रभावित रहीं।
हरिवंशराय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियारामशरण गुप्त, भगवतीचरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्राकुमारी चौहान, रामकुमार वर्मा, पं. नरेन्द्र शर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, जानकी वल्लभ शास्त्री, उदयशंकर भट्ट, रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामनरेश त्रिपाठी, आदि कवि भी इस काल के प्रभावी रचनाकार रहे।
इन कवियों की कविताएं यद्यपि छायावादी काल में रची गईं किन्तु इनकी रचनाओं पर इनकी अपनी दृष्टि अधिक प्रभावी रही। हरिवंशराय बच्चन की कविता मौज, मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता है। इनकी कविता की मादकता ने सहृदयों को आकर्षित किया। लाक्षणिक वक्रता से हटकर सहज-सीधी भाषा के प्रयोग के कारण बच्चन बहुत लोकप्रिय हुए। रामधारी सिंह दिनकर व्यक्तिवादी दृष्टि का प्रत्याख्यान लेकर साहित्य मंच पर आये। वे छायावादी एवं प्रगतिवादी के बीच की कड़ी हैं।
बालकृष्ण शर्मा नवीन फ़क्कड़ कवि के रूप में जाने जाते हैं इनकी कविताएं राजनीतिक परिदृश्य से जुड़ी रहीं। सियारामशरण गुप्त चिन्तनशील कवि रहे। सहानुभूति से भरा हृदय, संसार के प्रति अनासक्त जिज्ञासा इनके काव्य के मूल में है। इनकी रचनाओं पर गांधी का प्रभाव स्पष्ट है। भगवतीचरण वर्मा की रचनाओं में मस्ती और उल्लास है और अपने प्रति दृढ़ विश्वास। उनकी आत्मकेन्द्रित मस्ती बाद में उनके उपन्यासों में व्यक्त हुई।
माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में छायावादी तत्वों से अधिक देश-प्रेम एवं देश-कल्याण के लिए उत्कट भावना है। यद्यपि आरभ्भिक रचनाओं में निर्गुण एवं सगुण भक्ति और रहस्य-भावना भी लक्षित होती है।
सुभद्राकुमारी चौहान राजनीति में सक्रिय भाग लेती रहीं अतः इनकी रचनाओं में राष्ट् प्रेम का भाव प्रमुख है। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ रचनाएं पारिवारिक जीवन से प्रेरित हैं।
अन्य उल्लिखित कवियों की रचनाओं में भी छायावादी तत्वों के साथ अन्य समसामयिक विषय प्रधान रहे।
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि छायावाद ने अभिव्यक्ति-शैली के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति की।
छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया। वैयक्तिकता, भावात्मकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, कोमलता आदि सभी गीति-तत्वों का समावेश छायावादी काव्य में मिलता है। छन्द योजना में मौलिकता है। निराला ने अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए मुक्त छन्द का आविष्कार किया। प्रतीकात्मकता छायावाद की एक अन्य विशेषता है। अपने सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति के लिए लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली अपनाई, शब्द-शक्ति में अभिधा के स्थान पर लक्षणा व व्यंजना से काम लिया। उपमान-विधान के क्षेत्र में छायावादी कवियों ने मूर्त के लिए अमूर्त उपमान प्रयोग किये। इन कवियों ने जहां एक ओर उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक आदि पारम्परिक अलंकारों को लिया वहां दूसरी ओर उसमें मानवीकरण, विरोधाभास, विशेषण-विपर्पय आदि पाश्चात्य ढंग के अलंकार भी समाहित किये। छायावाद की भाषा का रूप प्रौढ़ हैं इसमें प्रायः संस्कृत की कोमल-कांत पदावली के दर्शन होते हैं। खड़ी बोली को संवारने में छायावादी कवियों का महत्त योगदान है।
सारांश यह कि भाव-पक्ष एवं कला-पक्ष दोनों ही दृष्टियों से छायावाद काव्य अत्यन्त प्रौढ़ है।
वामा
हमारे ग्रंथों में लिखे वाक्य
हमारे लिए आप्त वाक्य हैं
ऐसा ही कहते हैं सब।
कोई विरोध नहीं,
कोई चर्चा नहीं,
कोई मतभेद नहीं।
इन ग्रंथों में
ऐसा ही कुछ लिखा है
स्त्री के बारे में
कि पुरुष की वामा है वह।
हमारे ग्रंथ कहते हैं
स्त्रियों की उत्पत्ति
शिव के वाम अंग से हुई
इसी कारण
हर स्त्री वामांगी, अर्धांगिनी कहलाई।
सारे कर्मों में स्त्री को
पुरुष के
वाम अंग में ही रहना चाहिए।
कुछ बातें समझ न सकी मैं
इसलिए
प्राचीन कथाओं में चली गई।
वहाॅं जाकर ज्ञानवृद्धि हुई मेरी।
प्रथम यह
कि कुछ कर्म सांसारिक होते हैं
और कुछ पारलौकिक।
लौकिक ओर पारलौकिक
तो आप समझते ही होंगे न।
सांसारिक कर्मों में
स्त्री पुरुष की वामांगी है
और पारलौकिक कर्मों में
स्त्री दाईं ओर चली जाती है।
पता नहीं आप समझे या नहीं,
स्त्री की आवश्यकता
लौकिक कार्यों तक ही सीमित है।
अलौकिकता के आते ही
उसके वामांगी के, अर्धागिंनी के
सारे अधिकार
छीन लिये जाते हैं
और वह दाईं ओर चली जाती है।
रिश्ते
समय की मार में
जो बदल जायें
वे रिश्ते नहीं होते।
रिश्ते क्या होते है
तब ही समझ पाते हैं
जब वे
बदल जाते हैं।
***
अफ़सोस
कि हम
बदलते रिश्तों की सूरत
समझ नहीं पाते
और आजीवन
बिखरे रिश्तों को
ढोते रहते हैं।
**
समय की चोट
रिश्तों को
बार&बार
नया नाम दे देती है
और हम नासमझ
पुराने नामों के साथ ही
उन्हें
आजीवन ढोते रहते हैं।
***
टूटे]
रिश्तों को
छोड़ने की
हिम्मत नहीं करते
इस कारण
रोज़]
हर रोज़ मरते हैं।
**-*
आस बनाये रखना
ज़िन्दगी में आस बनाये रखना
मन में तुम उमंग जगाये रखना
न निराश हो कि जीवन हार रहा
धरा में अंकुरण बनाये रखना
इतना पानी बरसा
इतना पानी बरसा, देख-देखकर मन डरे
कितने घर उजड़ गये, आंखों में आंसू भरे
सड़कें सागर बन गईं, घर मानों गह्वर बने
कैसे चलेगा जीवन आगे, गहन चिन्ता करें।
दर्पण
दर्पण हाथ में लिए घूमती हूॅं
चेहरों को परखती घूमती हूॅं
अपना ही चेहरा मटमैला है
दर्पण बदलने के लिए घूमती हूॅं।
सुन्दर जीवन
रंगों में मनमोहक संसार बसा है
पंछियों के मन में नेह रमा है
मन ही मन में बात करें देखो
सुन्दर जीवन का रंग रचा है
मौसम में हलचल
मौसम में हलचल है, ओलों की मार है
कभी चमकती धूप, कभी होती बौछार है
कभी हवाएॅं उड़ा देतीं और शीत डराती,
कभी लगता आ गई गर्मी, मन बेकरार है
सत्य को नकार कर
झूठ, छल-कपट से नहीं चलती है ज़िन्दगी
सत्य को नकार कर नहीं बढ़ती है ज़िन्दगी
क्यों घोलते हो विषबेल अकारण ही शब्दों की
तुम्हारे इस बुरे व्यवहार से टूटती है ज़िन्दगी
जीवन
बात करते-करते मन अक्सर बुझ-सा जाता है
कभी आंखों में तरलता का आभास हो जाता है
तुम्हारी कड़वाहटें अन्तर्मन को झकझकोरती हैं
न जाने जीवन में ऐसा अक्सर क्यों हो जाता है
बालपन की मस्ती
बालपन की मस्ती है, अपनी पतंग छोड़ेगे नहीं
डालियाॅं कमज़ोर तो क्या, गिरने से डरते नहीं
मित्र हमारे साथ हैं, थामे हाथों में हाथ हैं
सूरज ने बांध ली पतंग, हम उसे छोडे़गे नहीं
खुश रहिए
पढ़ने का बहाना लेकर घर से बाहर आई हूॅं
रवि किरणों की मधुर मुस्कान समेटने आई हूॅं
उॅंचे-उॅंचे वृक्षों की लहराती डालियाॅं पुकारती हैं
हवाओं के साथ हॅंसने-गुनगुनाने आई हूॅं।
अमर होकर क्या करेंगे
अमर होकर क्या करेंगे, बहुत जीकर क्या करेंगे
प्रेम, नेह, दुख-सुख, हार-जीत सब चलते रहेंगे
रोज़ नये किस्से, नई कथाएॅं, न जाने क्या-क्या
कुछ अच्छा नहीं लगता, पर किस-किससे लड़ेंगे।
छोटी ही चाहते हैं मेरी
छोटा-सा जीवन, छोटी ही चाहते हैं मेरी
क्या सोचते हैं हम, कौन समझे भावनाएॅं मेरी
अमरत्व की चाह तो बहुत बड़ी है मेरे लिए
इस लम्बे जीवन में ही कहाॅं पहचान बन पाई मेरी
सीता की वेदना
सीता क्या पूछ पाई कभी विधाता से, मैं ही क्यों माध्यम बनी
मैं थी रावण धाम में फिर मेरे चरित्र पर ही क्यों अॅंगुली उठी
मृग की कामना, द्वार आये साधु का मान मेरा अपराध बन गया
किसी का श्राप, वरदान, मुक्ति क्यों मेरे निष्कासन का द्वार बनी।
डरने लगे हैं
हम द्वार खुले रखने से डरने लगे हैं
मन पर दूरियों के ताले लगने लगे हैं
कुछ कहने से डरता है मन हर बार
हम छाछ और पानी दोनों से जले हैं
प्राकृतिक सौन्दर्य
प्रतिबिम्बित होती किरणों की प्रतिच्छाया शोभित है
फूलों की दमकती गुलाबी आभा से मन मोहित है
तितली बैठी धूप सेंकती, फूलों से अनुराग बंधा
मोहक, सुन्दर, सौम्य छवि देख मन आलोकित है
मन में राम
मन में राम, कण-कण में राम
तो क्यों खोजें उनको चारों धाम
भला करेंगे सबका वे बिन पूछे
सच्चे मन से करते हम हर काम।