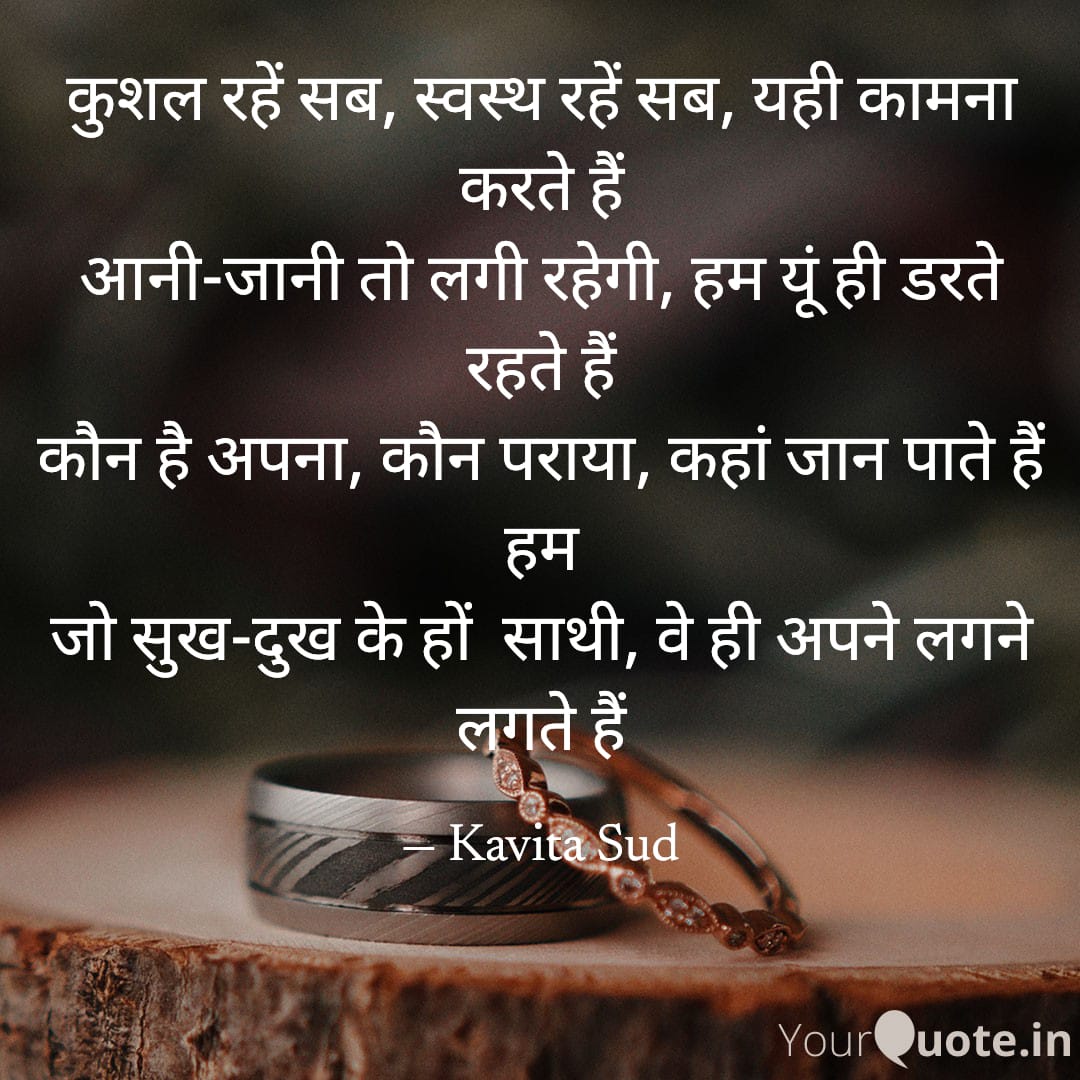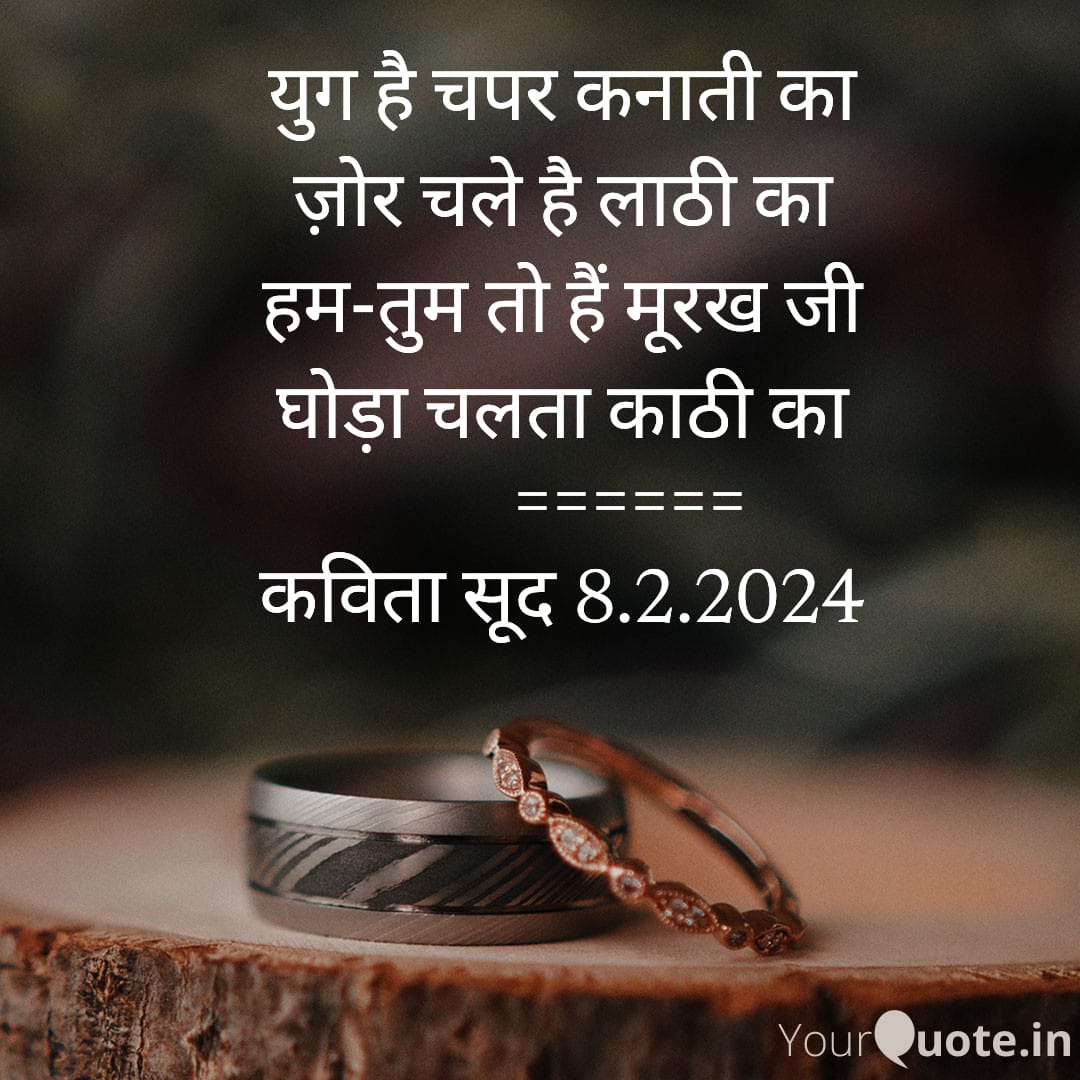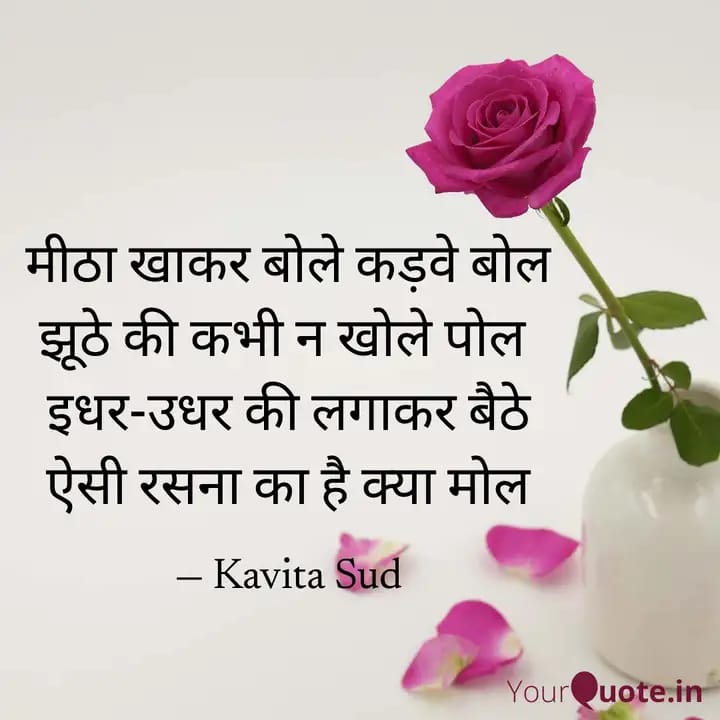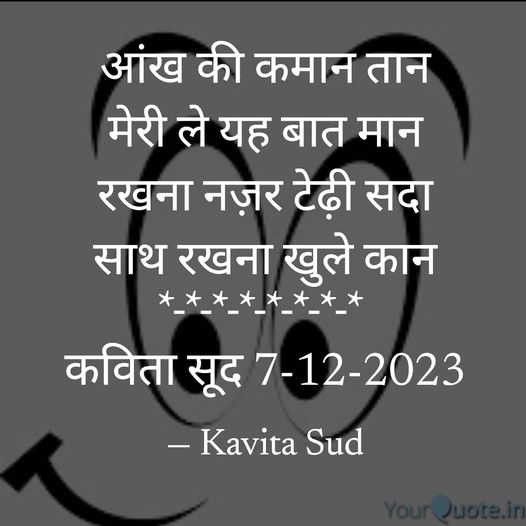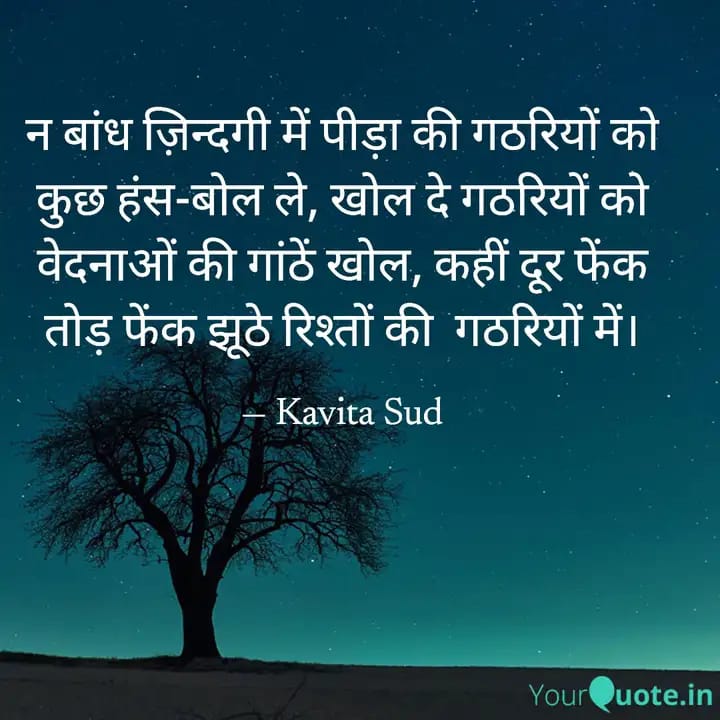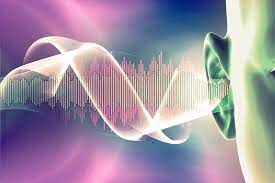कुशल रहें सब, स्वस्थ रहें
कुशल रहें सब, स्वस्थ रहें सब, यही कामना करते हैं
आनी-जानी तो लगी रहेगी, हम यूं ही डरते रहते हैं
कौन है अपना, कौन पराया, कहां जान पाते हैं हम
जो सुख-दुख के हों साथी, वे ही अपने लगने लगते हैं
रंगों में जीवन को आशा
मुक्त गगन में चिड़िया को उड़ते देखा
भोर के सूरज की सुरमई आभा को देखा
मन-मयूर कहता है चल उड़ चलें कहीं
रंगों में जीवन को आशाओं में पलते देखा
हम-तुम तो हैं मूरख जी
युग है चपर कनाती का
ज़ोर चले है लाठी का
हम-तुम तो हैं मूरख जी
घोड़ा चलता काठी का
कड़वे बोल
मीठा खाकर बोले कड़वे बोल
झूठे की कभी न खोले पोल
इधर-उधर की लगाकर बैठे
ऐसी रसना का है क्या मोल
चिड़ियाॅं रानी
गुपचुप बैठी चिड़ियाॅं रानी
चल कर लें दो बातें प्यारी
कुछ तुम बोलो, कुछ मैं बोलूं
मन की बातें कर लें सारी
मौसम के रॅंग
सहमी-सहमी धूप है, खिड़कियों से झांक रही
कुहासे को भेदकर देखो घर के भीतर आ रही
पग-पग चढ़ती, पग-पग रुकती, कहाँ चली ये
पकड़ो-पकड़ो भाग न जाये, मेरे हाथ न आ रही।
दुख-सुख तो आने-जाने हैं
मिल जाये जब मज़बूत सहारा राहें सरल हो जाती हैं
कौन है अपना, कौन पराया, ज़रा पहचान हो जाती है
दुख-सुख तो आने-जाने हैं, किसने देखा, किसने समझा
जब हाथ थाम ले कोई, राहें समतल,सरल हो जाती हैं।
तू कोमल नार मैं तेरा प्यार
हाथ जोड़ता हूँ तेरे, तेरी चप्पल टूट गई, ला मैं जुड़वा लाता हूँ
न जा पैदल प्यारी, साईकल लाया मैं, इस पर लेकर जाता हूँ
लोग न जाने क्या-क्या समझेंगे, तू कोमल नार मैं तेरा प्यार
आजा-आजा, आज तुझे मैं लाल-किला दिखलाने ले जाता हूँ
माँ की ममता
जीवन के सुखमय पल बस माँ के संग ही होते हैं
नयनों से बरसे नेह, संतति के सुखद पल होते हैं
हिलमिल-हिलमिल बस जीवन बीता जाता यूँ ही
किसने जाना, माँ की ममता में अनमोल रत्न होते हैं।
वन्दन करें अभिनन्दन करें
देश की आन, शान, बान के लिए शहीद हुए, मोल न लगाईये
उनकी दिखाई राह पर चल सकें, बस इतनी सोच ही बढ़ाईये
भारत की सुन्दर धरा को निखार सकें, इतना विचार कीजिए
वन्दन करें, अभिनन्दन करें, उनकी शान में शीश ही झुकाईये
आंख की कमान तान
आंख की कमान तान
मेरी ले यह बात मान
रखना नज़र टेढ़ी सदा
साथ रखना खुले कान
दो पंछी
गुपचुप, छुपछुपकर बैठे दो पंछी
नेह-नीर में भीग रहे दो पंछी
घन बरसे, मन हरषे, देख रहे
साथ-साथ बैठे खुश हैं दो पंछी
बस यूं ही
बेमौसम मन में बिजली कड़के
जब देखो दाईं आंख है फ़ड़के
मन यूं ही बस डरने लगता है
आंखों से तब गंगा-यमुना बरसे
वेदनाओं की गांठें खोल
न बांध ज़िन्दगी में पीड़ा की गठरियों को
कुछ हंस-बोल ले, खोल दे गठरियों को
वेदनाओं की गांठें खोल, कहीं दूर फेंक
तोड़ फेंक झूठे रिश्तों की गठरियों को
इच्छाएं अनन्त
इच्छाएं अनन्त, फैली दिगन्त
पूर्ण होती नहीं, भाव भिड़न्त
कितनी है भागम-भाग यहां
प्रारम्भ-अन्त सब है ज्वलन्त
धागा प्रेम का
रहिमन धागा प्रेम का
कब का गया है टूट।
गांठें मार-मार,
रहें हैं रस्सियाॅं खींच।
रस्सियाॅं भी अब गल गईं
धागा-धागा बिखर रहा।
गांठों को सहेजकर
बंधे नहीं अब मन की डोर।
न जाने किस आस में
बैठे हाथों को जोड़।
जो छूट गया
उसे छोड़कर
अब तो आगे बढ़।
प्रेम-प्यार के किस्से
हो गये अब तो झूठ
हीर-रांझा, लैला-मजनूं
को जाओ अब तुम भूल।
रस्सियों का अब गया ज़माना
कसकर हाथ पकड़कर घूम।
अच्छा ही हुआ
अच्छा ही हुआ
कोई समझा नहीं।
कुछ शब्द थे
जो मैं यूॅं ही कह बैठी,
मन का गुबार निकाल बैठी।
कहना कुछ था
कह कुछ बैठी।
न नाराज़गी थी
न थी कोई खुशी।
पर कुछ तो था
जो मैं कह बैठी।
बहुत कुछ होता है
जो नहीं कहना चाहिए
बस मन ही मन में
कुढ़ते रहना चाहिए
अन्तर्मन जले तो जले
पर दुनिया को
कुछ भी पता न चले।
वैसे भी मेरी बातें
कहाॅं समझ आती हैं
किसी को।
पर
ऐसा कुछ तो था
जो नहीं कहना चाहिए था
मैं यूॅं ही कह बैठी।
बसन्त के फूल खिलें
फूलों के बसन्त की
प्रतीक्षा नहीं करती मैं
मन में बसन्त के फूल खिलें
बस इतना ही चाहती हूं मैं
जीवन की राहों में
कदम-ताल करते चलें
मन में उमंग
भावों में तरंग
बगिया में हर रंग
और तुम संग
सुनहरे रंगों की लकीर
आप ही खिंच जाती है
ज़िन्दगी में
तो और क्या चाहिए भला।
जब से मुस्कुराना देखा हमारा
जब से मुस्कुराना देखा हमारा
न जाने क्यों आप चिन्तित दिखे
-
हमारे उपवन में फूल सुन्दर खिले
तुम्हारी खुशियों पर क्यों पाला पड़ा
-
चली थी चाॅंद-तारों को बांध मुट्ठी में मैं
तुम क्यों कोहरे की चादर लेकर चले
-
बारिश की बूंदों से आह्लादित था मेरा मन
तुम क्यों आंधी-तूफ़ान लेकर आगे बढ़े
-
भाग-दौड़ तो ज़िन्दगी में लगी रहती है
तुम क्यों राहों में कांटे बिछाते चले।
-
अब और क्या-क्या बताएॅं तुम्हें
-
हमने अपना दर्द छिपा लिया था
झूठी मुस्कुराहटों में
तुम कभी भी तो यह न समझ पाये।
कहीं सच न बोल बैठे
रहने दो मत छेड़ो दर्द को
कहीं सच न बोल बैठे।
राहों में फूल थे
न जाने कांटे कैसे चुभे।
चांद-सितारों से सजा था आंगन
न जाने कैसे शूल बन बैठे।
हरी-भरी थी सारी दुनिया
न जाने कैसे सूखे पल्लव बन बैठे।
सदानीरा थी नदियां
न जाने कैसे हृदय के भाव रीत गये।
रिश्तों की भीड़ थी मेरे आस-पास
न जाने कैसे सब मुझसे दूर हो गये।
स्मृतियों का अथाह सागर उमड़ता था
न जाने कैसे सब पन्ने सूख गये।
सूरज-चंदा की रोशनी से
आंखें चुंधिया जाती थीं
न जाने कैसे सब अंधेरे में खो गये।
बंद आंखों में हज़ारों सपने सजाये बैठी थी
न जाने कैसे आंख खुली, सब ओझल हो गये।
नहीं चाहा था कभी बहुत कुछ
पर जो चाहा वह भी सपने बनकर रह गये।
ध्वनियां विचलित करती हैं मुझे
कुछ ध्वनियां
विचलित करती हैं मुझे
मानों
कोई पुकार है
कहीं दूर से
अपना है या अजनबी
नहीं समझ पाती मैं।
कोई इस पार है
या उस पार
नहीं परख पाती मैं।
शब्दरहित ये आवाजे़ं
भीतर जाकर
कहीं ठहर-सी जाती हैं
कोई अनहोनी है,
या किसी अच्छे पल की आहट
नहीं बता पाती मैं।
कुछ ध्वनियां
मेरे भीतर भी बिखरती हैं
और बाहर की ध्वनियों से बंधकर
एक नया संसार रचती हैं
अच्छा या बुरा
दुख या सुख
समय बतायेगा।
वीरों को नमन
उन वीरों को हम
सदा नमन करें
जो हमें खुली हवाओं में
सांस लेने का अवसर
देकर गये।
उनके बलिदान का हम
सदा सम्मान करें
जो देश के लिए
दीवारों में चिन दिये गये।
उनके लिए
अपना देश ही धर्म था
और था आज़ादी का सपना।
आज़ादी और अपने धर्म के लिए
उनकी जलाई ज्योति
अखंड जली
और भारत आज़ाद हुआ।
महत्व इस बात का नहीं
कि उनकी आयु क्या थी
महत्व इस बात का
कि उनका लक्ष्य क्या था।
बस इतना स्मरण रहे
कि हम उनसे मिले भाव को
मिटा न दें
ऐसा कोई कर्म न करें
कि उनका बलिदान शर्मिंदा हो।
जीवन के नवीन रंग
प्रकृति
नित नये कलेवर में
अवतरित होती है
रोज़ बदलती है रंग।
कभी धूप
उदास सी खिलती है
कभी दमकती,
कभी बहकती-सी,
बादलों संग
लुका-छिपी खेलती।
बादल
अपने रंगों में मग्न
कभी गहरे कालिमा लिए,
कभी झक श्वेत,
आंखें चुंधिया जाते हैं।
और जब बरसते हैं
तो आंखों के मोती-से
मन भिगो-भिगो जाते हैं
कभी सतरंगी
ले आते हैं इन्द्रधनुष
नित नये रंगों संग
मन बहक-बहक जाता है।
प्रात में जब सूर्य-रश्मियां
नयनों में उतरती हैं
पंछियों का कलरव
नित नव संगीत रचता है,
तब हर दिन
जीवन नया-सा लगता है।
मधुर भावों की आहट
गुलाबी ठंड शीत की
आने लगी है।
हल्की-हल्की धूप में
मन लगता है,
धूप में नमी सुहाने लगी है।
कुहासे में छुपने लगी है दुनिया
दूर-दृष्टि गड़बड़ाने लगी है।
रेशमी हवाएं
मन को छूकर निकल जाती हैं
मधुर भावों की आहट
सपने दिखाने लगी है।
रातें लम्बी
दिन छोटे हो गये
नींद अब अच्छी आने लगी है।
चाय बनाकर पिला दे कोई,
इतनी-सी आस
सताने लगी है।
सूर्य उत्तरायण हो गये आज
सूर्यदेव उत्तरायण हो गये आज।
दिन बड़े होने लगे,रातें छोटी।
प्रकाश बढ़ने लगता है
और अंधेरी रातों का डर
कम होने लगता है,
और प्रकाश के साथ
सकारात्मकता का बोध
होने लगता है।
कथा है कि
भीष्म पितामह ने
प्रतीक्षा की थी
देह-त्याग के लिए
सूर्य के उत्तारयण की।
हमारे ग्रंथ कहते हैं
कि उत्तरायण के प्रकाश में
देह-त्याग करने वालों को
पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता,
मुक्त हो जाते हैं वे
जन्म-मरण के जाल से।
.
मैं नहीं चाहती मुक्ति।
चाहती हूॅं
जन्म मिले बार-बार,
न मरने से डरती हूॅं
न जीने से।
अच्छा लगता है
एक इंसान होना,
इच्छाओं के साथ जीना,
कामनाओं को पूरा करना।
जो इस बार न कर पाई
अगले जन्म में
या उससे भी
अगले जन्म में करुॅं,
बार-बार जीऊॅं,
बार- बार मरुॅं।
न जीने से डरती हूॅं
न मरने से।
चलो खिचड़ी पकाएॅं
वैसे तो
रोगियों का भोजन है
खिचड़ी,
स्वादहीन,
कोई खाना नहीं चाहता।
किन्तु जब
हमारे-तुम्हारे बीच पकती है
कोई खिचड़ी
तो सारी दुनिया के कान
खड़े हो जाते हैं,
मुहॅं का स्वाद
चटपटा हो जाता है
कहानियाॅं बनती हैं
मिर्च-मसाले से
जिह्वा जलने लगती है,
घूमने लगते हैं आस-पास
जाने-अनजाने लोग।
क्या पकाया, क्या पकाया?
अब क्या बताएॅं
तुम भी आ जाओ
हमारे गुट में
मिल-बैठ नई खिचड़ी पकायेंगे।
छिल जाती है कई ज़िन्दगियाॅं
कोई विशेष
वैज्ञानिक जानकारी तो नहीं मुझे,
पर सुना है
कि नसों, नाड़ियों में
रक्त बहता है,
हम देख नहीं सकते
बस एक अनुभव है
जानकारी मात्र।
कहते हैं,
जब व्यवधान आ जाता है
इन नसों, नाड़ियों में
तो वैसे ही साफ़ करवानी पड़ती हैं
ये नसें, नाड़ियाॅं
जैसे हमारे घरों की नालियाॅं ,
अन्तर बस इतना ही
कि घरों की
नालियों की सफ़ाई में
एक छोटा-सा मूल्य देना पड़ता है,
अन्यथा
और रास्ते भी निकल आते हैं प्रवाह के।
किन्तु जब रुकती हैं
देह की नसें, नाड़ियाॅं
तो छिल जाती है ज़िन्दगी
और
साथ जुड़ी कई ज़िन्दगियाॅं।
मैला मन में जमे
नसों-नाड़ियों में
या नालियों में,
समय रहते साफ़ करते रहें
नहीं तो
तो छिल जाती है ज़िन्दगी
और
साथ जुड़ी कई ज़िन्दगियाॅं।
शब्द अधूरे-से
प्रेम, प्यार
दो टूटू-फूटे-से शब्द
अधूरे-से लगते हैं।
पता नहीं क्यों
हम तरसते रहते हैं
इन अधूरे शब्दों को
पूरा करने के लिए
ज़िन्दगी-भर।
कहाॅं समझ पाता है कोई
हमारी भावनाओं को।
कहाॅं मिल पाता है कोई
जो इन
अधूरे शब्दों को
पूरा करने के लिए
अपना समर्पण दे।
यूॅं ही बीत जाती है
ज़िन्दगी।
नूतन श्रृंगार
इस रूप-श्रृंगार की
क्या बात करें।
नारी के
नूतन श्रृंगार की
क्या बात करें।
नयन मूॅंदकर
हाथ बांधकर
कहाॅं चली।
माथ है बिन्दी
कान में घंटा।
हाथ कंगन सर्पाकार,
सजे आलता,
गल हार पहन
कहाॅं चली।
यह नूतन सज्जा
मन मोहे मेरा,
किसने अभिनव रूप
सजाया तेरा
कौन है सज्जाकार।
नमन करुॅं मैं बारम्बार ।
सलवटें
कपड़ों पर पड़ी सलवटें कोशिश करते रहने से कभी छूट भी जाती हैं, किन्तु मन पर पड़ी अदृश्य सलवटों का क्या करें, जिन्हें निकालने की कोशिश में आंखें नम हो जाती हैं, वाणी बिखर जाती हैं, कपड़ों पर घूमती अंगुलियों में खरोंच आ जाती है। कपड़े तह-दर-तह सिमटते रहते हैं और मैं बिखरती रहती हूॅं।