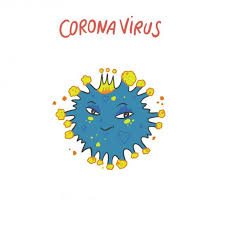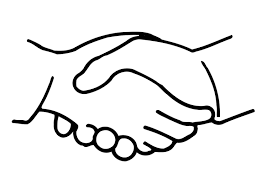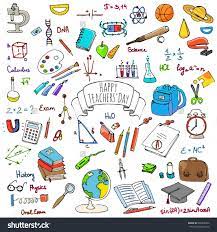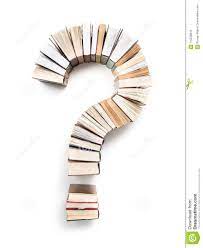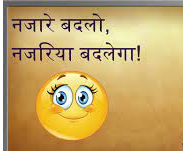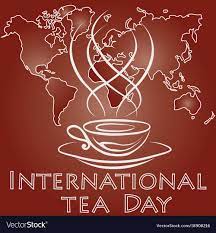भ्रष्टाचार
जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं और दूसरे की ओर उंगली उठाते हैं तो चार उंगलियां स्वयंमेव ही अपनी ओर उठती हैं जिन्हें हम स्वयं ही नहीं देखते। यह पुरानी कहावत है।
वास्तव में हम सब भ्रष्टाचारी हैं। बात बस इतनी है कि जिसकी जितनी औकात है उतना वह भ्रष्टाचार कर लेता है। किसी की औकात 100 रू. की है तो किसी की 100 करोड़ की। किन्तु 100 रू वाला स्वयं को ईमानदार कहता है। हम मंहगाई की बात करते हैं किन्तु सुविधाभेागी हो गये हैं। बिना कष्ट उठाये धन से हर कार्य करवा लेना चाहते हैं। हमें दूसरे का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार लगता है और अपना आवश्यकता, विवशता।
यदि हम अपनी ओर उठने वाली चार उंगलियों के प्रश्न और उत्तर दे सकें तो शायद हम भ्रष्टाचार के विरूद्ध अपना योगदान दे सकते हैं:
पहली उंगली मुझसे पूछती है: क्या मैं विश्वास से कह सकते हूं कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं।
दूसरी उंगली कहती है: अगर मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं तो क्या भ्रष्टाचार का विरोध करती हूं ?
तीसरी उंगली कहती है: कि अगर मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं किन्तु भ्रष्टाचार का विरोध नहीं करती तो मैं उनसे भी बड़े भ्रष्टाचारी हूं।
और अंत में चौथी उंगली कहती है: अगर मैं भी भ्रष्टाचारी हूं तो सामने की उंगली को भी अपनी ओर मोड़ लेना चाहिए और मुक्का बनाकर अपने पर वार करना चाहिए। दूसरों को दोष देने और सुधारने से पहले पहला कदम अपने प्रति उठाना होगा।
यदि प्रत्येक नागरिक आत्मनियन्त्रण करे तो भ्रष्टाचार अवश्य ही दूर होगा।
सचेत रहना या संदेह करना To
कुछ समय पूर्व मेरी अपनी महिला सहकर्मी से चर्चा हुई फेसबुक मित्रों पर, जो मेरी फेसबुक मित्र भी है। उसने बताया कि उसके फेसबुक मित्रों में केवल परिवार के अथवा पूर्व परिचित लोग ही हैं, कोई भी अपरिचित नहीं है जिसे उसने फेसबुक पर ही मित्र बनाया हो । वाट्सएप, एवं अन्य प्रकार से भी वे उसी दायरे में हैं। मैंने सोचा तो नया क्या ।
मैंने बताया कि एक अपने पुत्र, उसके मित्र एवं कुछ महिला मित्रों के अतिरिक्त मेरी मित्र सूची में अधिकांश अपरिचित हैं जिन्हें मैंने फेसबुक पर ही मित्र बनाया है। अलग से उनसे न तो कोई पारिवारिक, मैत्री सम्बन्ध है, न कोई पूर्व परिचय। ऐसे ही कुछ समूहों की भी सदस्य हूं और वहां भी कोई पूर्व परिचित नहीं है।
आज ज्ञानचक्षु खुले , बात एक ही है।
मेरे संदेश बाक्स में प्रतिदिन लगभग दस मित्रों के सुप्रभात से लेकर शुभरात्रि तक के संदेश प्राप्त् होते थे, जिनका मैं यथासमय उत्तर भी देती हूं। पिछले एक माह से संदेश निरन्तर आ रहे हैं मैं उत्तर नहीं दे पाई, किन्तु। एक भी प्रश्न नहीं हैं, ‘’कहां हैं आप’’।
शिकायत नहीं है किसी से, मैं भी कौन-सा किसी को पूछती हूं।
फिर मैंने और जानने का प्रयास किया तो जाना कि अधिकांश महिलाओं की मित्र सूची में परिवार के अथवा पूर्व परिचित लोग ही हैं। अर्थात वे अपने सामाजिक, पारिवारिक जीवन में, मोबाईल, वाट्स एप पर भी उनसे निरन्तर सम्पर्क में हैं और वे ही फेसबुक पर भी हैं।
फिर फेसबुक पर उनके लिए नया क्या ?
क्या हमें सत्य ही इतना डर कर रहना चाहिए जितना डराया जाता है।
क्यों हम सदैव ही किसी अपरिचित को अविश्वास की दृष्टि से ही देखे ?
जीवन में यदि हम अपरिचितों की उपेक्षा, संदेह, दूरियां ही बनाये रखेंगे तो समाज कैसे चलेगा।
सचेत रहना अलग बात है, अकारण संदेह में रहना अलग बात।
कोरोनामय वातावरण में मानसिकता
एक बात समझ नहीं पा रही हूं। जब से कोरोना या कोविड -19 आया है, पहले की तरह साधारण बुखार, वायरल, गला खराब, खांसी-जुकाम होना बन्द हो गया है क्या? मौसम बदलने पर, बारिश में भीगने पर, सर्दी लग जाने पर, ज़्यादा धूप में घूमने या लू लग जाने पर, ए सी या कूलर की सीधी हवा लग जाने से उक्त समस्याएं हो जाती थीं। अब क्या ये सब बन्द हो गई हैं, सीधा कोरोना ही होता है क्या? आजकल चिकित्सकों की बात से तो ऐसा ही लगता है। घर में किसी को इनमें से कोई समस्या होने पर किसी चिकित्सक को फोन कीजिए कि एक-दो दिन से बुखार है अथवा उक्त सारी समस्याओं में से कोई समस्या है। सीधा दो टूक उत्तर मिलता है कोरोना टैस्ट करवा लीजिए।
नहीं डाक्टर ऐसी बात नहीं है।
डाक्टर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं।
नहीं पहले आप कोरोना टैस्ट करवा लीजिए, फिर देखेंगे।
लेकिन डाक्टर, उसमें तो दो दिन लग जायेंगे, बुखार तो तेज़ है।
तो ठीक है ये दो गोली नोट कर लीजिए, 100 बुखार होने तक पहली गोली दे देना दिन में एक बार। 101 से ज़्यादा होने पर पी सी एम दे देना।
मिलते-जुलते उत्तर ही मिलते हैं।
अब मान लीजिए 1 तारीख को बुखार हुआ। हर कोई पहले तो घर में ही रखी पी सी एम या क्रोसीन ले लेता है। दूसरे दिन बुखार न उतरने पर डाक्टर को फोन किया। डाक्टर का उत्तर आपने पढ़ लिया। तीसरे दिन टैस्ट करवाया। पांचवें दिन रिपोर्ट मिली। नैगेटिव।
डाक्टर ने नैगेटिव रिपोर्ट की बात सुनकर कहा, चलो ठीक है, आप बुखार की ये दवाई ले लीजिए।
किन्तु वे पांच दिन कितने भारी थे, उन पांच दिन में बुखार बिगड़कर कोई भी रूप ले लेता है, कोरोना का नहीं। क्या उन पांच दिन के लिए साधारण बुखार की या वायरल की दवाई नहीं दी जा सकती थी, मैं तो डाक्टर नहीं हूं। कोई बतायेगा क्या?
जीवन की अनहोनी घटना
मेरे जीवन में ऐसी बहुत-सी घटनाएं घटी हैं जो अनहोनी हैं।
हमारे परिवार पर एक प्रकोप रहा है न जाने क्यों, कि कभी भी परिवार में एक मृत्यु नहीं होती थी, दो होती थीं। एक साथ नहीं किन्तु तेहरवीं से पहले। जैसे जब मेरे पिता का निधन हुआ तब मेरे चाचाजी के बेटे का चैथे दिन निधन हुआ। इसी प्रकार दूर-पार की रिश्तेदारी में किसी न किसी का निधन हो जाता था। वर्षों तक ये सब हमने देखा।
यह परम्परा है कि यदि क्रिया से पूर्व कोई पातक मृत्यु या सूतक जन्म हो जाये तो क्रिया उस दिन से 13 दिन आगे बढ़ जाती है।
अर्थात मेरे पिता की क्रिया और चाचाजी के बेटे की क्रिया जिसे तेरहवीं कहते हैं एक ही दिन पर हुई।
सबसे बड़ा हादसा हमारे परिवार में नर्वदा बहन के निधन के बाद हुआ।
नर्वदा का निधन 26 फ़रवरी को हुआ। उनकी क्रिया अर्थात तेरहवीं 10 मार्च को होनी थी। 9 मार्च को मेरी चाचाजी के घर पोते ने जन्म लिया। अर्थात सूतक हो गया। अब नर्वदा की क्रिया 13 दिन आगे बढ़ गई और शायद 22 मार्च निर्धारित हुई। किन्तु 20 मार्च को मेरी मां का निधन हो गया। अर्थात पातक। अब 3 अप्रैल को दोनों की एक साथ क्रिया सम्पन्न हुई, नर्वदा के निधन के लगभग सवा महीने बाद। वे अत्यन्त खौफ़नाक दिन थे हमारे लिए।
हमारा व्यवहार हमारी पहचान
हमारा व्यवहार हमारी पहचान Our Behavior Our Identity
निःसंदेह हमारा व्यवहार हमारी पहचान है।
किन्तु कभी आपने सोचा है कि हमारा व्यवहार कैसे बनता है? व्यवहार क्या है? हम किसी से कैसे बात करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, अपने मनोभावों को कैसे प्रकट करते हैं, यही व्यवहार है। हँसना, बोलना, बात करना, प्रतिक्रिया देना, हाँ-ना, सहायता करना, न करना, प्रसन्नता, नाराज़गी, सम्मान-अपमान, सभी व्यवहार ही तो हैं।
हर व्यक्ति का प्रयास रहता है कि वह सामने वाले से अच्छा व्यवहार करे कि उसकी छवि अच्छी बनी रहे। किन्तु क्या सदैव ऐसा हो पाता है? नहीं।
कारण, बहुत बार हमारा व्यवहार सामने वाले के व्यवहार की प्रतिच्छाया होता है। क्योंकि हम एक साधारण इंसान हैं, कोई पहुँचे हुए धर्मात्मा नहीं, इस कारण सामने वाले का व्यवहार हमारे व्यवहार को बदल सकता है।
जैसे मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। मैं नहीं कह सकती कि मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, ये तो मुझे जानने वाले ही बता सकते हैं। किन्तु मेरे व्यवहार में तात्कालिक प्रतिक्रिया है
मैं अपने साथ बात अथवा व्यवहार करने वाले के प्रति प्रतिक्रिया बहुत जल्दी देती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हमारे समाज में अपशब्दों का एवं और अनेक तरीकों से महिलाओं के साथ शाब्दिक, सांकेतिक दुव्र्यवहार होता है। ऐसे समय मेरा व्यवहार बदल जाता है। मैं अत्यधिक क्रोधित एवं आक्रामक हो जाती हूँ, मेरी सहनशक्ति मेरा साथ छोड़ देती है और मैं तत्काल प्रतिक्रिया करती हूँ। जो निश्चित रूप से क्रोध एवं प्रतिकार ही होती है।
ऐेसे समय में मेरा व्यवहार मेरा अपना नहीं होता , सामने वाले के व्यवहार की प्रतिच्छाया होता है। मेरा यह व्यवहार अथवा स्वभाव मेरा स्थायी व्यवहार नहीं है किन्तु मेरी पहचान अवश्य है कि मैं गलत का विरोध करने का साहस रखती हूँ।
अतः मेरी दृष्टि में हमारा व्यवहार परिस्थितियों, कार्य-क्षेत्र, हमारे आस-पास के वातावरण, लोगों पर बहुत निर्भर करता है और सम्भव है हमारा ऐसा व्यवहार स्थायी न हो और हमारी पहचान न हो।
अतः किसी के व्यवहार और उस व्यवहार से उसकी पहचान मानने के लिए किसी भी व्यक्ति की कोई एक बात से उसे समझा और जाना नहीं जा सकता, एक जीवन जीना पड़ता है किसी के व्यवहार को समझने के लिए और पहचान बनाने के लिए।
कोविड वातावरण के कारण अस्त-व्यस्त मन की बातें
आजकल कुछ लिखने के लिए मन करता है पर लिखना हो नहीं पाता। क्यों? पता नहीं। वैसे भी मैं जल्दी कुछ लिख नहीं पाती और लेखन में भटकाव आ जाता है। इस समय भी कुछ विचार एक साथ उलझे पड़े हैं जैसे कोरोना, विस्थापित होते मज़दूर, हमारी चिकित्सीय व्यवस्थाएं, वेतन एवं वसूली, धार्मिक स्थल, मदिरालय एवं हमारे समाचार वाहक।
इस कारण एक अटपटा, उलझा-सा आलेख।
एक ओर तो कोरोना से घर में बैठे हैं, टी. वी. पर चलने वाले समाचार, समाचार कम, एक तीसरी श्रेणी का धारावाहिक अधिक प्रतीत होते हैं। वास्तविकता से हम कोसों दूर हैं। अब समाचार पत्र भी मिलने लगे हैं क्योंकि हम रैड ज़ोन से औरेंज ज़ोन में प्रवेश कर गये हैं।
विस्थापित मज़दूरों को पैदल चलते, जिनमें बच्चे, वृद्ध, रोगी सब हैं, सिर पर सामान उठाये, देखकर ही मन भयाक्रातं है। एक सरकार कहती है हम भेज रहे हैं, दूसरी कहती है हमारे पास इनको रखने के लिए जगह नहीं है। किसकी गलती है, कौन क्या कर रहा है, सब उलझा पड़़ा है। कल किसके साथ क्या होगा, पता नहीं। जो कल तक दैनिक मजदूर थे, परिश्रमी थे, आज भिक्षुक बनकर रह गये।
क्या करते थे ये सब। कहां रहते थे, अचानक सड़क पर आ गये, छतविहीन, भोजन रहित। दो-चार नहीं , लाखों की संख्या में। अनेक शहरों में , अनेक राज्यों में। कोई इनकी यूनियन तो थी नहीं कि पूरे देश में वाट्सएप किया और निकल लिए। जिस राज्य में रह रहे थे वहां न छत मिल रही थी न भोजन। जहां भी कार्य कर रहे थे, सब बन्द हो गये। रोज़गार जाने के साथ ही निवास भी चले गये और भोजन की व्यवस्था भी। अब क्या करें? जहां जाना चाहते थे, मार्ग नहीं था, सुविधा नहीं थी, धन नहीं था, व्यवस्था नहीं थी। किन्तु रहें कहां। जब कुछ नहीं मिला तो पैदल ही चल दिये, किसी ने राह में भोजन दे दिया तो ठीक, नहीं तो चले जा रहे हैं मुंह पर कपड़ा लपेटे। सड़कों पर भटक रहे हैं, पुलिस रोक रही है, मत जाओ, लेकिन कहां रहें ये तो वह भी नहीं बता सकती। केवल रास्ते खाली करवा सकती है। किसी की समझ ने यह काम किया कि गाड़ी जिस राह जाती है वही राह वे पैदल चलेंगें तो अपने घर पहुंच जायेंगे, चल दिये रेल लाईन पर पैदल। ज़िन्दगी और मौत के बीच एक रेल लाईन भी होती है, किसे पता था।
ये वे श्रमिक हैं जो वर्षों से अथवा जन्म से ही इस देश के लिए काम कर रहे हैं, छोटे-छोटे कार्यों से लेकर बड़े कामों तक। इनके काम का कोई नाम नहीं है, श्रम का कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है, किन्तु इनके श्रम के बिना देश की अर्थव्यवस्था भी नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था में इनका कितना प्रतिशत योगदान है कभी किसी अर्थशास्त्री ने गणना की, मुझे नहीं पता।
वे छात्र किस श्रेणी के थे जिन्हें ए सी बसों में भेजा गया, निश्चित रूप से किसी श्रमिक के बच्चे तो रहे नहीं होंगे, नहीं तो वे भी पैदल ही जाते रेल-लाईन पर।
हां, अब मुझे यह पता लगा कि हमारे देश में जन्म लेकर यहां से पढ़लिखकर लोग विदेश जा बसे, वहां अपने श्रम का योगदान देने लगे, उनकी अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने लगे। अपने देश का अमूल्य धन विदेशों में लगाने लगे। पता नहीं कितने वर्षोे से। किन्तु इस समय उन्हें अपने देश की याद आई और वे लौटना चाहते हैं।
उनके लिए विमान सजे, तीन-तारा और पंचतारा होटलों में उनके एकान्तवास की व्यवस्था हो रही है। सरकारी ए सी बसों से उन्हें पहुंचाया जा रहा है।
और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रेलवे लाईन पर सो रही है, पैदल चल रही है, एक सरकार कहती है जाना है तो जाओ, दूसरी कहती है मत आओ, तुम्हारे लिए हमारे पास जगह नहीं है।
आज हम अपने-आपको घर के भीतर राशन जमाकर सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। किन्तु कल क्या होगा, पता नहीं।
बात तो पुरानी हो गई किन्तु लिखने का मन आज बना तो क्या करेे, अब बासी रोटी ही सही, कुछ न कुछ पेट तो भरेगा ही।
कुछ चैनल चार-पांच लोगों को, जिन्हें वे बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी , धार्मिक नेता आदि-आदि कहते हैं, उनके बीच शब्द-युद्ध में मग्न समय काट रहे हैं। इस धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म की कितनी महत्ता है, यह टीवी पर प्रसारित होने वाले वाक्-युद्ध से हम समझ सकते हैं।
कहीं भी समाचारों से ज्ञात नहीं हो पा रहा कि लाखों की फ़ीस लेने वाले निजी अस्पताल इस विकराल समस्या में अपना क्या योगदान दे रहे हैं। ज़रूर दे रहे होंगे, किन्तु जानकारी नहीं मिली। समाचारों में एक भी बार नहीं सुना कि फौर्टीज़, मैक्स, एल-कैमिस्ट जैसे बड़े-बड़े निजी अस्पताल इस समय क्या कर रहे हैं। गली-गली में बैठे निजी चिकित्सालय खोले एक विज़िट के 500 से 1000 तक की फ़ीस लेने वाले चिकित्सक इस समय कहां हैं? उलझी पड़ी हूं मैं।
उधर सुनने में आया है कि पड़ोसी देश सीमा पर गोलीबारी कर रहा है और हमारे पांच सैनिक शहीद हुए हैं। उनकी शहादत की कथा हम पिछले कई दिन से टी. वी. पर देख रहे हैं। समाचार पत्रों में भी कई पृष्ठ उन्हें ही समर्पित हैं। किन्तु उससे ही अगले दिन बार्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स के तीन जवान शहीद हुए उनके बारे में बस इतना ही समाचार मिला। समाचार पत्र में भी एक ही पंक्ति। क्या कैटेगरी अलग होने से शहादत का भाव भी बदल जाता है?
आजकल हम बहुत धार्मिक हो रहे हैं। वैसे तो सदा से ही हैं किन्तु इधर परेशानी बढ़ गई है।
धार्मिक स्थल, मन्दिर तो नहीं खुले, मदिरालय खोल दिये गये।
कपाट खोलने ज़रूरी हो गये हैं। अब यह सरकार की मर्ज़ी कि कौन से कपाट खोले। कौन से कपाट खोलने पर सरकार की तिज़ोरी सीधे-सीधे भरेगी, यह सरकार ही समझती है, मेरी आपकी समझ ऐसी कहां।मदिरालय खोलने का निर्णय सरकार का गलत हो सकता है किन्तु मन्दिर खोलने से क्या हो जायेगा मैं यह नहीं समझ पा रही हूं, ऐसे विषयों पर मंद बुद्धि हूं।
क्या किसी ने मांग की थी कि मदिरालय खोले जायें? शायद नहीं ! सरकार की राजस्व की आवश्यकता थी। कोरोना के नाम पर अरबों-खरबों से सरकार की तिजोरी भरी, कितनी, नहीं पता।
किन्तु मदिरा आम आदमी की कितनी आवश्यकता है यह ठेकों के सामने लगी दो-दो किलोमीटर लम्बी लाईन से पता लगा। ओले-बारिश में भी लोग जमे रहे।
मदिरा ठेकों पर बोतलों में मिलती है, हर प्रकार की, जहां से खरीद कर आप उसे घर ले जा सकते हैं। ठेके रात 12 और 2 बजे तक खुले रहते हैं। साथ आहाते होते हैं जहां आप बैठकर पी भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। इसके बाद अनेक होटल, रैस्टोरैंट, पब में भी मिलती है, जिसे आपको वहीं खरीद कर, वहीं बैठकर पीना होता है, आप घर नहीं ला सकते, जहां उसका मूल्य कई गुणा बढ़़ जाता है। इसकी होम डिलीवरी भी नहीं है। किसी माॅल में, बिग बाज़ार में अथवा जनरल आपूर्ति की दुकानों पर भी नहीं मिलेगी। लेकिन क्यों, इसी बात को समझने का प्रयास कर रही थी।
मदिरालय के ठेके करोड़ों-करोड़ों में बिकते हैं, बोली लगती है।
यदि मदिरा एवं धूम्रपान सरकार की एवं आम आदमी की इतनी बड़ी आवश्यकता है तो खुले आम क्यों नहीं।
हमारे देश में मदिरा एवं धूम्रपान को लेकर एक अलग-सा दृष्टिकोण है। पीने वालों को बुरा समझा जाता है। मान लिया जाता है कि इनका चरित्र 50 प्रतिशत तो गिरा हुआ ही होगा, परिवार के प्रति आर्थिक अपराधी हैं, अथवा ये बहुत बड़े आदमी हैं। महिलाओं के लिए तो बात करना भी अपराध है। सरकार का कौन सा दृष्टिकोण है समझ से बाहर है। मतलब यह कि जिसने पीनी है, उसके लिए सरकार प्रबन्ध करके ही रहेगी, तो छिपना-छिपाना क्यों, खुलकर पिलाईये, बेचिए, बांटिए।
बस इतना है कि हमारे फ़ेसबुकीय कवियों को एक और नया विषय मिल चुका है] मन्दिर या मदिरालय] वाह ! बढ़िया तुकबन्दी बन गई।।
मैं भी प्रयासरत हूं इस विषय पर एक अच्छी कविता के लिए
निकम्मे कर्मचारी
एक छोटा-सी हास्य रचना
एक पुरानी और बड़ी आई. टी. कम्पनी। वे दोनों मित्र घर से दूर, एक इस एक अच्छी आई. टी. कम्पनी में कार्यरत । वैसे तो शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती थी, किन्तु नया-नया शौक, पैसे कमाने की ललक, और सोचते घर रहकर भी क्या करेंगे, चलो आफ़िस चलते हैं। पहली नौकरी थी । शौक भी था कि काम ज्यादा करेंगे तो आगे बढ़ेंगें। और यदि कोई कर्मचारी ज्.यादा काम करना चाहता है तो प्रबन्धक क्यों मना करेंगे। आईये, आपको कोई अतिरिक्त भत्ता तो देना नहीं था।
सो अब शनिवार और रविवार को प्रायः आफ़िस खुलता। पहले ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि कि छुट्टी के दिन कभी आफिस खुलता हो। फिर जब कर्मचारी आयेंगे, तो सहायक कर्मचारियों को भी आना पड़ता है, उन्हें चाहे ओवर-टाईम मिलता हो, किन्तु छुट्टी तो खराब हो जाती है।
नई भर्तियों के बाद अब कुछ ज्यादा ही होने लगा था।
एक दिन उनके बॉस ने उन दोनों नये कर्मचारियों को बुलाया और कहा कि तुम्हारे विरूद्ध शिकायत आई है कि तुम दोनों बहुत निकम्मे हो।
दोनों घबरा गये कि क्या हुआ।
बॉस ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने शिकायत की है कि कैसे निकम्मे नये कर्मचारी भर्ती किये हैं, कि छुट्टी के दिन भी काम करने आना पड़ता है।
बैठे ठाले
चित्राधारित रचना हास्य
*********-**********
मैं जिस डाल पर बैठा हूं, उसे ही काट रहा हूं, आपको कोई आपत्ति, कोई कष्ट आपको? नहीं न, तो काटने दीजिए, गिरूंगा तो मैं गिरूंगा, हड्डियां टूटेंगी तो मेरी टूटेंगी, आपको क्या? क्यों अपनी टांग अड़ाते हैं आप किसी और के मामले में। बता दूं कि दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने पर भी टांग टूट जाती है।
हा हा! आजकल आरी से पेड़ कौन काटता है भला। आजकल तो मशीने हैं, पलभर में पूरा वृक्ष धराशायी। मैं जानता हूं कि आप क्या कहेंगे। आप कहेंगे कि यह तो मूर्खता प्रदर्शित करने का प्रतीक है कि जिस डाली पर बैठे उसी को काटना। मुहावरा है। किन्तु मूर्खता प्रदर्शित करने की आवश्यकता ही क्या ? प्रदर्शित करना है तो बुद्धिमानी कीजिए, चतुराई कीजिए, दक्षता कीजिए। किसी की भी मूर्खता तो उसके मुंह खोलते ही पता लग जाती है।
और हर समय गम्भीर बात करना ज़रूरी होता है क्या? जानता हूं मैं कि वृक्ष पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं। हमने विकास की आंधी में बहुत कुछ खो दिया है। आधुनिकता के पीछे भाग कर हम अपनी बहुत हानि कर रहे हैं। पर सूखा वृक्ष है तो काटेंगे ही, लकड़ी काम आयेगी और नये वृक्ष लगायेंगे किन्तु आपने तो पता नहीं कितनी कहानियां बना डालीं कि जिस डाल पर बैठा है, उसे ही काट रहा है।
मैं तो आप सबकी कल्पनाशक्ति देख रहा था कि मेरे इस चित्र को देखकर आप क्या सोचते हैं। आप ही इस चित्र को ध्यान से देखकर बताईये ज़रा, मैं इस वृक्ष पर चढ़ा कैसे? न डाली, न सहारा, न सीढ़ी। और लक्कड़हारे की तो मेरी यूनिफ़ार्म भी नहीं है। तो फिर ! प्रतीकात्मक है, मूर्खता प्रदर्शित करने का।
करिये योग भगाये रोग
कैसी विडम्बना एवं आश्चर्य की बात है कि जिस योग पद्धति का उल्लेख हमारे प्राचीनतम ग्रंथों ऋग्वेद एवं कठोपनिषद ग्रंथों में मिलता है, जो ईसा पूर्व के ग्रंथ हैं, उस प्राचीनतम योग पद्धति को हम आज प्रदर्शन के रूप में योगा डे के रूप में मना रहे हैं। पतंजलि का योगसूत्र योग का सबसे महत्वपूर्ण गं्रथ है। अन्य अनेक ग्रंथों में भी योग की परिभाषाएँ महत्व एवं क्रियाएँ उल्लिखित हैं। योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, अपितु एक मानसिक, चिकित्सीय पद्धति भी है।
वर्तमान में हम इस बात से ज़्यादा प्रसन्न नहीं हैं कि एक हमारी प्राचीनतम योग पद्धति जो लुप्त हो रही थी, पुनः प्रकाश में आई है, हमारे जीवन का हिस्सा बनने लगी है, उसके गुणों को हम अपने जीवन में उतारने में लगे हैं बल्कि हम इस बात की ज़्यादा खुशियाँ मनाने में लगे हैं कि देखिए हमारा योगा अब विश्व में मनाया जाने लगा है। हमारे योगा का अब अन्तर्राष्ट्रीय दिवस है।
यदि सत्य को समझने का साहस रखते हों तो आज भी योग हमारे दैनिक जीवन का, नित्यप्रति का हिस्सा नहीं बन सका है। चाहे विद्यालयों में यह एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा है किन्तु बच्चे भी इसे एक विषय के रूप में ही लेते हैं न कि दैनिक जीवन की एक अपरिहार्य क्रिया के रूप में, जीवन-शैली के रूप में अथवा चिकित्सा-पद्धति के रूप में। बड़े-बुजुर्ग पार्क में एकत्र होकर अनुलोम-विलोम आदि करते दिखाई दे जायेंगे अथवा एक-दो और क्रियाएँ , और हमारा योगा डे सम्पन्न हो जाता है।
21 जून को सड़कों पर छपी टी-शर्ट पहने, बढ़िया-सी चटाई बिछाये और बाद में कुछ खान-पानी ही योगा-डे की उपलब्धि बनकर रह जाते हैं।
हमारे प्राचीन ग्रंथों में योग का जो महत्व दर्शाया गया है एवं क्रियाएँ बताईं गईं हैं हम उनसे अभी भी बहुत-बहुत दूर हैं। आवश्यकता है प्रत्येक स्तर पर प्रयास की, अभ्यास की, सम्मान की और इसे अपने दैनिन्दन जीवन का हिस्सा बनाने की। योग को उचित रूप में जीवन का हिस्सा बनाने से निश्चित रूप से आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न मानसिक, शारीरिक एवं अने मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान हो पायेगा।
शिक्षक दिवस : एक संस्मरण
वर्ष 1959 से लेकर 1983 तक मैं किसी न किसी रूप में विद्यार्थी रही। विविध अनुभव रहे। किन्तु पता नहीं क्यों सुनहरी स्मृतियाँ नहीं हैं मेरे पास।
मुझे बचपन से ही मंच पर चढ़कर बोलना, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना बहुत अच्छा लगता था। मेरा उच्चारण एवं स्मरण-शक्ति भी अच्छी थी। सब पसन्द भी करते थे किन्तु सदैव किसी न किसी कारण से मेरा नाम प्रतियोगिताओं से कट जाता था और मैं रोकर रह जाती थी। अध्यापक कहते सबसे अच्छा इसने ही बोला किन्तु बाहर भेजते समय किसी और का नाम चला जाता और मैं मायूस होकर रह जाती।
जब कालेज पहुंची तो मैंने सोचा अब तो भेद-भाव नहीं होगा और यहां मेरी योग्यता को वास्तव में ही देखा जायेगा। किन्तु वहां तो पहले से ही एक टीम चली आ रही थी और हर जगह उसका ही चयन होता था । यहां भी वही हाल।
तभी कालेज में हिन्दी साहित्य परिषद का गठन हुआ और मैं उसकी सदस्य बन गई। कहा गया कि आप यहां कविता-कहानी आदि कुछ भी सुना सकते हैं। मेरे घर में तो पुस्तकों का भण्डार था। एक पुस्तक से मैंने निम्न पंक्तियाँ सुनाईं 1972 की बात कर रही हूं
हर आंख यहां तो बहुत रोती है
हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है
देख के रो दे जो ज़माने का गम
उस आंख से जो आंसू झरे मोती है
****-*****
सबने समझा यह मेरी अपनी लिखी है और मुझे बहुत सराहना मिली। तब मुझे लगा कि मैं अपनी पहचान कविताएं लिख कर ही क्यों न बनाउं। किन्तु समझ नहीं थी।
फिर उसके कुछ ही दिन बाद कालेज में ही वाद-विवाद प्रतियोगिता थी, संचालक ने मेरा नाम ही नहीं पुकारा। बाद में मैंने पूछा कि सूची में मेरा भी नाम था तो बोले कि मेरा ध्यान नहीं गया।
मैं आहत हुई और मैंने सोचा अब मैं कविताएं लिखूंगी जो यहां कोई नहीं लिखता और अपनी अलग पहचान बनाउंगी। उस दिन मैंने इसी भूलने के विषय पर अपनी पहली मुक्त-छन्द कविता लिखी ।
चाहे इसे शिक्षकों द्वारा किये जाने वाला भेद-भाव कहें अथवा उनकी भूल, किन्तु मेरे लिए लेखन का नवीन संसार उन्मुक्त हुआ जहां मैं आज तक हूं।
बड़ी याद आती है शिमला तुम्हांरी
एक संस्मरण
*-*-*-*-*-*-*
आज जाने कौन-सी स्मृतियों में खींच कर ले गया मुझे मेरा मन। । शिमला का माल-रोड, वहां खड़ी फ़ायर ब्रिगेड की गाड़ी, बर्फ से ढके दूर-दूर तक फैले चीड़-देवदार के वृक्ष। अनायास बिछी एक सफ़ेद चादर। कभी रूईं के फ़ाहों सी, कभी श्वेत रजत-सी, जैसे कहीं दूर से दौड़ती आती और सब कुछ ढककर चली जाती। धरा से आकाश तक। एक स्वर्गिक अनुभव जिसकी अभिव्यक्ति के लिए शब्द नहीं होते।
शिमला में बर्फ़ क्या पड़ी] न जाने कौन-सी स्मृतियों में खींच कर ले गई मुझे। हरीतिमा को अद्भुत सौन्दर्य प्रदान करती एक श्वेत आभा।
शीत ऋतु से लड़ाई के लिए सब तैय्यार रहते थे।नवम्बर आरम्भ होते ही सर्दी की तैयारियां शुरू हो जाती थीं। चार-पांच महीने का राशन, कोयला-लकड़ी भरवानी है, अंगीठियां तैयार रहें, रजाईयां और रजाईयां ही रजाईयां। परिवार में जितने सदस्य उतनी गर्म पानी की बोतलें, वह भी गिलाफ़ चढ़ाकर, कोट, मोटे स्वेटर, छाते, बरसाती यानी रेनकोट, टोपी, मफलर, स्कार्फ, दस्ताने, गर्म जुराबें, गमबूट और न जाने क्या क्या।
प्रायः दिसम्बर में बर्फ पड़ जाती थी किन्तु कभी किसी ने छुट्टी लेने का सोचा ही नहीं। तीन-तीन चार-चार फुट बर्फ में भी सभी प्रायः चार-पांच किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल, कालेज, कार्यालयों में पहुंचा करते थे। हर दफ्तर में स्टीम कोयले की अंगीठियां जला करती थीं जिन्हे महाम कहा जाता था। बाद में हीटर भी मिलने लगे। घरों में भी ऐसी ही अंगीठियां जलाते थे जिन पर साथ ही पानी भी गर्म हो सके। और पानी ! न जी न! पानी कहां। शून्य से नीचे के तापमान में पानी नलों में जम जाता था। पानी की पाईप फ़ट जाती थीं। पानी भरकर रखना पड़ता था और बर्तनों में भरकर रखे पानी में भी स्लेट जम जाती थी। सबसे आनन्द की बात तो यह होती थी कि न पानी आयेगा, न गर्म होगा न नहाना पड़ेगा।
25 दिसम्बर से 28 फरवरी तक सर्दी की छुट्टियां। दिन-रात अंगीठियां जली रहतीं। सारा दिन या तो अंगीठियों को घेरकर कम्बल-रजाईयां लपेटे बैठे रहते, खूब खाते। दिन भर में 12-15 चाय तो आम बात होती और वह भी आज के शब्दों में लार्ज। और बस मूंगफली। अथवा बिस्तरों में ही दुबके बैठे । आज सोचती हूं तो देखती हूं 8 सदस्यों के परिवार में 12-15 चाय अर्थात दिन-भर में 100 से अधिक चाय। काश! तब ठीक से सोचा होता तो परिवार से कोई तो प्रधानमंत्री बन सकता था। तभी तो दादी मां से कहती थी ‘’लाड़ी, पाणिये दी टांकिया बिच ही चीनी-पत्ती पाई देया कर, सारा दिन चाई दा डबरू इ चढ़ी रहंदा।‘’ (बहू, पानी की टांकी में ही चीनी-पत्ती डाल दिया कर, सारा दिन चाय का पतीला चढ़ा रहता है।) और बस मूंगफली और गुड़-शक्कर।
बर्फ को गिरते देखना, महसूस करना, हर बार एक नया आनन्द और अनुभव होता। बर्फ को हाथों से छूते, गोले बनाते, बर्फ के बुत बनाते, खाते और घर के अन्दर लाकर बर्तनों में भी रख देते। आश्चर्य होता था कि कैसे एक-एक पत्ती, कण-कण ढक जाता, एक कोमल श्वेत आभा से। टेढ़ी टीन की छतों पर से बर्फ धीरे-धीरे फ़िसलती, मानों कोई शरारत कर रहा हो। और हम नीचे खड़े प्रतीक्षा करते कि अब गिरी और तब गिरी। कभी धीरे-धीरे तो कभी धड़ाम से धमाका करती गिरती। ऐसे पलों की मानों हम प्रतीक्षा करते थे। जब बर्फ पिघलती, तो छत से टपकती बूंदों का स्वर आनन्दिन करता। तापमान शून्य से नीचे रहने पर छतों से टपकती बूंदे हवा में ही जमने लगतीं, और छतों से लटकती, लम्बी-लम्बी, मोटी पारदर्शी नलियाँ सुन्दर आकार ले लेंतीं, जिन्हें हम नलपियां कहते थे। उनका सौन्दर्य अद्भुत होता था। जब सूरज चमकता तो उनके भीतर से रंग-बिरंगी धाराएं दिखतीं। उन्हें तोड़-तोड़कर खाने का आनन्द लेते। वे इतनी सख्त और नुकीलीं होती थीं कि किसी को चुभ जाये अथवा मारी जाये तो गहरी चोट लग सकती थी।
और बर्फ में बनी कुल्फी ! जब रात को मौसम साफ होता था तो लोटे में चीनी मिश्रित गर्म दूध ढककर बर्फ में दबा देते थे और उसके चारों ओर नमक डाला जाता था। वाह ! क्या आनन्द था उस स्वाद का।
जब बर्फ गिरने लगती तो बाहर बरामदे में आकर बैठ जाते। मां चिल्लाती रह जाती, पर कौन सुनता। हाथों से छूते, गोले बनाते, बर्फ के बुत बनाते, खाते और घर के अन्दर लाकर बर्तनों में भी रख देते।
आज जब सब याद करती हूं तो देखती हूं कि कितनी भी समस्याएं होती थीं कभी समस्या लगी ही नहीं। बिजली नहीं, पानी नहीं, आवागमन का कोई साधन नहीं, किन्तु कभी इस बारे में सोचते ही नहीं थे, बस आनन्द ही लेते थे। कैसा भी मौसम हो शाम को माल-रोड के तीन चक्कर तो लगाने ही हैं स्कैंडल-प्वाईंट से लेडीज़ पार्क तक। और हाथ में बालज़ीस की आईसक्रीम-कोण।
बड़ी याद आती है शिमला तुम्हारी ।।।
इस ऋतु के लिए तैय्यारियां तो पूरा वर्ष ही चली रहती थीं। स्वेटर, गर्म जुराबें ,दस्ताने , मफ़लर तो घर पर ही बुने जाते थे। शिमला की महिलाएं इस बात के लिए बहुत प्रसिद्ध रही हैं कि उनके हाथ में सदैव उन-सिलाईयां रहती थीं।
प्रायः दिसम्बर में बर्फ पड़ जाती थी किन्तु कभी किसी ने छुट्टी लेने का सोचा ही नहीं। और वैसे कभी छुट्टी लें भी लें, किन्तु बर्फ में तो जाना ही है। और यदि छुट्टी है तो पहली बर्फ़ का आनन्द लेने तो माल-रोड जाना ही होगा। तीन-तीन चार-चार फुट बर्फ में भी सभी प्रायः चार-पांच यहां तक कि आठ-दस किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल, कालेज, कार्यालयों में पहुंचा करते थे और वह भी समय से। उस समय वाहन की सुविधाएं न के बराबर थीं। हम शिमला में लोअर कैथू रहते थे, स्कूल था छोटा-शिमला में ,लगभग पांच किलोमीटर। पांच वर्ष से 17 वर्ष तक हज़ारों किलोमीटर सफ़र तो इसी रूट पर तय कर लिया होगा आज सोचती हूं। बाद में कालेज, विश्वविद्यालय, बैंक। चढ़ाई-उतराई कुछ न महसूस होती। प्रतिदिन इतनी लम्बी यात्रा का भरपूर आनन्द उठाते थे। बर्फ गिरने के बाद जब दिन भर धूप रहती अथवा बादल, तो बर्फ़ पिघलने लगती। और यदि रात को मौसम साफ़ हो तो सड़कों पर पानी की अदृश्य स्लेटें जम जातीं। खूब फ़िसलन होती, लोगों को गिरते देखने में बड़ा आनन्द आता था।
आज जब सब याद करती हूं तो देखती हूं कि कितनी भी समस्याएं होती थीं कभी समस्या लगी ही नहीं। बिजली नहीं, पानी नहीं, आवागमन का कोई साधन नहीं, किन्तु कभी इस बारे में सोचते ही नहीं थे, बस आनन्द ही लेते थे। कैसा भी मौसम हो शाम को माल-रोड के तीन चक्कर तो लगाने ही हैं स्कैंडल-प्वाईंट से लेडीज पार्क तक। और आकाश से गिरती बर्फ़ और हाथ में बालजीस की आईसक्रीम-कोण।
बड़ी याद आती है शिमला तुम्हांरी ।।।
चेतना का जागरण
जब मैं अपना शोध कार्य कर रही थी तब मैंने पढ़ा था कि एक सामाजिक चेतना हुआ करती है जो कालिक होती है। जैसे हिन्दी साहित्य के मध्यकाल में भक्ति भाव की चेतना थी। कवि, चित्रकार, गायक, संगीतकार, शिल्पी सब भक्ति-भाव में डूबे थे। उसके बाद चेतना में परिवर्तन आया और रीति काल का आगमन हुआ। इस काल में सब श्रृंगारिक भाव में डूब गये, यह एक कालिक चेतना हुआ करती थी, जिस कारण सबके मन में एक से ही भाव उमड़ते थे, और समान भाव पर सृजन होता था। यही छायावादी काल, प्रगतिवाद और कुछ और वादों के काल में भी हुआ। यह मैं नहीं कह रही, मैंने कहीं पढ़ा था इस सामाजिक चेतना के बारे में।
आप कहेंगे, आज क्यों याद आ गई मुझे इस चेतना की।
अब मुझे क्यों याद आई इस चेतना की , बताने के लिए ही तो यह लिखना शुरू किया है, यह तो मात्र भूमिका था, आपको उलझाने के लिए।
तो ऐसा है कि पहले यह चेतना शताब्दियों की होती थी। शायद 250-300 वर्षों की। जैसे भक्ति काल और रीति काल। फिर अवधि घटने लगी। दशकों तक आ गई, जैसे भारतेन्दु युग, छायावादी काल, प्रगतिवाद, नई कविता आदि। मेरा ज्ञान थोड़ा कच्चा और जिसे Time out कहते हैं, यदि आपको लगे तो सम्हाल लीजिएगा।
फिर दशक छूटे, साल रह गये। और वर्तमान में यह चेतना दैनिक हो गई है।
मुझे इतना ज्ञान कैसे मिला, यहीं फ़ेसबुक से मित्रो, आपकी जिज्ञासा शांत करती हूं। यह मेरा शोध कार्य है।
वर्तमान में चेतनाओं का रूप बहुत विस्तृत हो गया है।
पिछले वर्ष से कोरोना की चेतना गतिमान है। इस बीच मदिरा की चेतना आई थी और फिर श्रमिकों की। वास्तविक श्रमिक चेतना एक मई को आती है। अनेक बार मातृ चेतना होती है। आजकल सरकारी तौर पर बेटी चेतना का बहुत विस्तार हुआ है।
वर्तमान में चेतनाएं दैनिक अधिक होने लगी हैं, जो कभी-कभी एक-दो दिन तक विस्तारित हो जाती हैं। 14 फ़रवरी को प्रेम के देवता की दैनिक चेतना होती है। ऐसे ही 8 मार्च को महिलाओं की दैनिक चेतना होती है, किसी दिन बेटी की। वर्ष में एक दिन योग की भी चेतना होती है । वर्ष में तीन-चार अलग-अलग दिनों में राष्ट्र प्रेम की चेतना होती है। देवियों की चेतना वर्ष में दो बार नौ-नौ दिन की होती है। पूरे वर्ष में 25-30 या इससे भी ज़्यादा देवी देवताओं की चेतना दैनिक होती है। कुछ चेतनाएं घटनावश सृजित होती हैं। जैसे किसी आतंकवादी घटना के घटने पर, प्राकृतिक प्रकोप पर, मानवीय दुर्घटना आदि पर।
इन सबके अतिरिक्त राजनीतिक चेतना, व्यापारिक चेतना, धार्मिक चेतना, नकल चेतना, रिश्वत चेतना आदि का भी विस्तार है, जिन पर अभी मैं शोध कार्य कर रही हूं।
इनके अतिरिक्त राजनीतिक चेतना, व्यापारिक चेतना, धार्मिक चेतना, नकल चेतना, रिश्वत चेतना आदि चेतनाएँ भी अत्यन्त महत्वपूर्ण चेतनाएँ हैं जिन पर भविष्य में अवश्य एक नवीन चेतना के साथ चिन्तन होगा।बेटा पूछता है, पुत्र दिवस की चेतना कब होती है मां। किसी को पता हो तो बताईएगा।
मैं भी आजकल प्रतिदिन योगासन कर रही हूं नवीन चेतनाओं के जागरण के लिए।
परिधान
हमारे समाज में महिलाओं के परिधान की अनेक तरह से बहुत चर्चा होती है। वय-अनुसार, पारिवारिक पोस्ट के अनुसार, अर्थात अविवाहित युवती, भाभी, ननद, बहन, माँ, दादी आदि के लिए। इसके अतिरिक्त भारत में रीति-परम्पराओं, राज्यानुसार प्रचलित, एवं धार्मिक आख्यानों में भी इतनी विविधता है कि उसके अनुसार भी महिलाओं के वस्त्रों पर दृष्टि रहती है।
और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे आधुनिक समाज में महिलाओं के परिधानों के अनुसार ही उनका चरित्र-चित्रण किया जाता है। आधुनिक वस्त्र धारण करने वाली युवती के लिए मान लिया जाता है कि यह बहुत तेज़ होगी, घर-गृहस्थी के योग्य नहीं होगी, पति, सास-ससुर की सेवा करने वाली नहीं होगी। ( किन्तु जब महिलाओं की बात होती है तब सेवा-भाव वाली बात आती ही क्यों है, उसके अपने अस्तित्व की बात क्यों नहीं की जाती। परिवार के सदस्य की बात क्यों नहीं आती?, पुरुषों के सन्दर्भ में तो इस तरह की बात कभी नहीं आती। इस विषय पर चर्चा को विराम देती हूँ, यह भिन्न चर्चा का विषय है।)
किन्तु पुरुषों के परिधान, वस्त्रों पर कभी कोई बात नहीं करता।
क्योंकि महिलाएं खुलेआम टिप्पणी नहीं कर पातीं इस कारण कहती नहीं।
सबसे बुरा लगता है जब पुरुष केवल अन्तर्वस्त्रों में अथवा तौलिए में प्रातःकाल बरामदे में घूमते दिखते हैं। गर्मियों में तो जैसे उनका अधिकार होता है अर्द्धनग्न रहना। मुझे नहीं पता कि उनके घर की महिलाएं उन्हें टोकती हैं अथवा नहीं।
मैं शिमला से हूँ। वहां हमने सदैव ही यही देखा है कि पुरुष भी महिलाओं की भांति स्नानागार से पूरे वस्त्रों में ही तैयार होकर निकलते हैं। किन्तु जब मंै यहां आई तो मुझे बहुत शर्म आती थी कि घर के बच्चे क्या, युवा, अधेड़, बुजुर्ग सब आधे-अधूरे कपड़ों में घूमते हैं। हमें यह अश्लील लगता है। अभिनेत्रियों के वस्त्रों पर भी बहुत कुछ लिखा जाता है किन्तु जब बड़े.बड़े मंचों पर बड़े नामी कलाकार नग्न प्रदर्शन करते हैं तब वह भव्यता होती है। इन नग्नता की तुलना हम किसी कार्य या खेल में पहने जाने वस्त्रों से नहीं कर सकते।
पुरुष की वस्त्रहीनता उसका सौन्दर्य है और स्त्री के देह-प्रदर्शनीय वस्त्र अश्लीलता।
सबसे बड़ी बात जो मुझे अचम्भित भी करती है और हमारे समाज की मानसिकता को भी प्रदर्शित करती है वह यह कि हमारे प्रायः सभी प्राचीन पात्रों के चित्रों में उपरि वस्त्र धारण नहीं दिखाये जाते। फिर वह चित्रकारी हो अथवा अभिनय। किसने देखा है वह काल कि ये लोग उपरि वस्त्र पहनते थे अथवा नहीं। क्यों यह अश्लीलता नहीं दिखती और कभी भी क्यों इस पर आपत्ति नहीं होती। निश्चित रूप से उस युग को तो किसी ने नहीं देखा, यह हमारी ही मानसिकता का प्रतिफल है। किसने देखा है कि देवता, भगवान क्या पहनते थे। यह उस कलाकार की अथवा भक्त की मानसिकता है जो अपने आराध्य की सुन्दर, सुघड़ देहयष्टि दिखाना चाहता है।
महिलाएं पुरुषों के पहनावे से आहत होती हैं। प्रकृति ने पुरुष को छूट दी है, यह हमारी सोच है। मुझे आश्चर्य तब होता है जब हम महिलाएं भी उसी बनी.बनाई लीक पर चलती हैं।
एक अन्य तथ्य यह कि जब भी भारतीय संस्कृति, परम्पराओं, रीति-रिवाज़ों के अनुसार पहनावे की बात उठती है तब केवल महिलाओं के सन्दर्भ में ही चर्चा होती है, पुरुषों के पहरावे पर कोई बात नहीं की जाती।
इतना और कहना चाहूंगी कि कमी मर्दों की मानसिकता में नहीं महिलाओं की मानसिकता में है जो पुरुष नग्नता का विरोध नहीं करतीं।
मूर्तियों की आराधना
चित्राधारित रचना
जब मैं अपना शोध कार्य रही थी तब मैंने मूर्तिकला एवं वास्तुकला पर भी कुछ पुस्तकें पढ़ी थीं।
मैंने अपने अध्ययन से यह जाना कि प्रत्येक मूर्ति एवं वास्तु के निर्माण की एक विधि होती है। किसी भी मूर्ति को यूँ ही सजावट के तौर पर कहीं भी बैठकर नहीं बनाया जा सकता यदि उसका निर्माण पूजा-विधि के लिए किया जा रहा है। स्थान, व्यक्ति, निर्माण-सामग्री, निर्माण विधि सब नियम-बद्ध होते हैं। जो व्यक्ति मूर्ति का निर्माण करता है वह अनेक नियमों का पालन करता है, शाकाहारी एवं बहुत बार उपवास पर भी रहता है जब तक उसका कार्य पूरा नहीं हो जाता।
हमारे धर्म में अनेक देवी-देवताओं की पूजा होती है उनमें गणेश जी भी एक हैं। प्राचीन काल में प्रत्येक देवी-देवता की सम्पूर्ण पूजा विधि का पालन किया जाता था और उसी के अनुसार मूर्ति-निर्माण एवं स्थापना का कार्य।
आज हमारी पूजा-अर्चना व्यापारिक हो गई है। यह सिद्ध है कि प्रत्येक देवी-देवता की पूजा-विधि, मूर्ति-निर्माण विधि, पूजन-सामग्री एवं पूजा-स्थल में उनकी स्थापना विधि अलग-अलग है। किन्तु आज इस पर कोई विचार ही नहीं करता। एक ही धर्म-स्थल पर एक ही कमरे में सारे देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की जाती है, जबकि प्राचीन काल में ऐसा नहीं था।
सबसे बड़ी बात यह कि हम यह मानते हैं कि हमारा स्थान ईश्वर के चरणों में है न कि ईश्वर हमारे चरणों में।
हम निरन्तर यह तो देख रहे हैं कि कौन किसे खींच रहा है, कौन देख रहा है किन्तु यह नहीं देख पा रहे कि गणेश जी की मूर्ति को पैरों में रखकर ले जाया जा रहा है, कैसे होगी फिर उनकी पूजा-आराधना?
पर उपदेश कुशल बहुतेरे
यह मुहावरा सुना तो बहुत बार था किन्तु कभी इसकी गुणवत्ता की ओर ध्यान ही नहीं गया। धन्यवाद इस मंच का जिसने इस मुहावरे की महत्ता एवं विशेषताओं पर चिन्तन करने का अवसर प्रदान किया।
पर उपदेश कुशल बहुतेरे!!
वाह!!
इसका अर्थ यह है कि जो कुशल होगा वही तो पर को अर्थात अन्य को बहुत सारे उपदेश दे सकेगा। जो कुशल ही नहीं है वह किसी को क्या उपदेश देगा और क्या मार्ग-दर्शन करेगा।
हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं हमारी जवाबदेही तय होती है। घर-परिवार में, समाज में, नौकरी में, कार्यालय में, व्यवसाय में, सड़क पर चलते हुए, हर जगह, हर जगह। हानि-लाभ, अच्छा-बुरा, खरा-खोटा, उत्तर-प्रति-उत्तर, लिखित, मौखिक। हम बच नहीं पाते।
किन्तु उपदेश देने में किसी उत्तरदायित्व का वहन नहीं होता। आप उपदेश दीजिए, चाय-नाश्ता लीजिए और निकल लीजिए। किन्तु ध्यान रहे कि न तो अपने घर बुलाकर उपदेश दीजिए और न किसी उपवन-बात में। जिसे उपदेश देना हो सीधे उसके घर जाकर ही स्थापित रहिए। उपदेशात्मक संस्था खोल लीजिए, दान-दक्षिणा लीजिए, दिल खोलकर परामर्श दीजिए।
किन्तु बस पहले से ही बचने का उपाय बांधकर चलिए।
कुछ ऐसे ‘‘ देखिए मैं तो अपने मन से एक अच्छा परामर्श आपको दे रहा हूँ /दे रही हूँ, यह तो आप पर और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि फ़लित हो। और आपकी मनोभावनाओं का भी इस पर प्रभाव रहेगा। बस कोई कमी नहीं रहनी चाहिए हमारे बताये उपाय में। ’’
और जब आपका बताया परामर्श फ़लित न हो तो आपके पास पहले से ही तैयार उत्तर होगा कि ‘‘देखिए मैंने तो पहले ही कहा था कि मन से कीजिएगा, अथवा आपने कोई न कोई विधि तो छोड़ दी होगी। ’’
और साथ ही कुछ अगली सलाहें परोस दीजिए।। और आप जब अपना समय दे रहे हैं, दिमाग़ दे रहे हैं तो कुछ न कुछ मूल्य तो लेंगे ही, चाहे अच्छा चाय-पानी ही।
किन्तु यह उपदेश मैं आप सब मित्रों को दे रही हूँ, मेरे अपने लिए नहीं है।
अपनेपन की दुविधा
हमारे भारतीय परिवारों में दो ऐसे समय होते हैं जब निकट-दूर के सब अपरिचित-परिचित अगली-पिछली भूलकर एक साथ होते हैं अथवा कहें कि दिखाई देते हैं। एक
विवाह-समारोहों में और दूसरा किसी के निधन पर। विवाह-समारोह तो केवल दो-तीन दिन के ही होते हैं, और इस अवसर वे ही लोग होते हैं, जिन्हें सही से निमन्त्रित किया गया हो।
किन्तु किसी के निधन पर तो 16-17 दिन ऐसे लोगों के बीच बीतते हैं, जिनमें से कुछ बहुत अपने होते हैं। कुछ कभी-कभार चिट्ठी-पत्री जैसे, जिनका नाम देखकर हम बन्द लिफ़ाफा रख देते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। कुछ समाचार पत्र की सूचनाओं जैसे, कुछ दीपावली, जन्मदिवस, नये वर्ष पर शुभकामनाओं जैसे, और कुछ ऐसे जिन्हें हम बरसों-बरस नहीं मिले होते, और कुछ ऐसे जो न जाने कहां-कहां से अलमारी की पुरानी पुस्तकों से निकलकर सामने आ खड़े होते हैं । ऐसी पुस्तकें जिन्हें हम न तो रद्दी में बेच पाते हैं और न सहेज पाते हैं, इसलिए अलमारी के किसी कोने में पीछे-से रख देते हैं। और ऐसी ही दो-चार अधूरी पढ़ी, छूटी पुस्तकों के माध्यम से हम जीवन के सारे अध्याय पुन: पढ़ डालते हैं न चाहते हुए भी।
जीवन में कौन साथ है और कौन नहीं, हम कभी जान ही नहीं पाते और हमें ही कोई कितना जान पाया है, ऐसे ही समय ज्ञात होता है। बस हवाओं में जीते हैं, हवाओं से लड़ते हैं, और उन्हें ही ओढ़-बिछाकर सो जाते हैं।
निजी एवं सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर
मेरे विचार में यदि केवल एक नियम बना दिया जाये कि सभी सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के बच्चे उनके अपने ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे तो इन विद्यालयों के अध्यापक स्वयं ही शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास करेंगे।
निजी विद्यालयों एवं सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में अन्तर के मुख्य कारण मेरे विचारानुसार ये हैं:
निजी विद्यालयों में स्थानान्तरण नहीं होते, अवकाश भी कम होते हैं तथा जवाबदेही सीधे सीधे एवं तात्कालिक होती है।
निजी विद्यालयों में प्रवेश ही चुन चुन कर अच्छे विद्यार्थियों को दिया जाता है चाहे वह प्रथम कक्षा ही क्यों न हो।
कमज़ोर विद्यार्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।
- भारी भरकम वेतन पर अध्यापकों की नियुक्ति, मिड डे मील,यूनीफार्म आदि बेसिक सुविधाओं से शिक्षा का स्तर नहीं उठाया जा सकता। बदलती सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा के बदलते मानदण्डों , शिक्षा की नवीन पद्धति, समयानुकूल पाठ्यक्रमों में परिवर्तन की ओर जब तक ध्यान नहीं दिया जायेगा सरकारी विद्यालयों की शिक्षा पिछड़ी ही रहेगी।
, यदि हम यह मानते हैं कि निजी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है तो यह हमारी भूल है। वर्तमान में निजी विद्यालयों में भी शिक्षा नाममात्र रह गई है। क्योंकि यहां उच्च वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं तो वे ट्यूशन पर ही निर्भर होते हैं। निजी विद्यालयों में तो नाम, प्रचार, अंग्रेज़ी एवं अन्य गतिविधियों की ओर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है।
सबसे बड़ी बात यह कि हम निजी विद्यालयों की शिक्षा पद्धति एवं शिक्षा नीति को बहुत अच्छा समझने लग गये हैं । किन्तु वास्तव में यहाँ प्रदर्शन अधिक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि निजी विद्यालयों की तुलना में सरकारी विद्यालय पिछड़े हुए दिखाई देते हैं किन्तु इसका कारण केवल सरकारी अव्यवस्था, अध्यापकों पर शिक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिए किसी भी प्रकार के दबाव का न होना एवं निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों का ही इन विद्यालयों में प्रवेश लेना, जिनकी पढ़ाई में अधिक रुचि ही नहीं होती।
मेरे विचार में कमी व्यवस्था में है। सरकार विद्यालय दूर दराज के क्षेत्रों में भी हैं जहां कोई भी जाना नहीं चाहता।
भ्रष्टाचार पर चर्चा
जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं और दूसरे की ओर अंगुली उठाते हैं तो चार अंगुलियाँ स्वयंमेव ही अपनी ओर उठती हैं जिन्हें हम स्वयं ही नहीं देखते। यह पुरानी कहावत है।
वास्तव में हम सब भ्रष्टाचारी हैं। बात बस इतनी है कि जिसकी जितनी औकात है उतना वह भ्रष्टाचार कर लेता है। किसी की औकात 100 रुपये की है तो किसी की 100 करोड़ की। किन्तु 100 रुपये वाला स्वयं को ईमानदार कहता है। हम मंहगाई की बात करते हैं किन्तु सुविधाभेागी हो गये हैं। बिना कष्ट उठाये धन से हर कार्य करवा लेना चाहते हैं। हमें दूसरे का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार लगता है और अपना आवश्यकता, विवशता।
यदि हम अपनी ओर उठने वाली चार अंगुलियों के प्रश्न और उत्तर दे सकें तो शायद हम भ्रष्टाचार के विरूद्ध अपना योगदान दे सकते हैं:
पहली अंगुली मुझसे पूछती है: क्या मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ ।
दूसरी अंगुली कहती है: अगर मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं तो क्या भ्रष्टाचार का विरोध करती हूँ ?
तीसरी अंगुली कहती है: कि अगर मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं किन्तु भ्रष्टाचार का विरोध नहीं करती तो मैं उनसे भी बड़े भ्रष्टाचारी हूँ ।
और अंत में चौथी अंगुली कहती है: अगर मैं भी भ्रष्टाचारी हूं तो सामने की अंगुली को भी अपनी ओर मोड़ लेना चाहिए और मुक्का बनाकर अपने पर वार करना चाहिए। दूसरों को दोष देने और सुधारने से पहले पहला कदम अपने प्रति उठाना होगा।
नज़रिया बदलें, नज़ारे बदलेंगे
किसी मित्र ने मुझसे कहा कि आपकी सोच यानी मेरी यानी कविता की सोच बहुत नकारात्मक है। यदि मैं अच्छा सोचूँगी, सकारात्मक रहूँगी तो सब अच्छा ही होगा। इस बात पर उन्होंने एक मुहावरा पढ़ डाला ‘‘नज़रिया बदलें, नज़ारे बदलेंगे’’ किन्तु कैसे उन्होने नहीं बताया।
तो इस मुहावरे पर मेरा एक सरल सा हास्य-व्यंग्य
*-*-*-*-*-*-*
आप अवश्य ही सोचेंगे इसकी तो बुद्धि ही उलट-पुलट है। किन्तु जैसी है, वैसी ही है, मैं क्या कर सकती हूँ। आप सब हर विषय पर गम्भीरता का ताना-बाना क्यों ओढ़ लेते हैं?
अब आप कह रहे हैं, नज़रिया बदलें, नज़ारे बदलेंगे। कैसे भई, किस तरह?
अब इस आयु में मैं तो बदलने से रही। कोई भी योगी-महायोगी कहेगा, बदलने, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बस प्रयास करना पड़ता है। अब सारा जीवन प्रयास करते ही निकल गया, कभी किसी के लिए बदले, तो कभी किसी के लिए। बचपन में माँ-पिता, बड़े भाई-बहनों के आदेश-निर्देश बदलने के लिए, फिर ससुराल पक्ष के, उपरान्त बच्चों के और अब आप शुरु हो गये। अब तो थोड़ा मनमर्ज़ी से आराम करने दीजिए।
चलिए, कुछ गम्भीर बात कर लेते हैं। क्या मात्र नज़रिया बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं? पता नहीं, चलिए विचार करने का प्रयास करते हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि नज़ारे बदलें तो नज़रिया अवश्य बदलता है।
मन उदास है और बाहर खिली-खिली धूप है, गुंजन करते भंवरे, हवाओं से लहलहाते पुष्प, पंछियों की चहक, दूर तक फैली हरियाली, देखिए कैसे नज़रिया बदलता है। आप ही चेहरे पर मुस्कुराहट खिल आती है, मन आनन्दमय होने लगता है और चाय पीने का मन हो आता है जिसे हम गुस्से में अन्दर छोड़ आये थे।
कोई यदि हमारे सामने अपशब्दों का प्रयोग करता है तो हम नज़रिया कैसे बदल लें? किन्तु मन खिन्न होने पर हमें कोई सान्त्वना के दो मधुर शब्द बोल देता है, हमारे हित में बात करता है, तो नज़रिया बदल जाता है।
*
किन्तु मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बु़िद्ध उलट-पुलट है। अब आपके पक्ष से विचार करते हैं। नज़रिया बदलें, नज़ारे बदलेंगे।
मैंने नज़रिया बदल लिया।
करेला कड़वा नहीं है, नीम मीठी है। मिर्च तीखी नहीं है, कौआ कितना मीठा गाता है, गोभी का फूल कितना सुन्दर है किसी को भेंट करने के लिए।
हमने करेले-नीम की सब्जी बनाई और यह कहकर सबको खिलाई कि मेरे सकारात्मक विचारों से बनी देखिए कितनी मीठी सब्ज़ी है।
अब यह नज़रिया बदलने पर हमारे क्या नज़ारे बदले न ही पूछिए, क्योंकि हम जानते हैं आप अत्यधिक सकारात्मक विचारों के हैं हमारा दर्द क्या समझेंगे।
एक किस्सागोई
कुछ बातें बेवजह याद आती हैं लेकिन निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पातीं।
वैसे तो 22 मार्च 2020 से ही घर पर हूं, जब पहला लॉक डाउन हुआ था किन्तु आधिकारिक तौर पर 20 जुलाई 2020 को त्यागपत्र देकर घर ही हूं।
तो कल तक जब यानी 20 जुलाई 2020 से पूर्व कोई मुझे पूछता था कि आप क्या करती हैं तो मैं पहले कहा करती थी, बैंक में कार्यरत हूं, उपरान्त मैं इस विद्यालय में वरिष्ठ लेखाकार हूं।
21 जुलाई 2020 से मेरी पोस्ट बदल गई। अब मेरी पोस्ट क्या है, यही विचार करने के लिए यह आलेख लिख रही हूं।
बात यह कि कुछ वर्ष पहले तक जो महिला नौकरी नहीं करती थी, उसे घरेलू महिला हाउस वाईफ़ कहा जाता था, और इसे बड़े सामान्य तौर पर लिया जाता था, चाहे वह महिला कितनी ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न हो। और नौकरी न करना कोई अपराध अथवा हीन भावना भी नहीं होती थी।
वर्तमान में स्थिति बदल चुकी है।
विद्यालय में बच्चों के प्रवेश फ़ार्म में माता-पिता के विवरण के विस्तृत काॅलम होते हैं, जिनमें उनकी शिक्षा, नौकरी, कार्यक्षेत्र, कार्यस्थल, वेतन, अन्य अनुभवों आदि की जानकारी मांगी जाती है।
इसी काॅलम से मेरा यह आलेख निकला। मैंने देखा कि कुछ फ़ार्मों में माता के विवरण में जाॅब/बिजनैस के आगे लिखा मिलने लगा: हाउस मेकर, हाउस मैनेजर, हाउस इंचार्ज। किन्तु विभाग के आगे कोई सूचना नहीं लिखी गई थी। मैं महामूर्ख। मुझे लगा सम्भवतः किसी हास्पिटैलिटीए होटल आदि में कोई पोस्ट होगी।
मैं एक महिला से पूछ बैठी मैम आपने डिपार्टमैंट नहीं लिखा। डिपार्टमैंट मतलब? मैंने लिखा तो है हाउस मैनेजर। जी हां, पोस्ट तो लिखी है, डिपार्टमैंट, आफिॅस का पता भी तो लिखिए।
उसे बड़ा अपमानजनक लगा मेरा प्रश्न। क्रोध से बोली, आप कहना क्या चाहती हैं कि जो लेडीज जाॅब नहीं करतीं, वो केवल घरेलू, अनपढ़, गंवार, निकम्मी होती हैं क्या? मैं हाउस मेकर, हाउस मैनेजर हूं, घर हम औरतें ही बनाती हैं।
मैं एकदम हकबका-सी गई, तो क्या ये पोस्ट हो गई। तो फिरघर में पति की क्या पोस्ट है, पूछ नहीं पाई।
मैं अचानक ही बोल बैठी, तो आप हाउस-वाईफ़ हैं। आपने पोस्ट के सामने हाउस मैनेजर लिखा है न, मुझे लगा किसी विभाग में पोस्ट का नाम होगा। साॅरी अगर आपको बुरा लगा।
अब नाराज़गी चरम पर थी। बोली, हाउस वाईफ़ का क्या मतलब होता है? मैं कोई अनपढ़, गंवार औरत हूं कि बस एक घरेलू औरत हूं। घर हम औरतें ही चलाती हैं। क्या वह काम नहीं है? क्या आपकी तरह बाहर नौकरी न करने वाली औरतें क्या बस घरेलू ही हैं। क्या आप ही काम करती हैं जो घर से बाहर नौकरी करती हैं। हम घर चलाती हैं, घर सम्हालती हैं तो हाउस मैनेजर, हाउस मेकर हुई या नहीं। हमारे बिना घर चल सकता है क्या? हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं है क्या? घर तो हम औरतें ही बनाती हैं न।
मैं भी सिरे की ढीठ। उल्टी खोपड़ी। पीछे हटने वाली कहां। मैंने आगे से कहा, मैम वो तो सारी ही महिलाएं करती हैं, हम नौकरी वाली भी करती हैं तो क्या मुझे अपनी पोस्ट के साथ ओब्लीग करके हाउस मेकर भी लिखना चाहिए। और घर सम्हालना कोई नौकरी तो नहीं हुई न। यहां काॅलम जाॅब/बिज़नेस है।
वह महिला देर तक बड़बड़ाती रही। और उसने वर्तमान में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय, विरोध, शोषण, उनके अधिकारों के हनन, सम्मान की कमी, पारिवारिक समस्याओं और न जाने कितने विषयों पर भाषण दे डाला।
मैं समझ नहीं पाई कि घर से बाहर नौकरी न करना हीन भावना क्यों बनने लगा है और घर में रहना एक जाॅब या नौकरी कैसे बना। निःसदेह महिलाओं के साथ अनेक क्षेत्रों में अन्याय, विरोधाभास है किन्तु इन बातों के अत्यधिक प्रचार-प्रसार ने महिलाओं की सोच को भी प्रभावित कर दिया है। इसका दुष्परिणाम यह कि महिलाओं की परिवार के प्रति सोच संकुचित होने लगी है और वे उन क्षेत्रों में भी अधिकारों की बातें करने लगी हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र की नहीं हैं। मुझे लगता है महिलाओं में इस तरह की सोच, प्रवृत्ति, उन्हें आत्मनिर्भर, स्वाबलम्बी, स्वतन्त्र नहीं बना रही, पुरुष समाज के विरुद्ध अकारण खड़ा कर रही है। उनमें पारिवारिक दायित्वों के प्रति एक विमुखता ला रही है। अपने पारिवारिक दायित्वों को एक जाॅब या नौकरी समझने से सोच बहुत बदली है और महिलाओं की मानसिकता में गहरी नकारात्मकता आने लगी है।
आत्म संतोष क्या जीवन की उपलब्धि है 2
पिछले कुछ समय से मैं एक गम्भीर प्रश्न का उत्तर ढूंढ रही हूं। प्रश्न आर्थिक/वित्तीय है। अपने इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए मैं शहर के विभिन्न बैंकों में गई, वित्तीय संस्थानों में पूछताछ की। स्टॉक एक्सचेंज की खाक छानी, विदेशी मुद्रा विनिमय केन्द्रों में गई, बड़े-बड़े वित्तीय अधिकारियों से मिली, किन्तु मेेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ।
अब मैं अपना प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जब बड़ी-बड़ी संस्थाएँ और बड़े-बडे़ लोग मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाये तो मैं अपने वयोवृद्ध दादाजी के पास जा बैठी। मुझे रुंआसी देखकर दादाजी ने कारण पूछा। डूबते को क्या चाहिए एक तिनके का सहारा। मैंने अपना प्रश्न दादाजी के मामन रख दिया। दादाजी, लोग रुपये की बात करते हैं डॅालर, पौंड, यूरो और न जाने कितना विदेशी मुद्राओं की बात करते हैं किन्तु मैंने एक नये धन का नाम सुना है जिसे सन्तोष धन कहा जाता है। यह धन तो मैंने किसी के पास नहीं देख।
जिससे पूछती हूं वही मेरा उपहास करता हे कि अरे इस पगली लड़की को देखो, भला आज के ज़माने में भी कहीं संतोष धन पाया जाता है। दादाजी कोई नहीं मानता कि संतोष भी कोई धन होता है। अब आप ही बताईये दादाजी , यह संतोष धन कौन-सा धन है कहां मिलता है, कहां पाया जाता है , कौन प्रयोग करता है । किस काम आता है। यह कैसा गुप्त धन है जिसके बारे में बड़े-बड़े लोग नहीं जानते।
दादाजी मेरी बात सुनकर ठठाकर हंस दिये। बोले बेटी, संतोष धन तो मनुष्य ने सदियों पहले ही खो दिया। और तुम पुरातात्विक विभाग की वस्तु को आधुनिक विज्ञान की मशीनों में खोजोगी तो भला बताओ कैसे मिलेगी? अब आधुनिकता की दौेड़ में जुटे लोगों की रुचि भला पंद्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी की वस्तुओं में कैसे हो सकती है।
लेकिन वे चकित भी थे कि मुझे इस संतोष धन का पता कैसे लगा। क्या मैंने इस धन को पा लिया है। मैं हंस दी नहीं दादाजी मुझे यह धन नहीं मिला। मैंने उन्हें बताया कि कोई कबीरदास हुआ करते थे वे लिख गये हैं जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अब दादाजी से तो बहुत बातें हूईं किन्तु उनसे वार्तालाप में मेरे सामने अनेक प्रश्न उठ खड़े हुए। उन्हीं पर चिन्तन करते हुए मैं आपके समक्ष हूं।
क्या सत्य में ही आधुनिकता के पीछे भाग रहे मनुष्य ने संतोष धन खो दिया है। कबीरदास ने कहा कि जिस मनुष्य के पास संतोष धन है उसके सामने सब धन धूल के समान हैं अर्थात उनका कोई महत्व नहीं।
किन्तु वर्तमान में इस दोहे के अर्थ बदल गये हैं। वर्तमान में इस दोहे का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास संतोष धन है उसके लिए सब धन धूल के समान हो जातेे हैं अर्थात उसे जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाती।
तो क्या जीवन में सचमुच संतोष ही सबसे बड़ी उपलब्धि है? मेरी दृष्टि में नहीं। मेरी दृष्टि में संतोष का अभिप्राय है एक ठहराव, निप्क्रियता, इच्छाओं का दमन। यदि मानव ने अपनी स्थितियों पर संतोेष कर लिया होता तो वह आज भी वन में पत्थर रगड़ कर आग जला रहा होता, पत्तों के वस्त्र धारण कर वृक्षों पर सो रहा होता। मेरी दृप्टि में संतोष न करने का अभिप्राय है, आगे बढ़ने की इच्छा, प्रगति की कामना, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, नव-नवोन्मेष प्रतिभा एवं विचारो का स्तवन, अनुसंधान, स्वाबलम्बन, अच्छे से अच्छा करने की कामना।
संतोष न करने का ही परिणाम हे कि आज हम चांद पर पहुंच गये हैं, समुद्र की अतल गहराईयों को नाप रहे हैं। लाखों मीलों की दूरी कुछ ही घंटों में तय कर लेते हैं।
विश्व के एक कोने में बैठकर सम्पूर्ण विश्व के लोगों से वार्तालाप कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं।
यदि मैं संतोष धन अपना लूं तो कभी भी अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास ही न करुं। उत्तीर्ण होकर भी क्या करता है, संतोष धन तो पा ही लिया है। माता-पिता से कहूँगी मैंने संतोष धन प्राप्त कर लिया है मुझे आगे मत पढ़ाईये।
मेरे कुछ साथी संतोष-असंतोष की तुलता कर सकते हैं कि संतोष न होने का अर्थ है असंतोष। किन्तु मेरी दृष्टि में असंतोष एक मानसिक वेदना है जो ईर्ष्या-द्वेष-भाव से उपजती है जबकि संतोष न करने की भावना प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है।
खामोशियां भी बोलती है
नई बात। अब कहते हैं मौन रहकर अपनी बात कहना सीखिए, खामोशियाँ भी बोलती हैं। यह भी भला कोई बात हुई। ईश्वर ने गज़ भर की जिह्वा दी किसलिए है, बोलने के लिए ही न, शब्दाभिव्यक्ति के लिए ही तो। आपने तो कह दिया कि खामोशियाँ बोलती हैं, मैंने तो सदैव धोखा ही खाया यह सोचकर कि मेरी खामोशियाँ समझी जायेगी। न जी न, सरासर झूठ, धोखा, छल, फ़रेब और सारे पर्यायवाची शब्द आप अपने आप देख लीजिएगा व्याकरण में।
मैंने तो खामोशियों को कभी बोलते नहीं सुना। हाँ, हम संकेत का प्रयास करते हैं अपनी खामोशी से। चेहरे के हाव-भाव से स्वीकृति-अस्वीकृति, मुस्कान से सहमति-असहमति, सिर से सहमति-असहमति। लेकिन बहुत बार सामने वाला जानबूझकर उपेक्षा कर जाता है क्योंकि उसे हमें महत्व देना ही नहीं है। वह तो कह जाता है तुम बोली नहीं तो मैंने समझा तुम्हारी मना है।
कहते हैं प्यार-व्यार में बड़ी खामोशियाँ होती हैं। यह भी सरासर झूठ है। इतने प्यार-भरे गाने हैं तो क्या वे सब झूठे हैं? जो आनन्द अच्छे, सुन्दर, मन से जुड़े शब्दों से बात करने में आता है वह चुप्पी में कहाँ, और यदि किसी ने आपकी चुप्पी न समझी तो गये काम से। अपना ऐसा कोई इरादा नहीं है।
मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए। खामोशी की भाषा अभिव्यक्ति करने वाले से अधिक समझने वाले पर निर्भर करती है। शायद स्पष्ट ही कहना पड़ेगा, गोलमाल अथवा शब्दों की खामोशी से काम नहीं चलने वाला।
मेरा अभिप्राय यह कि जिस व्यक्ति के साथ हम खामोशी की भाषा में अथवा खामोश अभिव्यक्ति में अपनी बात कहना चाह रहे हैं, वह कितना समझदार है, वह खामोशी की कितनी भाषा जानता है, उसकी कौन-सी डिग्री ली है इस खामोशी की भाषा समझने में। बस यहीं हम लोग मात खा जाते हैं।
इस भीड़ में, इस शोर में, जो जितना ऊँचा बोलता है, जितना चिल्लाता है उसकी आवाज़ उतनी ही सुनी जाती है, वही सफ़ल होता है। चुप रहने वाले को गूँगा, अज्ञानी, मूर्ख समझा जाता है।
ध्यान रहे, मैं खामोशी की भाषा न बोलना जानती हूँ और न समझती हूँ, मुझे अपने शब्दों पर, अपनी अभिव्यक्ति पर, अपने भावों पर पूरा विश्वास है और ईश प्रदत्त गज़-भर की जिह्वा पर भी।
मोबाईल: आवश्यकता अथवा व्यसन
हमारी एक प्रवृत्ति हो गई है कि हम बहुत जल्दी किसी भी बात की आलोचना अथवा सराहना करने लगते हैं। कोई एक करता है और फिर सब करने लगते हैं जैसे मानों नम्बर बनाने हों कि किसने कितनी आलोचना कर ली अथवा सराहना कर ली। जैसे हमारी विचार-शक्ति समाप्त हो जाती है और हम निर्भाव बहती धारा के साथ बहने लगते हैं।
मोबाईल!!!
आधुनिकता के इस युग में मोबाईल जीवन की आवश्यकता बन चुका है। चाहे कितनी भी आलोचना कर लें किन्तु वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में इसके महत्व और आवश्यकता को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि आपको मोबाईल किस स्तर का चाहिए और किस कार्य के लिए।
एक समय था जब विद्यालयों में मोबाईल ले जाना प्रतिबन्धित था। फिर समय ऐसा आया कि यही मोबाईल शिक्षा का केन्द्र बन गया। कोराना काल ने आम आदमी के जीवन में इतने परिवर्तन कर दिये कि एक बार तो वह स्वयं ही समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। जब तक समझ आती, जीवन की धाराएँ ही बदल चुकीं थीं।
शिक्षा का यह ऐसा काल था, लगभग दो वर्ष का, जिसने शिक्षा, ज्ञान और परीक्षाओं के सारे प्रतिमान ही बदल कर रख दिये। शिक्षा की इस नवीन प्रणाली ने पारिवारिक व्यवस्थाएँ, आवश्यकताएँ, जीवन का ढाँचा ही बदल कर रख दिया। देश के मध्यमवर्गीय परिवारों में रोटी से अधिक महत्वपूर्ण मोबाईल हो उठे। फिर वह पहली कक्षा का विद्यार्थी हो अथवा किसी बड़ी कक्षा का। किसी-किसी परिवार में एक साथ दो-दो लैपटॉप और तीन-चार मोबाईल की आवश्यकता उठ खड़ी हुई अर्थात लाखों का व्यय। आय बन्द, व्यवसाय बन्द, वेतन आधा और मोबाईल ज़रूरी। ऐसे कितने ही परिवार मैंने इस समय में देखे जहाँ माता-पिता के पास एक-एक मोबाईल था और पिता के पास लैपटॉप। अब तीन बच्चे। तीनों की एक समय ऑनलाईन क्लास। माता अध्यापिका। अब एक लैपटॉप और तीन मोबाईल की अनिवार्यता उठ खड़ी हुई। चाहिए भी एंड्राएड अर्थात कम से कम 15-20 हज़ार प्रति। जहाँ मोबाईल पढ़ाई की आवश्यकता बने वहाँ आदत का हिस्सा भी। असीमित ज्ञान का भण्डार। आय-व्यय, बैंकिंग, भुगतान-प्राप्ति का सरल साधन, डिजिटल पेमंट, खेल का माध्यम। बच्चे घर में बैठकर पूरी दुनिया से जुड़ रहे थे, ज्ञान का असीमित भण्डार का पिटारा मानों उनके सामने खुल गया था और वे अचम्भित थे। माता-पिता से जल्दी बच्चे यह सब सीखने लगे। इसमें कहीं भी कुछ भी ग़लत अथवा ठीक नहीं कहा जा सकता था, यह सब समय की आवश्यकता के कारण विकसित हो रहा था, जो धीरे-धीरे हमारे स्वभाव का हिस्सा बनता गया। यदि शिक्षा के क्षेत्र में यह मोबाईल न होता तो बच्चे दो वर्ष पीछे चले जाते और उन्होंने ऑन लाईन जो ज्ञान प्राप्त किया, आधुनिकता से जुड़े, वह एक बहुत बड़ा अभाव रह जाता।
आज का समय ऐसा नहीं है कि बच्चे विद्यालय से निकले और घर। नहीं जी, ट्यूशन, डांस क्लास, स्विमिंग, क्रिकेट और न जाने क्या-क्या। तब माता-पिता और बच्चों के बीच यही एक वार्तालाप का सहारा बनता है
ऐसा नहीं कि कोरोना काल में ही मोबाईल ने हमारे जीवन को प्रभावित किया। इससे पूर्व भी विद्यालयों में सीनियर कक्षाओं में प्रोजेक्ट वर्क, आर्ट वर्क और अनेक गृह कार्य ऐसे दिये जाते थे जो गूगल देवता की सहायता से ही किये जाते थे। कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड और अनेक तकनीक प्रयोग में पहले से ही चल रहे थे, बस मोबाईल की इसमें वृद्धि हुई।
किसी सीमा तक यह बात ठीक है कि जब किसी वस्तु का हम अत्याधिक प्रयोग करने लगत हैं तब आवश्यकता से बढ़कर वह हमारी आदत बन जाती है, हमें उसकी लत लग जाती है और जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ने लगता है।
निश्चित रूप से बच्चे आज पक्षियों की भांति स्वतन्त्र पंछी नहीं रह गये हैं। इसका एक कारण मोबाईल हो सकता है किन्तु सारा दोष केवल मोबाईल को नहीं दिया जा सकता। आधुनिकतम जीवन शैली, शिक्षा एवं ज्ञान का माध्यम, बच्चे तो क्या हमारी पीढ़ी भी इसमें उलझी बैठी है। अब यह माता-पिता का कर्तव्य है और शिक्षा-संस्थानों का भी कि बच्चों को मोबाईल के उचित प्रयोग एवं सीमित प्रयोग के लिए प्रेरित करें न कि उन्हें आरोपित।
विश्व चाय दिवस
सुबह से भूली-भटकी अभी मंच पर आगमन हुआ तो ज्ञात हुआ कि आज तो अन्तर्राष्ट्रीय चाय दिवस अथवा विश्व चाय दिवस है।
ऐसा कैसे सम्भव है। चाय का और केवल एक दिवस! नहीं, नहीं, यह तो चाय का और चाय के नशेड़ियों का घोर अपमान है।
शिमला में हम परिवार में आठ सदस्य थे, दिन-भर में 80-90 चाय तो बनती ही होगी और वह भी लार्ज पटियाला साईज़, पीतल के बड़े गिलास। मेरी दादी मेरी माँ से कहती थी पानी की टंकी में ही चीनी-पत्ती डाल दे, अपने-आप सब दिन-भर पीते रहेंगे।
दिन भर में पाँच-छः चाय तो अब भी पी ही लेती हूँ। कुछ वर्ष पहले तक दस-बारह हो ही जाती थी। उससे पहले 12-15। गज़ब की पाचन-क्षमता रही है मेरी। प्रातः घर से 7.30 निकल जाती थी किन्तु आम बात थी कि चार से पांच चाय पी लेती थी। काम करते-करते एक कप खाली हुआ, दूसरा तैयार। एक नाश्ते के साथ और दूसरा नाश्ते के बाद। फिर कार्यालय पहुँचकर टेबल पर सबसे पहले चाय। चाय देने वाले को भी पता था कि मैडम को कितनी चाय चाहिए होती है। वैसे भी छोटे-छोटे गिलास में आती चाय वैसे ही मूड खराब कर देती है इस कारण मुझे हर जगह अपना ही कप या गिलास रखना पड़ता था। जब मेरा स्थानान्तरण हुआ तो मज़ाक किया जाता था कि कंटीन तो अब बन्द हो जायेगी, कविता तो जा रही है।
मेरे लिए चाय का अर्थ है शुद्ध चाय। अर्थात पानी, ठीक-सा दूध, चीनी और पत्ती। कुछ लोग चाय के नाम पर काढ़ा पीना पसन्द करते हैं। हाय! अदरक नहीं डाला, छोटी इलायची के बिना तो स्वाद ही नहीं आता, दालचीनी वाली चाय बड़ी स्वाद होती है। दूध वाली गाढ़ी चाय होनी चाहिए। अरे तो दूध ही पी लीजिए, चाय के बहाने दूध क्यों पी रहे हैं, सीधे-सीधे कहिए कि दूध पीना है। कुछ लोग चाय का मसाला बनाकर रखते हैं। अरे ! ऐसी ही चाय पीनी है तो गर्म मसाला ही पी लीजिए, चाय को क्यों बदनाम कर रहे हैं।
लोग कहते हैं चाय से गैस हो जाती है, नींद नहीं आती है अथवा नींद आ जाती है। पता नहीं कैसे हैं यह लोग।
आह! किसी समय, कितनी बार, कहीं भी, बस चाय, चाय और चाय।
जीवन और परिवर्तन
परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, जिस पर मनुष्य का नियन्त्रण नहीं। मानव कितना ही शक्तिशाली हो जाये, प्रकृति में नित्य प्रति आने वाले परिवर्तन पर नियन्त्रण नहीं कर सकता। शीत को ग्रीष्म में और ग्रीष्म को शिशिर में नहीं बदल सकता।
वास्तव में परिवर्तन विकास, चेतना, चिन्तन का प्रतीक है। परिवर्तन हमारी इच्छाओं, कामनाओं, लालसाओं का दूसरा नाम है। जिस दिन परिवर्तन रुक जायेगा, उस दिन मानवता भी ठहर जायेगी। हम कह सकते हैं कि परिवर्तन विकास का ही दूसरा नाम है।
एक परिवर्तन सहज-स्वाभाविक है और दूसरा परिवर्तन सप्रयास। परिवर्तन प्रायः आवश्यकता आधारित होता है और अब आवश्यकताएँ लगभग पूर्ण होने लगती हैं तब लालसा एवं प्रदर्शन के कारण भी हम जीवन में परिवर्तन करने लगते हैं।
मनुष्य की चेतना उसकी सर्वोत्तम उपलब्धि तथा अन्य सभी गुणों का आधार है। यह व्यक्ति मानस की प्रमुख विषेशता होने के साथ.साथ निरन्तर परिवर्तनशील हैए अतः विकासोन्मुख हैए स्थिर या जड़ नहीं। यही उसे पाशव स्तर से उठाकर मानव स्तर तक ले आती है।
इसी कारण सृष्टि के आरम्भ होते ही परिवर्तन, विकास और चिन्तन की प्रक्रिया आरम्भ हुई, इसी कारण आज मानव आधुनिकता के इस द्वार पर खड़ा है। जंगल में रहते हुए मानव ने अपने हित में, अपनी सुरक्षा और जीवन-यापन के लिए प्रकृति के साथ मिलकर परिवर्तन की प्रक्रिया आरम्भ की होगी। गुफ़ाओं को घर बनाया होगा, उन्हें सुरक्षित किया होगा, जीवन-यापन के लिए, भोज्य सामग्री की तलाश की होगी। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सुरक्षा साधनों का विकास किया होगा। परिवर्तन और विकास की यह प्रक्रिया इतनी लम्बी रही होगी कि हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। एकल मानव संगठित हुआ, समूह बने होंगें, और अन्ततः परिवर्तन और विकास की आँधी ने उसे आज आधुनिकता के चरम तक पहुँचा दिया है।
जीवन के इस परिवर्तन को यदि हम सहज-स्वाभाविक रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। क्योंकि जब भौतिक परिवर्तन होता है तब विचारों, भावों, रीति-परम्पराओं, रहन-सहन, शिक्षा, संस्कारों, व्यवहार, सामाजिकता, पारिवारिक संगठन, परिवेश, वेश-भूषा सबमें परिवर्तन अवश्यम् भावी है। भौतिक परिवर्तन एवं विकास के साथ बहुत कुछ पुराना छूटना स्वाभाविक है और नये को स्वीकार करना जीवनगत आवश्यकता।
इस वास्तविकता को, इस परिवर्तन को, हम जितनी सहजता से स्वीकार कर लें, जीवन की प्रक्रिया भी उतनी ही सरल-सहज होने लगती है।
किन्तु समस्या यह कि हम भौतिक परिवर्तन को तो स्वीकार कर रहे हैं किन्तु कहीं-कहीं पुरातनता का लबादा ओढ़ने में, प्रदर्शन करने में हमें आनन्द मिलता है। हम भौतिक परिवर्तन एवं वैचारिक परिवर्तन में तालमेल नहीं बिठाना चाहते।
हमारे आधुनिक समाज की यही समस्या है कि हम आधुनिक तो होना चाहते हैं, सब सुविधाएँ भी चाहिए किन्तु न जाने कहाँ-कहाँ पुरातनता ढूँढते हैं और अपने सुखमय वर्तमान को कोसते रहते हैं। आवश्यकता है, भौतिक परिर्वतन अर्थात भौतिक विकास एवं वैचारिक परिवर्तन अर्थात विचारधारा में एक परिपक्व समझ की।
परिवर्तन सकारात्मक भी होते हैं और विरोधाभासी भी। नकारात्मक परिवर्तन हमारे विचारों में होते हैं जिस कारण अनेक बार विकासात्मक परिवर्तन बाधित होता है।
वर्तमान में परिवर्तन में जिस विषय पर सर्वाधिक चर्चा की जाती है वह है हमारे विचारों, भावों, संस्कारों, रीति-रिवाज़ों, व्यवहार आदि में परिवर्तन की। निःसंदेह हमारी प्राचीन संस्कृति, रीति, परम्पराएँ, व्रतोपवास, पूजा-विधि, उपचार-पद्धति आदि उत्कृष्ट रहे हैं किन्तु वर्तमान जीवन पद्धति में प्राचीन काल की भाँति इनका अनुपालन सम्भव ही नहीं है। विशेषकर नई पीढ़ी आधुनिकता की सीढ़ियाँ चढ़ती प्राचीनता के प्रति आग्रही नहीं हो पा रही है। हम बच्चों को प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिकतम् सुविधाएँ प्रदान करना चाहते हैं, विलासितापूर्ण जीवन देना चाहते हैं, जीवन की प्रत्येक सुख-सुविधा प्रदान करना चाहते हैं फिर वह शिक्षा हो, रहन-सहन हो, पहनावा हो अथवा अन्य कोई भी सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक अथवा भौतिक आवश्यकता। किन्तु हम इस बात पर कदापि विचार नहीं करते कि जब भौतिक सुख-साधन बदलते हैं तब मानसिक विचारधाराएँ स्वयंमेव ही बदल जाती हैं। इस परिवर्तन में कुछ भी ठीक अथवा गलत नहीं होता, यह स्वाभाविक होता है। परिवर्तन के इस दोहरे रूप को समझना और स्वीकार करना ही जीवन की सफ़लता है।
आत्म संतोष क्या जीवन की उपलब्धि है
प्रायः कहा जाता है कि जीवन में आत्म-संतोष ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही परम संतोष है।
किन्तु आत्म संतोष क्या है?
क्या अपनी इच्छाओं, अभिलाषाओं का दमन आत्म-संतोष का मार्ग है?
वास्तविक धरातल पर जीवन जीना जितना कठिन और कटु है उपदेश देना और सुनाना उतना ही सरल।
पर उपदेश कुशल बहुतेरे।
वर्तमान उलझनों भरे जीवन, भागम-भाग की जीवन शैली, प्रतियोगिताओं, एक-दूसरे से आगे निकल जाने की दौड़, प्रतिदिन कुछ नया पाने की चाहत, पुरातनता और नवीनता के बीच उलझते, परम्पराओं, संस्कृति और आधुनिकतम जीवन शैली; तब आत्म संतोष कहाँ और परम संतोष कहाँ! हम अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं को किसी सीमा में नहीं बांध सकते, क्योंकि हमारी इच्छाएँ और सीमाएँ केवल हमारी नहीं होती, हमारे परिवेश से जुड़ी होती हैं।
आत्म संतोष की सीमा क्या है, कौन सा द्वार है जहाँ पहुँच कर हम यह समझ लें कि अब बस। जीवन की समस्त उपलब्धियाँ प्राप्त कर ली हमने। अब परम धाम चलते हैं। क्या ऐसा सम्भव है?
जी नहीं, बनी-बनाई उपदेशात्मक सूक्तियाँ सुना देना, कुछ आप्त वाक्य बोल देना, ग्रंथों से सूक्तियाँ उद्धृत करना और यह कहना कि हममें आत्म संतोष होना चाहिए और वह ही परम संतोष है, किसी के भी जीवन का सबसे बड़ा झूठ और छल है।
हम यह नहीं कह सकते कि आत्म-संतोष मिल गया और हम परम संतोष की अवस्था में पहुँच गये।
मेरे विचार में आत्म संतोष क्षणिक है, सीमित है, इसका विस्तार जीवनगत नहीं है। जैसे हम कहते हैं आज मेरे बच्चे को मेरा बनाया भोजन बहुत पसन्द आया, मुझे आत्म संतोष मिला। अथवा आज मैंने किसी की सहायता की, मन आत्म-संतोष से भर गया, और मैं परम संतोष की अवस्था में पहुँच गई। अथवा मेरे व्यवहार से वे प्रसन्न हुए, मुझे आत्म-संतोष मिला अथवा परम संतोष मिला।
संतोष की अन्तिम स्थिति हमारे जीवन में सम्भव ही नहीं क्योंकि हम सामाजिक, पारिवारिक प्राणी हैं और आत्म संतोष एवं परम संतोष के लिए प्रतिदिन हम प्रयासरत रहते हैं।
सामाजिक जीवन में, समाज में रहते हुए, अपनी इच्छाओं का दमन करना आत्म संतोष नहीं है, आत्म-संतोष है जीवन में उपलब्धि, लक्ष्य की प्राप्ति, सफ़लता। जीवन में आत्म संतोष किसी एक कार्य से नहीं मिलता, प्रति दिन और बार-बार किये जाने वाले कार्यों से मिलता रहता है, यह एक आजीवन प्रक्रिया है।
अतः आत्म संतोष अथवा परम संतोष जीवन की चरम प्राप्ति अथवा उपलब्धि नहीं है, हमारे कार्यों, व्यवहार से उपजा भाव है जिसकी प्राप्ति के लिए हम हर समय प्रयासरत रहते हैं।
बुद्धम् शरणम गच्छामि
कथाओं के अनुसार आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व की कथा है। 563 ईसा पूर्व। एक राजकुमार अपनी सोती हुई पत्नी एवं नवजाव शिशु को आधी रात में त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए चला गया। उस युवक ने घोर तपस्या की, साधना की और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने सम्पूर्ण जगत को जरा, मरण, दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए, सत्य एवं दिव्य ज्ञान की खोज के लिए जगत के हित के लिए वर्षों कठोर साधना की और अन्त में बिहार बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई ओर वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गये।
जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अपने परिवार का परित्याग किया, जो कि उनका दायित्व था क्या उस ज्ञान का उपयोग आज यह संसार कर रहा है? क्या जगत के लिए उनका ज्ञान और उपदेश चरम उपलब्धि था?
यदि था तो उनके उपरान्त क्यों आवश्यकता पड़ी कि एक-अनेक युग-पुरुष आये जिन्होंने संसार को पुनः उपदेश दिये, अपने ज्ञान की धारा बहाई, ग्रंथ लिखे गये, आप्त वाक्य बने और यह क्रम आज भी चल रहा है। एक समय बाद ज्ञान की धारा धर्म का रूप ले लेती है। उपदेश की पुनरावृत्ति होती है हर युग में, केवल नाम बदलते हैं, स्थापनाएँ नहीं बदलतीं।
जब भी गौतम बुद्ध के त्याग, ज्ञान, बौद्धित्व, साधना की बात की जाती है मुझे केवल नवजात शिशु और यशोधरा की याद आती है, उनके प्रति कर्तव्य, विश्वास की डोर टूटी तो सम्पूर्ण जगत के साथ कैसे जोड़ी?
धर्मगुरुओं के अधार्मिक आचरण
हमारे देश में धर्मगुरुओं की बहुत बात होती है और अनगिनत धर्मगुरु हमारे चारों ओर छाये हुए हैं।
किन्तु ये धर्मगुरु कौन हैं? हम किसे धर्मगुरु कह सकते हैं? वे कौन से धर्म के ज्ञाता हैं? किस धर्म की व्याख्या वे करते हैं, कौन से धर्म की चर्चा कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ पाता। कौन से ग्रंथों का वाचन करते हैं अथवा कौन सी परम्पराओं, आचरण, व्यवहार, संस्कृति का विश्लेषण करते हैं सम्भवतः वे स्वयं ही नहीं जानते। उनके भाषण सुनने पर कई बार ऐसा प्रतीत होता है मानों वे पांचवी कक्षा की नैतिक शिक्षा की पुस्तक से पाठ सुना रहे हैं।
वास्तव में ये तथाकथित धर्मगुरु अपने समय के कथा-वाचक हैं। पहले समय में ये अपनी मंडलियों के साथ जीवन-यापन के लिए गांवों -शहरों में कथाएं सुनाते घूमते थे। लोगों की छोटी-छोटी दान-दक्षिणा से इनका जीवन-यापन होता था। ये बंजारों की तरह घुमंतू हुआ करते थे। किन्तु समय के साथ इनके श्रोता कम होने लगे और इन लोगों ने भी किसी मन्दिर, सामाजिक स्थानों के निकट अपना एक निश्चित ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। इन कथा-वाचकों के साथ अब निठल्लों, अपराधियों, बेरोज़गारों का भी साथ होने लगा। जीवन-यापन के लिए इन्होंने धर्म की आड़ लेनी शुरू कर दी। धर्म के साथ पाखंड जुड़ा, फिर राजनीति।
ऐसे लोगों पर देश का प्रायः कोई कानून लागू नहीं होता। इस बात का ही फा़यदा उठाकर; देश में फैले अंधविश्वास, निर्धनता, निरक्षरता, और दूसरी ओर राजनीति, काली कमाई के चलते इन लोगों को हमने ही उच्च पदासीन कर दिया और अपनी गाढ़ी कमाई से इनके बड़े-बडे़ करोड़ों-अरबों के आश्रम, मन्दिर, मूर्तियां, सिंहासन रच दिये। जब ये धर्मगुरू ही नहीं तो धार्मिक आचरण की अपेक्षा ही कैसे?
ऐसे तथाकथित गुरुओं, स्वामियांे के लिए कानून होना चाहिए कि वे एक सीमा से अधिक सम्पत्ति अर्जित न कर सकें, अपनी आय का सम्पूर्ण विवरण जनता को दें, इन्हें कर के दायरे में लिया जाना चाहिए एवं सरकारी सम्पत्ति अथवा भूमि पर कार्यक्रमों की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात मीडिया को इनका प्रचारक नहीं बनना चाहिए फिर वे विज्ञापन हों अथवा धार्मिक प्रसारण।
अहंकार द्वेष ईर्ष्या
तीनों शब्द अहंकार ,द्वेष ,ईर्ष्या बोलने में हम साथ साथ बोल लेते हैं किन्तु सभी भिन्नार्थक हैं।
अहंकार मानव अपने आप पर करता है। जब मनुष्य को अपने गुणों, स्थिति, धन-सम्पत्ति अथवा योग्यता अर्थात व्यक्तिगत उपलब्धियों पर अभिमान होने लगता है और वह दूसरे को अपने से हीन मानने लगता है तब वह अहंकार की स्थिति में आ जाता है।
ईर्ष्या प्रतियोगिता की अगली सीढ़ी है। जब हम प्रतियोगिता में किसी से आगे नहीं बढ़ सकते, तब उससे ईर्ष्या करने लगते हैं
ईर्ष्या तब होती है जब हम अपने आप को दूसरों से हीन समझने लगते हैं तभी तो किसी की प्रगति, उपलब्धि, धन-सम्पत्ति, योग्यता आदि की जब अकारण ही आलोचना करने लगते हैं, उसकी योग्यताओं में कमियां ढूंढने लगते हैं तब वह ईर्ष्या की स्थिति बन जाती है।
द्वेष ईर्ष्या की अगली सीढ़ी है। ईर्ष्या में वैर-भाव, हानि पंहुचाने का भाव नहीं रहता, जबकि द्वेष-भाव की स्थिति में मनुष्य सामने वाले से आगे बढ़ने के लिए कोई भी तरीका अपनाने का प्रयास करता है, उसका बुरा चाहने लगता है। फिर वह उसका रास्ता काटना हो, उसके रास्ते में रोड़े अटकाना हो अथवा स्वयं गलत रास्ते पर चलकर उससे आगे बढ़ना।
प्रतियोगिता का भाव मानव मन में बने रहना आवश्यक है तभी वह प्रगति कर सकता है। किन्तु कब वह अंहकार, ईर्ष्या, द्वेष में परिवर्तित हो जाता है वह मानव स्वयं भी नहीं जानता।
असमंजस में नई पीढ़ी
आज हमारी पीढ़ी तीन कालखण्डों में जी रही है।
एक वह जो हमारे पूर्वज हमें सौंप गये। दूसरा हमारा स्वयं का विकसित वर्तमान और तीसरा हमारी भावी पीढ़ी जिसमें हम अपना भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों खोजते हैं।
वर्तमान समाज की सबसे कठिन समस्या है इन तीनों के मध्य सामंजस्य बिठाना। अतीत हमें छोड़ता नहीं, वर्तमान हमारी आवश्यकता है। और भविष्य हमें अपने हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है।
एक असमंजस की स्थिति है। धर्म, परम्परा, संस्कृति, रीति रिवाज़, संस्कार, व्यवहार, जो हमें पूर्वजों से मिले हैं उनकी गठरी अपनी पीठ पर बांधे हम विवश से घूम रहे हैं। न ढोने की स्थिति में हैं और न परित्याग कर सकते हैं क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अन्तर है। हम उस गठरी का परित्याग करना तो चाहते हैं किन्तु समाज से डरते हैं। और इस चिन्ता में भी रहते हैं कि इसमें न जाने कब कुछ काम का मिल जाये। अपनी आवश्यकतानुसार, सुविधानुसार उसमें कांट छांट कर लेते हैं। अपनी जीवन शैली को सरल सहज, सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ जोड़ लेते हैं कुछ छोड़ देते हैं। और जो मनभावन प्रतीत नहीं होता उसे तिरोहित कर देते हैं। उनका गुणगान तो करते हैं किन्तु निभा नहीं पाते।
इसका दुष्परिणाम हमारी भावी पीढ़ी भुगत रही है। हमने अपनी पीठ की गठरी के साथ साथ अपने समय की भी एक गठरी भी तैयार कर ली है और हम चाहते हैं कि हमारी भावी पीढ़ी अपनी नवीन जीवन शैली के साथ इन दोनों के बीच संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित करे। उसका अपना एक नवीन, आधुनिक, विकसित, वैज्ञानिक समाज है जहां हमने स्वयं उसे भेजा है। किन्तु उसे हम स्वतन्त्रतापूर्वक आगे बढ़ने नहीं दे रहे, अपनी तीनों गठरियों का बोझ उनके कंधे पर लाद कर चले हैं।